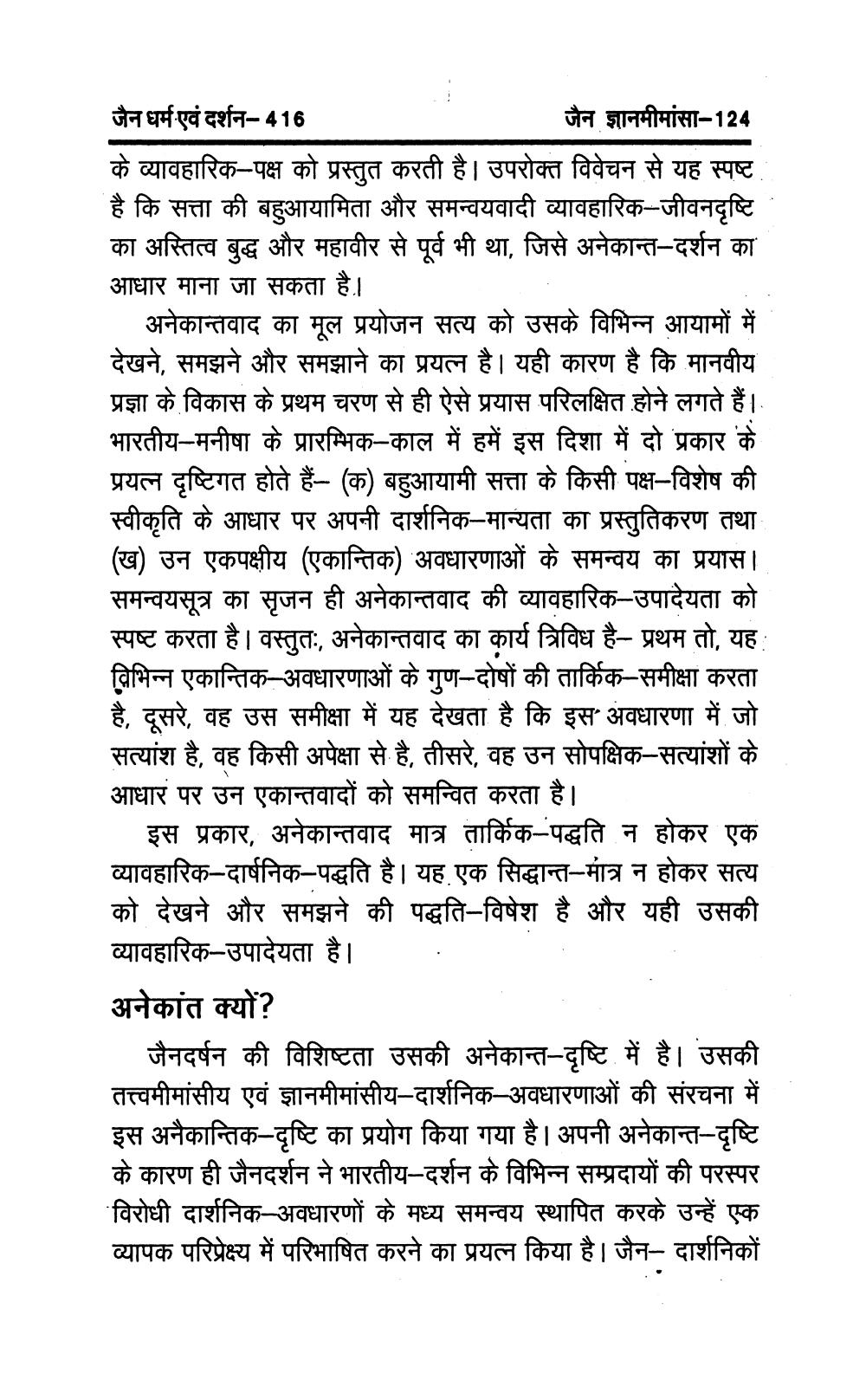________________ जैन धर्म एवं दर्शन-416 जैन ज्ञानमीमांसा-124 के व्यावहारिक-पक्ष को प्रस्तुत करती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सत्ता की बहुआयामिता और समन्वयवादी व्यावहारिक-जीवनदृष्टि का अस्तित्व बुद्ध और महावीर से पूर्व भी था, जिसे अनेकान्त-दर्शन का आधार माना जा सकता है। ___ अनेकान्तवाद का मूल प्रयोजन सत्य को उसके विभिन्न आयामों में देखने, समझने और समझाने का प्रयत्न है। यही कारण है कि मानवीय प्रज्ञा के विकास के प्रथम चरण से ही ऐसे प्रयास परिलक्षित होने लगते हैं। भारतीय-मनीषा के प्रारम्भिक काल में हमें इस दिशा में दो प्रकार के प्रयत्न दृष्टिगत होते हैं- (क) बहुआयामी सत्ता के किसी पक्ष-विशेष की स्वीकृति के आधार पर अपनी दार्शनिक-मान्यता का प्रस्तुतिकरण तथा (ख) उन एकपक्षीय (एकान्तिक) अवधारणाओं के समन्वय का प्रयास। समन्वयसूत्र का सृजन ही अनेकान्तवाद की व्यावहारिक-उपादेयता को स्पष्ट करता है। वस्तुतः, अनेकान्तवाद का कार्य त्रिविध है- प्रथम तो, यह विभिन्न एकान्तिक अवधारणाओं के गुण-दोषों की तार्किक-समीक्षा करता है, दूसरे, वह उस समीक्षा में यह देखता है कि इस अवधारणा में जो सत्यांश है, वह किसी अपेक्षा से है, तीसरे, वह उन सोपक्षिक-सत्यांशों के आधार पर उन एकान्तवादों को समन्वित करता है। इस प्रकार, अनेकान्तवाद मात्र तार्किक-पद्धति न होकर एक व्यावहारिक–दार्षनिक-पद्धति है। यह एक सिद्धान्त-मात्र न होकर सत्य को देखने और समझने की पद्धति-विषेश है और यही उसकी व्यावहारिक-उपादेयता है। अनेकांत क्यों? __ जैनदर्षन की विशिष्टता उसकी अनेकान्त-दृष्टि में है। उसकी तत्त्वमीमांसीय एवं ज्ञानमीमांसीय-दार्शनिक अवधारणाओं की संरचना में इस अनैकान्तिक-दृष्टि का प्रयोग किया गया है। अपनी अनेकान्त-दृष्टि के कारण ही जैनदर्शन ने भारतीय-दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों की परस्पर विरोधी दार्शनिक अवधारणों के मध्य समन्वय स्थापित करके उन्हें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जैन- दार्शनिकों