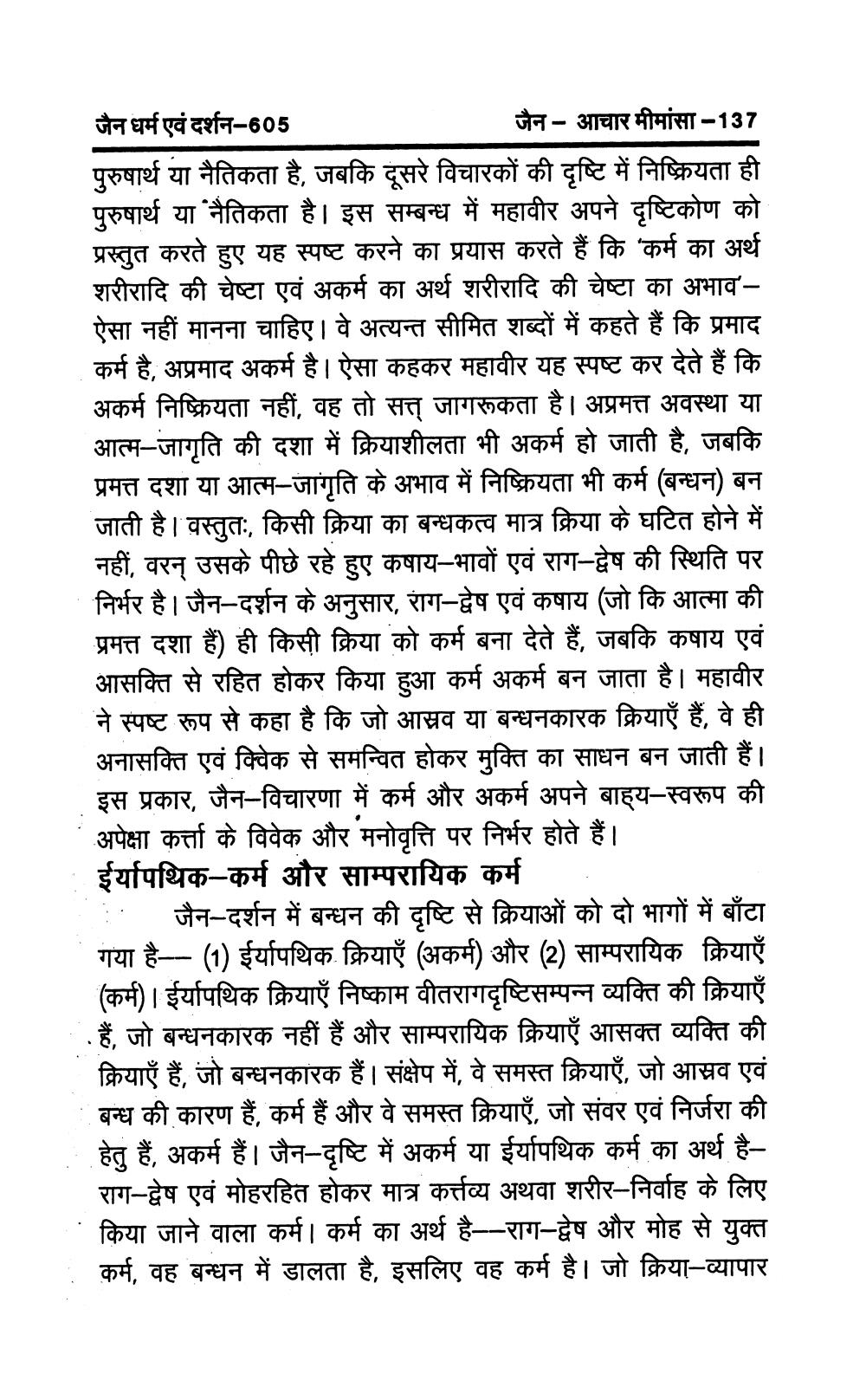________________ जैन धर्म एवं दर्शन-605 जैन- आचार मीमांसा-137 पुरुषार्थ या नैतिकता है, जबकि दूसरे विचारकों की दृष्टि में निष्क्रियता ही पुरुषार्थ या नैतिकता है। इस सम्बन्ध में महावीर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि 'कर्म का अर्थ शरीरादि की चेष्टा एवं अकर्म का अर्थ शरीरादि की चेष्टा का अभाव'ऐसा नहीं मानना चाहिए। वे अत्यन्त सीमित शब्दों में कहते हैं कि प्रमाद कर्म है, अप्रमाद अकर्म है। ऐसा कहकर महावीर यह स्पष्ट कर देते हैं कि अकर्म निष्क्रियता नहीं, वह तो सत्त जागरूकता है। अप्रमत्त अवस्था या आत्म-जागृति की दशा में क्रियाशीलता भी अकर्म हो जाती है, जबकि प्रमत्त दशा या आत्म-जागृति के अभाव में निष्क्रियता भी कर्म (बन्धन) बन जाती है। वस्तुतः, किसी क्रिया का बन्धकत्व मात्र क्रिया के घटित होने में नहीं, वरन् उसके पीछे रहे हुए कषाय-भावों एवं राग-द्वेष की स्थिति पर निर्भर है। जैन-दर्शन के अनुसार, राग-द्वेष एवं कषाय (जो कि आत्मा की प्रमत्त दशा हैं) ही किसी क्रिया को कर्म बना देते हैं, जबकि कषाय एवं आसक्ति से रहित होकर किया हुआ कर्म अकर्म बन जाता है। महावीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आस्रव या बन्धनकारक क्रियाएँ हैं, वे ही अनासक्ति एवं क्वेिक से समन्वित होकर मुक्ति का साधन बन जाती हैं। इस प्रकार, जैन-विचारणा में कर्म और अकर्म अपने बाह्य-स्वरूप की अपेक्षा कर्ता के विवेक और मनोवृत्ति पर निर्भर होते हैं। ईर्यापथिक-कर्म और साम्परायिक कर्म - जैन-दर्शन में बन्धन की दृष्टि से क्रियाओं को दो भागों में बाँटा गया है- (1) ईर्यापथिक क्रियाएँ (अकर्म) और (2) साम्परायिक क्रियाएँ (कर्म)। ईर्यापथिक क्रियाएँ निष्काम वीतरागदृष्टिसम्पन्न व्यक्ति की क्रियाएँ . हैं, जो बन्धनकारक नहीं हैं और साम्परायिक क्रियाएँ आसक्त व्यक्ति की क्रियाएँ हैं, जो बन्धनकारक हैं। संक्षेप में, वे समस्त क्रियाएँ, जो आस्रव एवं बन्ध की कारण हैं, कर्म हैं और वे समस्त क्रियाएँ, जो संवर एवं निर्जरा की हेतु हैं, अकर्म हैं। जैन-दृष्टि में अकर्म या ईर्यापथिक कर्म का अर्थ हैराग-द्वेष एवं मोहरहित होकर मात्र कर्त्तव्य अथवा शरीर-निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। कर्म का अर्थ है-राग-द्वेष और मोह से युक्त . कर्म, वह बन्धन में डालता है, इसलिए वह कर्म है। जो क्रिया-व्यापार