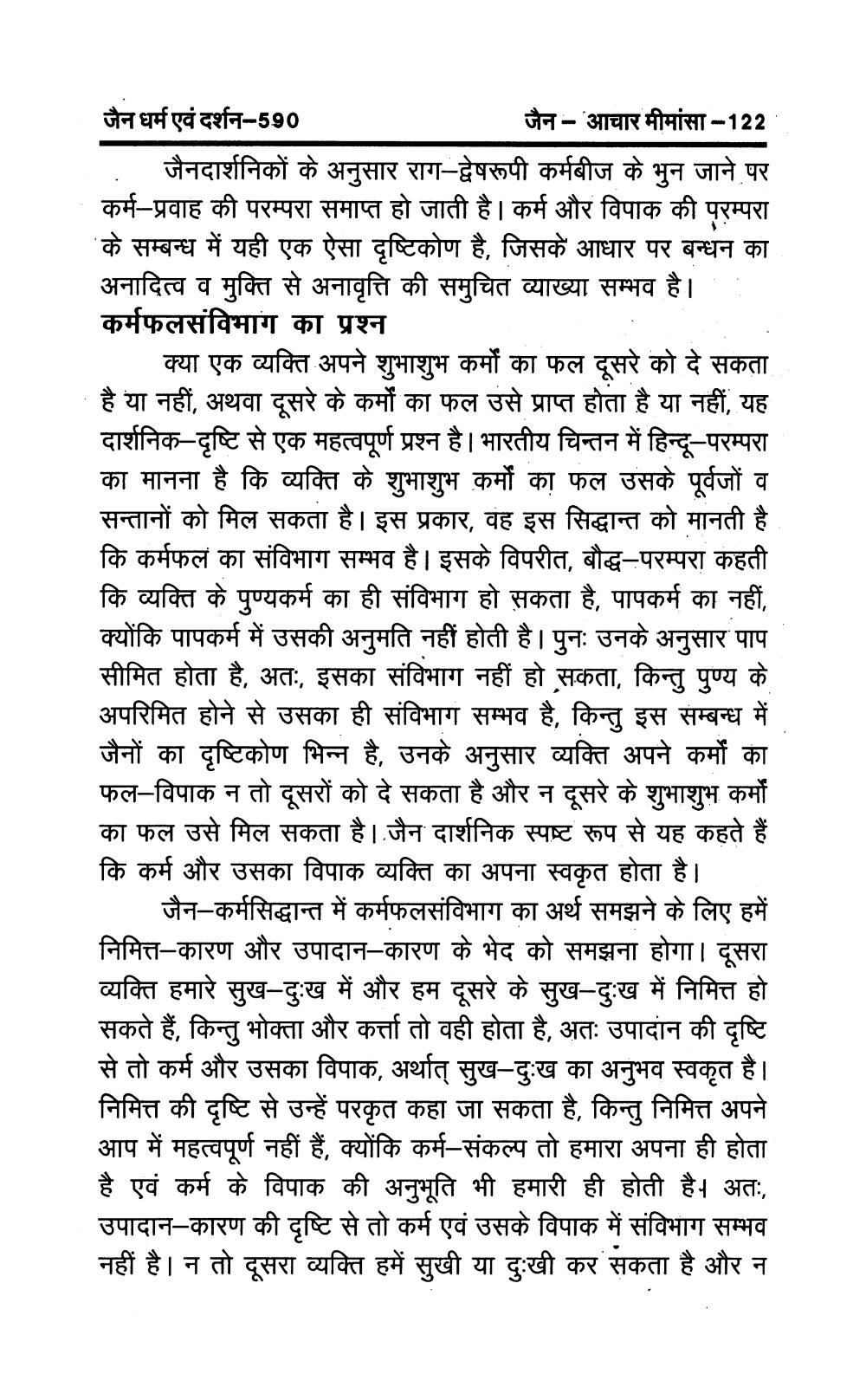________________ जैन धर्म एवं दर्शन-590 जैन -आचार मीमांसा-122 . जैनदार्शनिकों के अनुसार राग-द्वेषरूपी कर्मबीज के भुन जाने पर कर्म-प्रवाह की परम्परा समाप्त हो जाती है। कर्म और विपाक की परम्परा के सम्बन्ध में यही एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर बन्धन का अनादित्व व मुक्ति से अनावृत्ति की समुचित व्याख्या सम्भव है। कर्मफलसंविभाग का प्रश्न क्या एक व्यक्ति अपने शुभाशुभ कर्मों का फल दूसरे को दे सकता है या नहीं, अथवा दूसरे के कर्मों का फल उसे प्राप्त होता है या नहीं, यह दार्शनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय चिन्तन में हिन्दू परम्परा का मानना है कि व्यक्ति के शुभाशुभ कर्मों का फल उसके पूर्वजों व सन्तानों को मिल सकता है। इस प्रकार, वह इस सिद्धान्त को मानती है कि कर्मफल का संविभाग सम्भव है। इसके विपरीत, बौद्ध-परम्परा कहती कि व्यक्ति के पुण्यकर्म का ही संविभाग हो सकता है, पापकर्म का नहीं, क्योंकि पापकर्म में उसकी अनुमति नहीं होती है। पुनः उनके अनुसार पाप सीमित होता है, अतः, इसका संविभाग नहीं हो सकता, किन्तु पुण्य के अपरिमित होने से उसका ही संविभाग सम्भव है, किन्तु इस सम्बन्ध में जैनों का दृष्टिकोण भिन्न है, उनके अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों का फल-विपाक न तो दूसरों को दे सकता है और न दूसरे के शुभाशुभ कर्मों का फल उसे मिल सकता है। जैन दार्शनिक स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि कर्म और उसका विपाक व्यक्ति का अपना स्वकृत होता है। जैन-कर्मसिद्धान्त में कर्मफलसंविभाग का अर्थ समझने के लिए हमें निमित्त-कारण और उपादान–कारण के भेद को समझना होगा। दूसरा व्यक्ति हमारे सुख-दुःख में और हम दूसरे के सुख-दुःख में निमित्त हो सकते हैं, किन्तु भोक्ता और कर्ता तो वही होता है, अतः उपादान की दृष्टि से तो कर्म और उसका विपाक, अर्थात् सुख-दुःख का अनुभव स्वकृत है। निमित्त की दृष्टि से उन्हें परकृत कहा जा सकता है, किन्तु निमित्त अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि कर्म-संकल्प तो हमारा अपना ही होता है एवं कर्म के विपाक की अनुभूति भी हमारी ही होती है। अतः, उपादान-कारण की दृष्टि से तो कर्म एवं उसके विपाक में संविभाग सम्भव नहीं है। न तो दूसरा व्यक्ति हमें सुखी या दुःखी कर सकता है और न