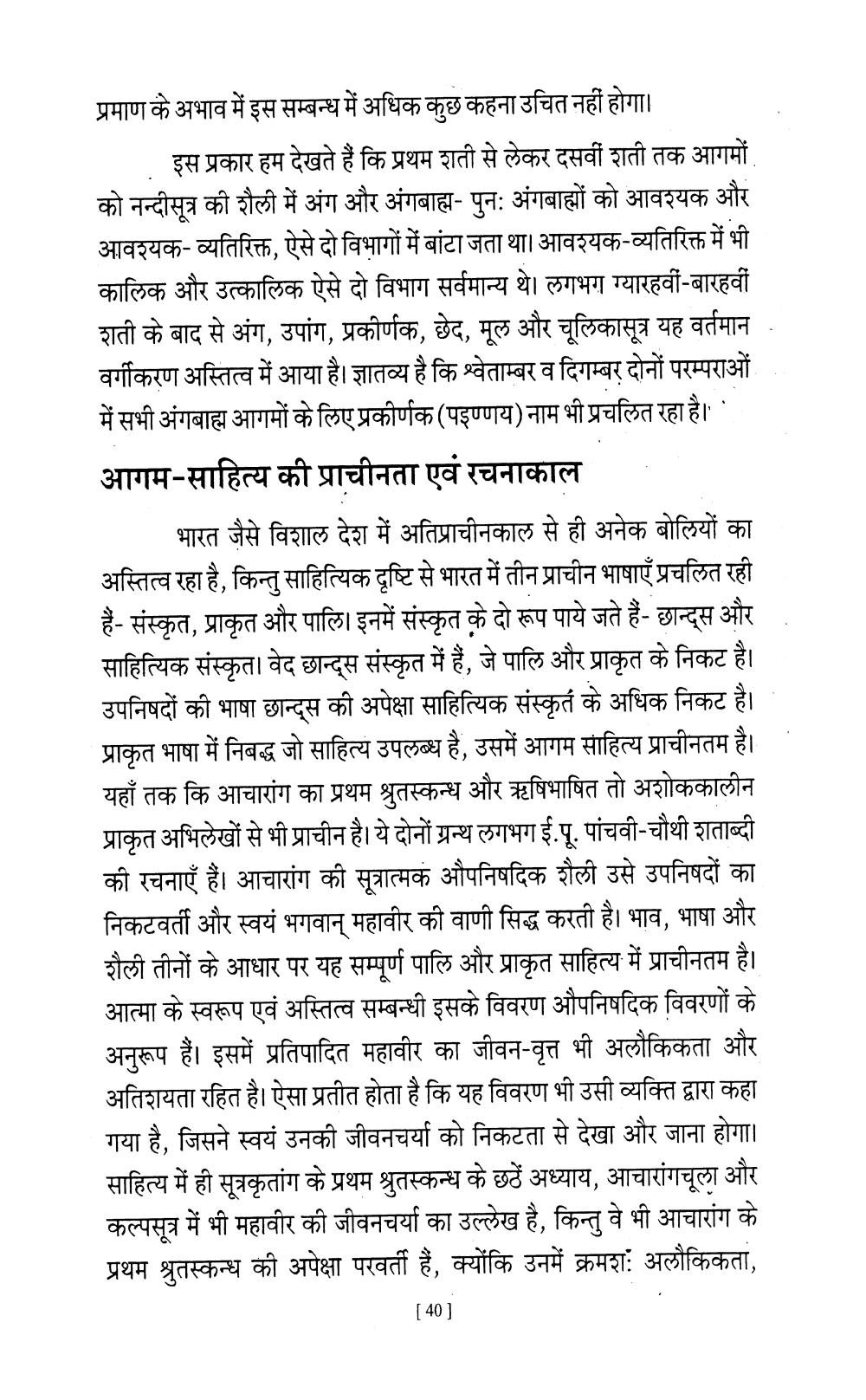________________ प्रमाण के अभाव में इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कहना उचित नहीं होगा। . इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम शती से लेकर दसवीं शती तक आगमों को नन्दीसूत्र की शैली में अंग और अंगबाह्म- पुन: अंगबारों को आवश्यक और आवश्यक- व्यतिरिक्त, ऐसे दो विभागों में बांटा जता था। आवश्यक-व्यतिरिक्त में भी कालिक और उत्कालिक ऐसे दो विभाग सर्वमान्य थे। लगभग ग्यारहवीं-बारहवीं शती के बाद से अंग, उपांग, प्रकीर्णक, छेद, मूल और चूलिकासूत्र यह वर्तमान वर्गीकरण अस्तित्व में आया है। ज्ञातव्य है कि श्वेताम्बर व दिगम्बर दोनों परम्पराओं में सभी अंगबाह्म आगमों के लिए प्रकीर्णक (पइण्णय) नाम भी प्रचलित रहा है। ' आगम-साहित्य की प्राचीनता एवं रचनाकाल ___भारत जैसे विशाल देश में अतिप्राचीनकाल से ही अनेक बोलियों का अस्तित्व रहा है, किन्तु साहित्यिक दृष्टि से भारत में तीन प्राचीन भाषाएँ प्रचलित रही है- संस्कृत, प्राकृत और पालि। इनमें संस्कृत के दो रूप पाये जते हैं- छान्द्स और साहित्यिक संस्कृत। वेद छान्द्स संस्कृत में हैं, जे पालि और प्राकृत के निकट है। उपनिषदों की भाषा छान्स की अपेक्षा साहित्यिक संस्कृतं के अधिक निकट है। प्राकृत भाषा में निबद्ध जो साहित्य उपलब्ध है, उसमें आगम साहित्य प्राचीनतम है। यहाँ तक कि आचारांग का प्रथम श्रुतस्कन्ध और ऋषिभाषित तो अशोककालीन प्राकृत अभिलेखों से भी प्राचीन है। ये दोनों ग्रन्थ लगभग ई.पू. पांचवी-चौथी शताब्दी की रचनाएँ हैं। आचारांग की सूत्रात्मक औपनिषदिक शैली उसे उपनिषदों का निकटवर्ती और स्वयं भगवान् महावीर की वाणी सिद्ध करती है। भाव, भाषा और शैली तीनों के आधार पर यह सम्पूर्ण पालि और प्राकृत साहित्य में प्राचीनतम है। आत्मा के स्वरूप एवं अस्तित्व सम्बन्धी इसके विवरण औपनिषदिक विवरणों के अनुरूप हैं। इसमें प्रतिपादित महावीर का जीवन-वृत्त भी अलौकिकता और अतिशयता रहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवरण भी उसी व्यक्ति द्वारा कहा गया है, जिसने स्वयं उनकी जीवनचर्या को निकटता से देखा और जाना होगा। साहित्य में ही सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्याय, आचारांगचूला और कल्पसूत्र में भी महावीर की जीवनचर्या का उल्लेख है, किन्तु वे भी आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध की अपेक्षा परवर्ती हैं, क्योंकि उनमें क्रमश: अलौकिकता, [40]