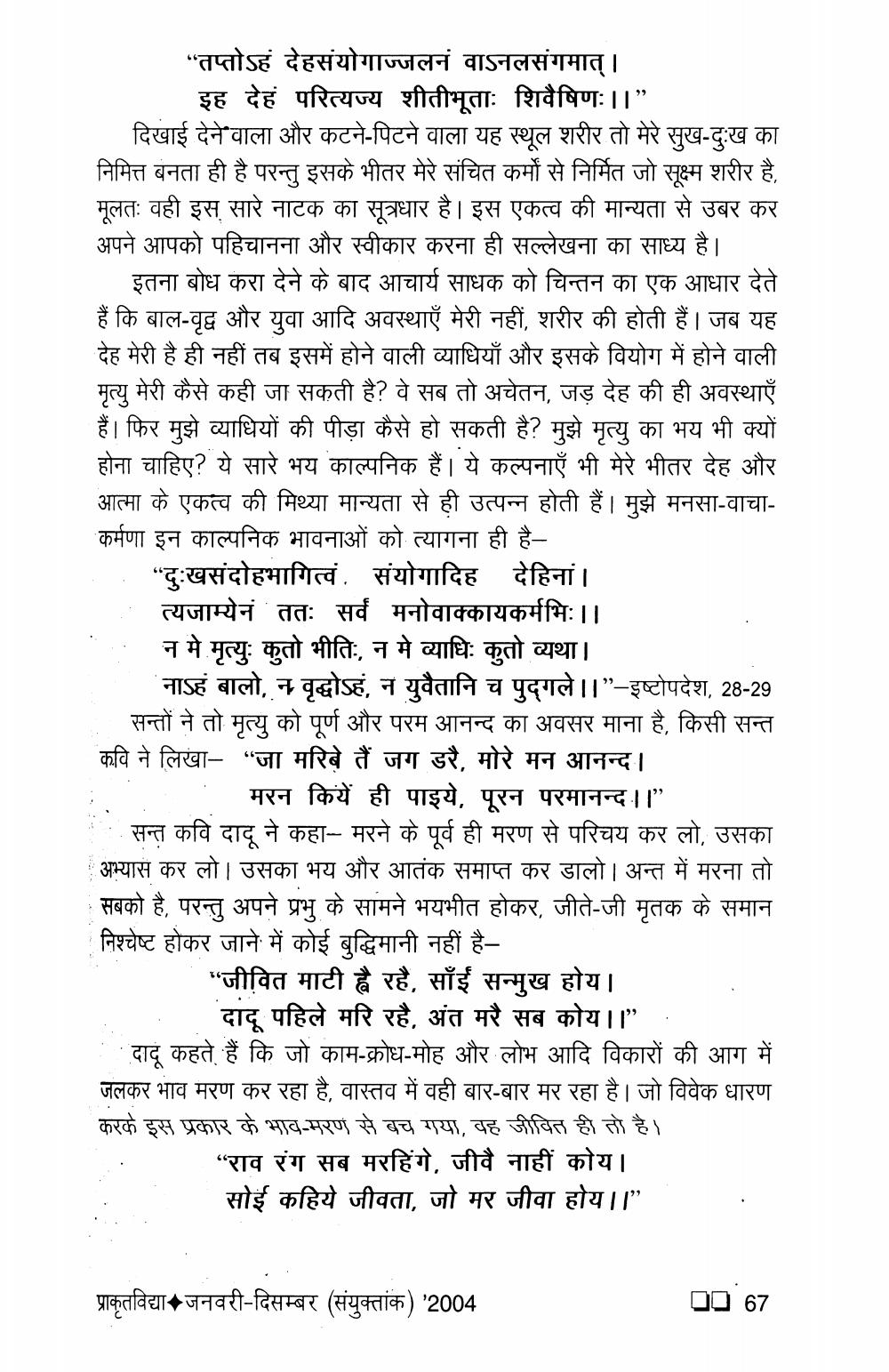________________ “तप्तोऽहं देहसंयोगाज्जलनं वाऽनलसंगमात् / इह देहं परित्यज्य शीतीभूताः शिवैषिणः।।" दिखाई देने वाला और कटने-पिटने वाला यह स्थूल शरीर तो मेरे सुख-दुःख का निमित्त बनता ही है परन्तु इसके भीतर मेरे संचित कर्मों से निर्मित जो सूक्ष्म शरीर है, मूलतः वही इस सारे नाटक का सूत्रधार है। इस एकत्व की मान्यता से उबर कर अपने आपको पहिचानना और स्वीकार करना ही सल्लेखना का साध्य है। इतना बोध करा देने के बाद आचार्य साधक को चिन्तन का एक आधार देते हैं कि बाल-वृद्व और युवा आदि अवस्थाएँ मेरी नहीं, शरीर की होती हैं। जब यह देह मेरी है ही नहीं तब इसमें होने वाली व्याधियाँ और इसके वियोग में होने वाली मृत्यु मेरी कैसे कही जा सकती है? वे सब तो अचेतन, जड़ देह की ही अवस्थाएँ हैं। फिर मुझे व्याधियों की पीड़ा कैसे हो सकती है? मुझे मृत्यु का भय भी क्यों होना चाहिए? ये सारे भय काल्पनिक हैं। ये कल्पनाएँ भी मेरे भीतर देह और आत्मा के एकत्व की मिथ्या मान्यता से ही उत्पन्न होती हैं। मुझे मनसा-वाचाकर्मणा इन काल्पनिक भावनाओं को त्यागना ही है "दुःखसंदोहभागित्वं. संयोगादिह देहिनां। त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः / / न मे मृत्युः कुतो भीतिः, न मे व्याधिः कुतो व्यथा। नाऽहं बालो, न वृद्धोऽहं, न युवैतानि च पुद्गले।।”–इष्टोपदेश, 28-29 सन्तों ने तो मृत्यु को पूर्ण और परम आनन्द का अवसर माना है, किसी सन्त कवि ने लिखा- “जा मरिबे तैं जग डरै, मोरे मन आनन्द। - मरन कियें ही पाइये, पूरन परमानन्द / / " - सन्त कवि दादू ने कहा- मरने के पूर्व ही मरण से परिचय कर लो, उसका अभ्यास कर लो। उसका भय और आतंक समाप्त कर डालो। अन्त में मरना तो सबको है, परन्तु अपने प्रभु के सामने भयभीत होकर, जीते-जी मृतक के समान निश्चेष्ट होकर जाने में कोई बुद्धिमानी नहीं है "जीवित माटी है रहै, साँई सन्मुख होय। दादू पहिले मरि रहै, अंत मरै सब कोय।।" - दादू कहते हैं कि जो काम-क्रोध-मोह और लोभ आदि विकारों की आग में जलकर भाव मरण कर रहा है, वास्तव में वही बार-बार मर रहा है। जो विवेक धारण करके इस प्रकार के भाव-मरण से बच गया, वह जीवित ही तो है। “राव रंग सब मरहिंगे, जीवै नाहीं कोय। सोई कहिये जीवता, जो मर जीवा होय।।" प्राकृतविद्या-जनवरी-दिसम्बर (संयुक्तांक) '2004 1067