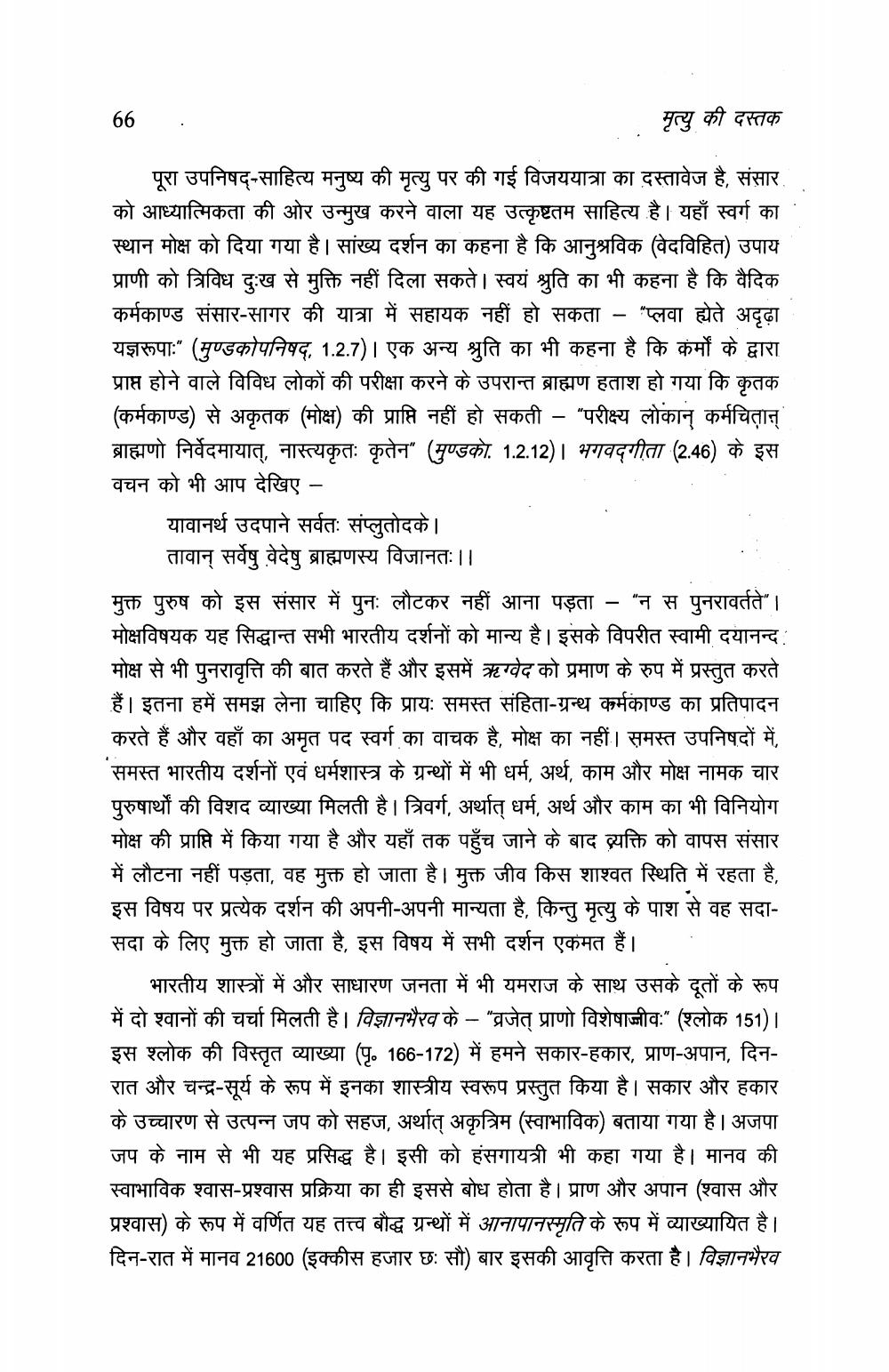________________ 66 . मृत्यु की दस्तक पूरा उपनिषद्-साहित्य मनुष्य की मृत्यु पर की गई विजययात्रा का दस्तावेज है, संसार को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करने वाला यह उत्कृष्टतम साहित्य है। यहाँ स्वर्ग का स्थान मोक्ष को दिया गया है। सांख्य दर्शन का कहना है कि आनुश्रविक (वेदविहित) उपाय प्राणी को त्रिविध दुःख से मुक्ति नहीं दिला सकते। स्वयं श्रुति का भी कहना है कि वैदिक कर्मकाण्ड संसार-सागर की यात्रा में सहायक नहीं हो सकता - “प्लवा ह्येते अदृढ़ा यज्ञरूपाः” (मुण्डकोपनिषद्, 1.2.7) / एक अन्य श्रुति का भी कहना है कि कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले विविध लोकों की परीक्षा करने के उपरान्त ब्राह्मण हताश हो गया कि कृतक (कर्मकाण्ड) से अकृतक (मोक्ष) की प्राप्ति नहीं हो सकती - “परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात्, नास्त्यकृतः कृतेन" (मुण्डको. 1.2.12) / भगवद्गीता (2.46) के इस वचन को भी आप देखिए - यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः / / मुक्त पुरुष को इस संसार में पुनः लौटकर नहीं आना पड़ता - “न स पुनरावर्तते / मोक्षविषयक यह सिद्धान्त सभी भारतीय दर्शनों को मान्य है। इसके विपरीत स्वामी दयानन्द मोक्ष से भी पुनरावृत्ति की बात करते हैं और इसमें ऋग्वेद को प्रमाण के रुप में प्रस्तुत करते हैं। इतना हमें समझ लेना चाहिए कि प्रायः समस्त संहिता-ग्रन्थ कर्मकाण्ड का प्रतिपादन करते हैं और वहाँ का अमृत पद स्वर्ग का वाचक है, मोक्ष का नहीं। समस्त उपनिषदों में, समस्त भारतीय दर्शनों एवं धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार पुरुषार्थों की विशद व्याख्या मिलती है। त्रिवर्ग, अर्थात् धर्म, अर्थ और काम का भी विनियोग मोक्ष की प्राप्ति में किया गया है और यहाँ तक पहुँच जाने के बाद व्यक्ति को वापस संसार में लौटना नहीं पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। मुक्त जीव किस शाश्वत स्थिति में रहता है, इस विषय पर प्रत्येक दर्शन की अपनी-अपनी मान्यता है, किन्तु मृत्यु के पाश से वह सदासदा के लिए मुक्त हो जाता है, इस विषय में सभी दर्शन एकमत हैं। भारतीय शास्त्रों में और साधारण जनता में भी यमराज के साथ उसके दूतों के रूप में दो श्वानों की चर्चा मिलती है। विज्ञानभैरव के - "व्रजेत् प्राणो विशेषाज्जीवः” (श्लोक 151) / इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या (पृ. 166-172) में हमने सकार-हकार, प्राण-अपान, दिनरात और चन्द्र-सूर्य के रूप में इनका शास्त्रीय स्वरूप प्रस्तुत किया है। सकार और हकार के उच्चारण से उत्पन्न जप को सहज, अर्थात् अकृत्रिम (स्वाभाविक) बताया गया है। अजपा जप के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इसी को हंसगायत्री भी कहा गया है। मानव की स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया का ही इससे बोध होता है। प्राण और अपान (श्वास और प्रश्वास) के रूप में वर्णित यह तत्त्व बौद्ध ग्रन्थों में आनापानस्मृति के रूप में व्याख्यायित है। दिन-रात में मानव 21600 (इक्कीस हजार छ: सौ) बार इसकी आवृत्ति करता है। विज्ञानभैरव