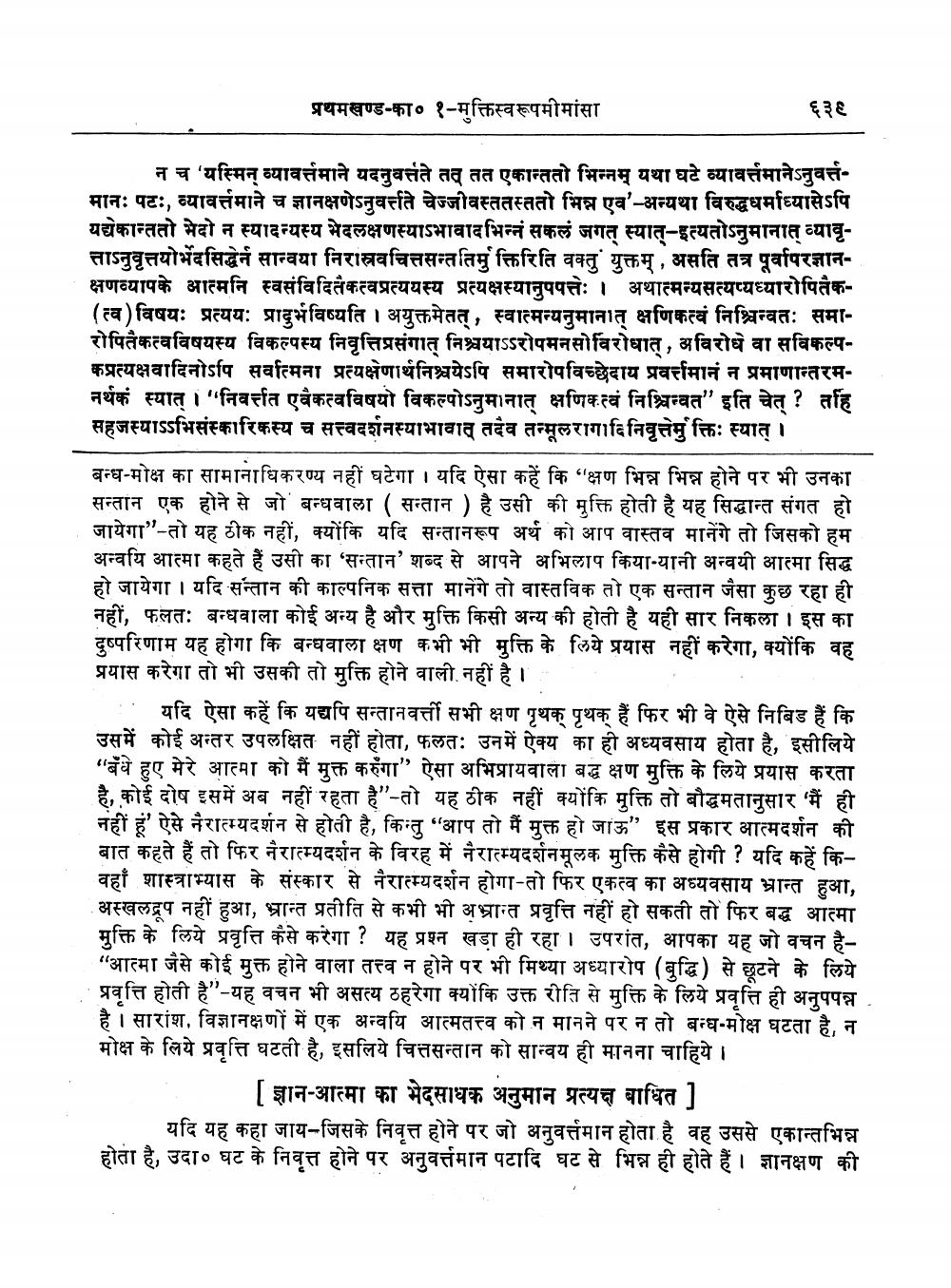________________ प्रथमखण्ड-का० १-मुक्तिस्वरूपमीमांसा 636 न च 'यस्मिन् व्यावर्त्तमाने यदनुवर्तते तत् तत एकान्ततो भिन्नम् यथा घटे व्यावर्त्तमानेऽनुवर्तमानः पटः, व्यावर्त्तमाने च ज्ञानक्षणेऽनुवर्तते चेज्जीवस्ततस्ततो भिन्न एव'-अन्यथा विरुद्धधर्माध्यासेऽपि यद्येकान्ततो भेदो न स्यादन्यस्य भेदलक्षणस्याऽभावादभिन्नं सकलं जगत् स्यात्-इत्यतोऽनुमानात व्यावृताऽनुवृत्तयोर्भेदसिद्धेर्न सान्वया निरास्रवचित्तसन्ततिमुक्तिरिति वक्तुयुक्तम् , असति तत्र पूर्वापरज्ञानक्षणव्यापके आत्मनि स्वसंविदितैकत्वप्रत्ययस्य प्रत्यक्षस्यानुपपत्तेः / अथात्मन्यसत्यप्यध्यारोपितक(त्व) विषयः प्रत्ययः प्रादुर्भविष्यति / अयुक्तमेतत् , स्वात्मन्यनुमानात् क्षणिकत्वं निश्चिन्वतः समारोपितैकत्वविषयस्य विकल्पस्य निवृत्तिप्रसंगात निश्चयाऽऽरोपमनसोविरोधात , अविरोधे वा सविकल्पकप्रत्यक्षवादिनोऽपि सर्वात्मना प्रत्यक्षेणार्थनिश्चयेऽपि समारोपविच्छेदाय प्रवर्त्तमानं न प्रमाणान्तरमनर्थकं स्यात् / "निवर्त्तत एवैकत्वविषयो विकल्पोऽनुमानात् क्षणिकत्वं निश्चिन्वत" इति चेत् ? तर्हि सहजस्याऽऽभिसंस्कारिकस्य च सत्त्वदर्शनस्याभावात् तदैव तन्मूलरागादिनिवृत्तेमुक्तिः स्यात् / बन्ध-मोक्ष का सामानाधिकरण्य नहीं घटेगा। यदि ऐसा कहें कि "क्षण भिन्न भिन्न होने पर भी उनका सन्तान एक होने से जो बन्धवाला ( सन्तान ) है उसी की मुक्ति होती है यह सिद्धान्त संगत हो जायेगा"-तो यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि सन्तानरूप अर्थ को आप वास्तव मानेंगे तो जिसको हम अन्वयि आत्मा कहते हैं उसी का 'सन्तान' शब्द से आपने अभिलाप किया-यानी अन्वयी आत्मा सिद्ध हो जायेगा / यदि सन्तान की काल्पनिक सत्ता मानेंगे तो वास्तविक तो एक सन्तान जैसा कुछ रहा ही नहीं, फलतः बन्धवाला कोई अन्य है और मुक्ति किसी अन्य की होती है यही सार निकला। इस का दुष्परिणाम यह होगा कि बन्धवाला क्षण कभी भी मुक्ति के लिये प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वह प्रयास करेगा तो भी उसकी तो मुक्ति होने वाली नहीं है। .. यदि ऐसा कहें कि यद्यपि सन्तानवर्ती सभी क्षण पृथक् पृथक् हैं फिर भी वे ऐसे निबिड हैं कि उसमें कोई अन्तर उपलक्षित नहीं होता, फलतः उनमें ऐक्य का ही अध्यवसाय होता है, इसीलिये "बंधे हुए मेरे आत्मा को मैं मुक्त करूंगा” ऐसा अभिप्रायवाला बद्ध क्षण मुक्ति के लिये प्रयास करता है, कोई दोष इसमें अब नहीं रहता है"-तो यह ठीक नहीं क्योंकि मुक्ति तो बौद्धमतानुसार 'मैं ही नहीं हूं' ऐसे नैरात्म्यदर्शन से होती है, किन्तु "आप तो मैं मुक्त हो जाऊ” इस प्रकार आत्मदर्शन की बात कहते हैं तो फिर नैरात्म्यदर्शन के विरह में नैरात्म्यदर्शनमूलक मुक्ति कैसे होगी? यदि कहें किवहाँ शास्त्राभ्यास के संस्कार से नैरात्म्यदर्शन होगा-तो फिर एकत्व का अध्यवसाय भ्रान्त हुआ, अस्खलद्रूप नहीं हुआ, भ्रान्त प्रतीति से कभी भी अभ्रान्त प्रवृत्ति नहीं हो सकती तो फिर बद्ध आत्मा मुक्ति के लिये प्रवृत्ति कैसे करेगा? यह प्रश्न खड़ा ही रहा / उपरांत, आपका यह जो वचन है"आत्मा जैसे कोई मुक्त होने वाला तत्त्व न होने पर भी मिथ्या अध्यारोप (बुद्धि) से छूटने के लिये होती है"-यह वचन भी असत्य ठहरेगा क्योंकि उक्त रीति से मुक्ति के लिये प्रवृत्ति ही अनुपपन्न है। सारांश, विज्ञानक्षणों में एक अन्वयि आत्मतत्त्व को न मानने पर न तो बन्ध-मोक्ष घटता है, न मोक्ष के लिये प्रवृत्ति घटती है, इसलिये चित्तसन्तान को सान्वय ही मानना चाहिये। [ ज्ञान-आत्मा का भेदसाधक अनुमान प्रत्यक्ष बाधित ] यदि यह कहा जाय-जिसके निवृत्त होने पर जो अनुवर्तमान होता है वह उससे एकान्तभिन्न होता है, उदा० घट के निवृत्त होने पर अनुवर्तमान पटादि घट से भिन्न ही होते हैं। ज्ञानक्षण की