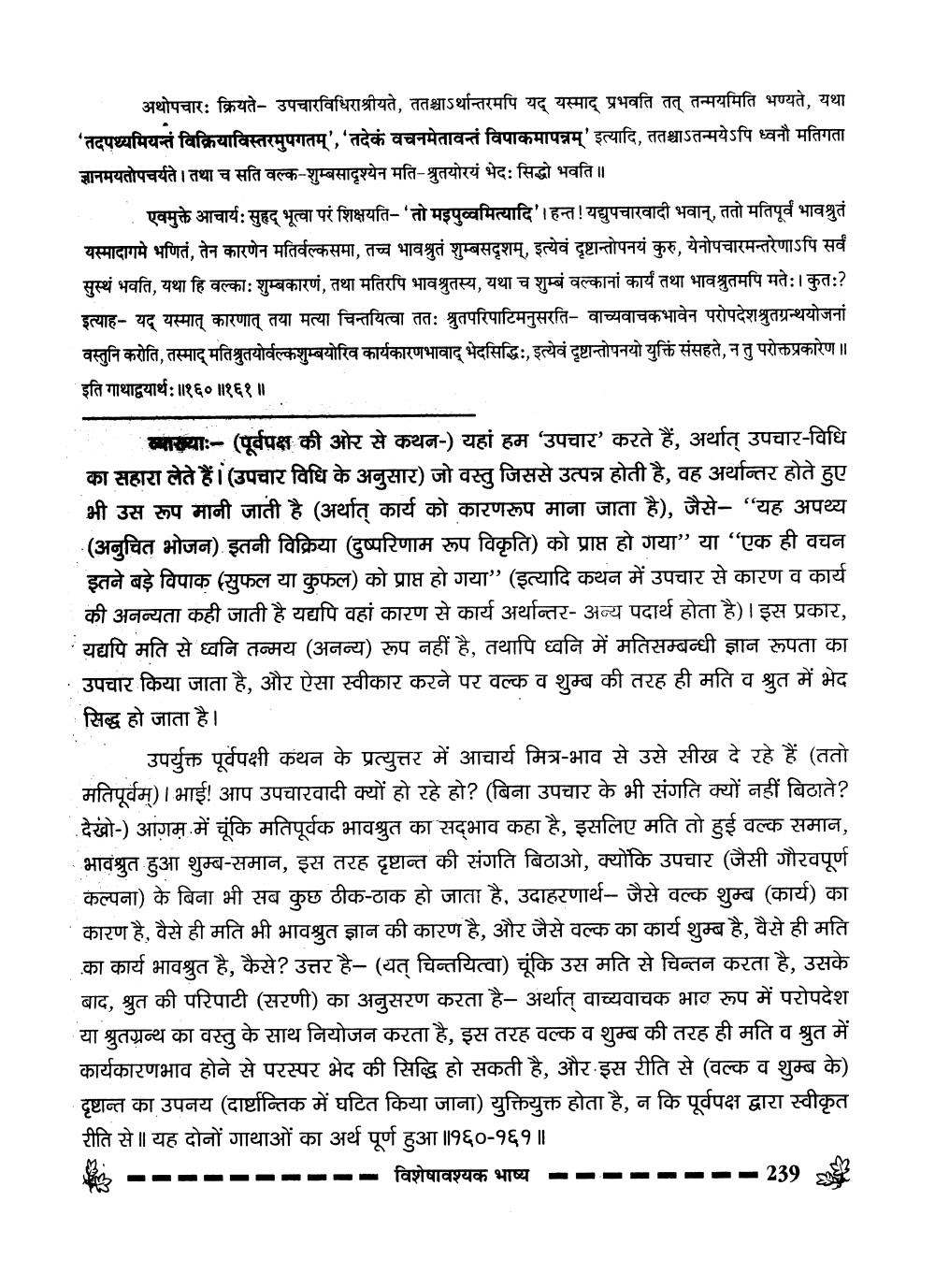________________ अथोपचारः क्रियते- उपचारविधिराश्रीयते, ततश्चाऽर्थान्तरमपि यद् यस्माद् प्रभवति तत् तन्मयमिति भण्यते, यथा 'तदपथ्यमियन्तं विक्रियाविस्तरमुपगतम्', 'तदेकं वचनमेतावन्तं विपाकमापन्नम्' इत्यादि, ततश्चाऽतन्मयेऽपि ध्वनौ मतिगता ज्ञानमयतोपचर्यते। तथा च सति वल्क-शुम्बसादृश्येन मति-श्रुतयोरयं भेदः सिद्धो भवति // . एवमुक्ते आचार्यः सुहृद् भूत्वा परं शिक्षयति- 'तो मइपुव्वमित्यादि'। हन्त ! यधुपचारवादी भवान्, ततो मतिपूर्वं भावश्रुतं यस्मादागमे भणितं, तेन कारणेन मतिर्वल्कसमा, तच्च भावश्रुतं शुम्बसदृशम्, इत्येवं दृष्टान्तोपनयं कुरु, येनोपचारमन्तरेणाऽपि सर्वं सुस्थं भवति, यथा हि वल्काः शुम्बकारणं, तथा मतिरपि भावश्रुतस्य, यथा च शुम्बं वल्कानां कार्यं तथा भावश्रुतमपि मतेः। कुतः? इत्याह- यद् यस्मात् कारणात् तया मत्या चिन्तयित्वा ततः श्रुतपरिपाटिमनुसरति- वाच्यवाचकभावेन परोपदेशश्रुतग्रन्थयोजनां वस्तुनि करोति, तस्माद् मतिश्रुतयोर्वल्कशुम्बयोरिव कार्यकारणभावाद् भेदसिद्धिः, इत्येवं दृष्टान्तोपनयो युक्तिं संसहते, न तु परोक्तप्रकारेण // इति गाथाद्वयार्थः // 160 // 161 // व्याख्याः - (पूर्वपक्ष की ओर से कथन-) यहां हम 'उपचार' करते हैं, अर्थात् उपचार-विधि का सहारा लेते हैं। (उपचार विधि के अनुसार) जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, वह अर्थान्तर होते हुए भी उस रूप मानी जाती है (अर्थात् कार्य को कारणरूप माना जाता है), जैसे- “यह अपथ्य (अनुचित भोजन) इतनी विक्रिया (दुष्परिणाम रूप विकृति) को प्राप्त हो गया” या “एक ही वचन इतने बड़े विपाक (सुफल या कुफल) को प्राप्त हो गया" (इत्यादि कथन में उपचार से कारण व कार्य की अनन्यता कही जाती है यद्यपि वहां कारण से कार्य अर्थान्तर- अन्य पदार्थ होता है)। इस प्रकार, यद्यपि मति से ध्वनि तन्मय (अनन्य) रूप नहीं है, तथापि ध्वनि में मतिसम्बन्धी ज्ञान रूपता का * उपचार किया जाता है, और ऐसा स्वीकार करने पर वल्क व शुम्ब की तरह ही मति व श्रुत में भेद सिद्ध हो जाता है। उपर्युक्त पूर्वपक्षी कथन के प्रत्युत्तर में आचार्य मित्र-भाव से उसे सीख दे रहे हैं (ततो मतिपूर्वम्)। भाई! आप उपचारवादी क्यों हो रहे हो? (बिना उपचार के भी संगति क्यों नहीं बिठाते? देखो-) आगम में चूंकि मतिपूर्वक भावश्रुत का सद्भाव कहा है, इसलिए मति तो हुई वल्क समान, भावश्रुत हुआ शुम्ब-समान, इस तरह दृष्टान्त की संगति बिठाओ, क्योंकि उपचार (जैसी गौरवपूर्ण कल्पना) के बिना भी सब कुछ ठीक-ठाक हो जाता है, उदाहरणार्थ- जैसे वल्क शुम्ब (कार्य) का कारण है, वैसे ही मति भी भावश्रुत ज्ञान की कारण है, और जैसे वल्क का कार्य शुम्ब है, वैसे ही मति का कार्य भावश्रुत है, कैसे? उत्तर है- (यत् चिन्तयित्वा) चूंकि उस मति से चिन्तन करता है, उसके बाद, श्रुत की परिपाटी (सरणी) का अनुसरण करता है- अर्थात् वाच्यवाचक भाव रूप में परोपदेश या श्रुतग्रन्थ का वस्तु के साथ नियोजन करता है, इस तरह वल्क व शुम्ब की तरह ही मति व श्रुत में कार्यकारणभाव होने से परस्पर भेद की सिद्धि हो सकती है, और इस रीति से (वल्क व शुम्ब के) दृष्टान्त का उपनय (दार्टान्तिक में घटित किया जाना) युक्तियुक्त होता है, न कि पूर्वपक्ष द्वारा स्वीकृत रीति से // यह दोनों गाथाओं का अर्थ पूर्ण हुआ // 160-161 // Mi ---------- विशेषावश्यक भाष्य --------239 AM