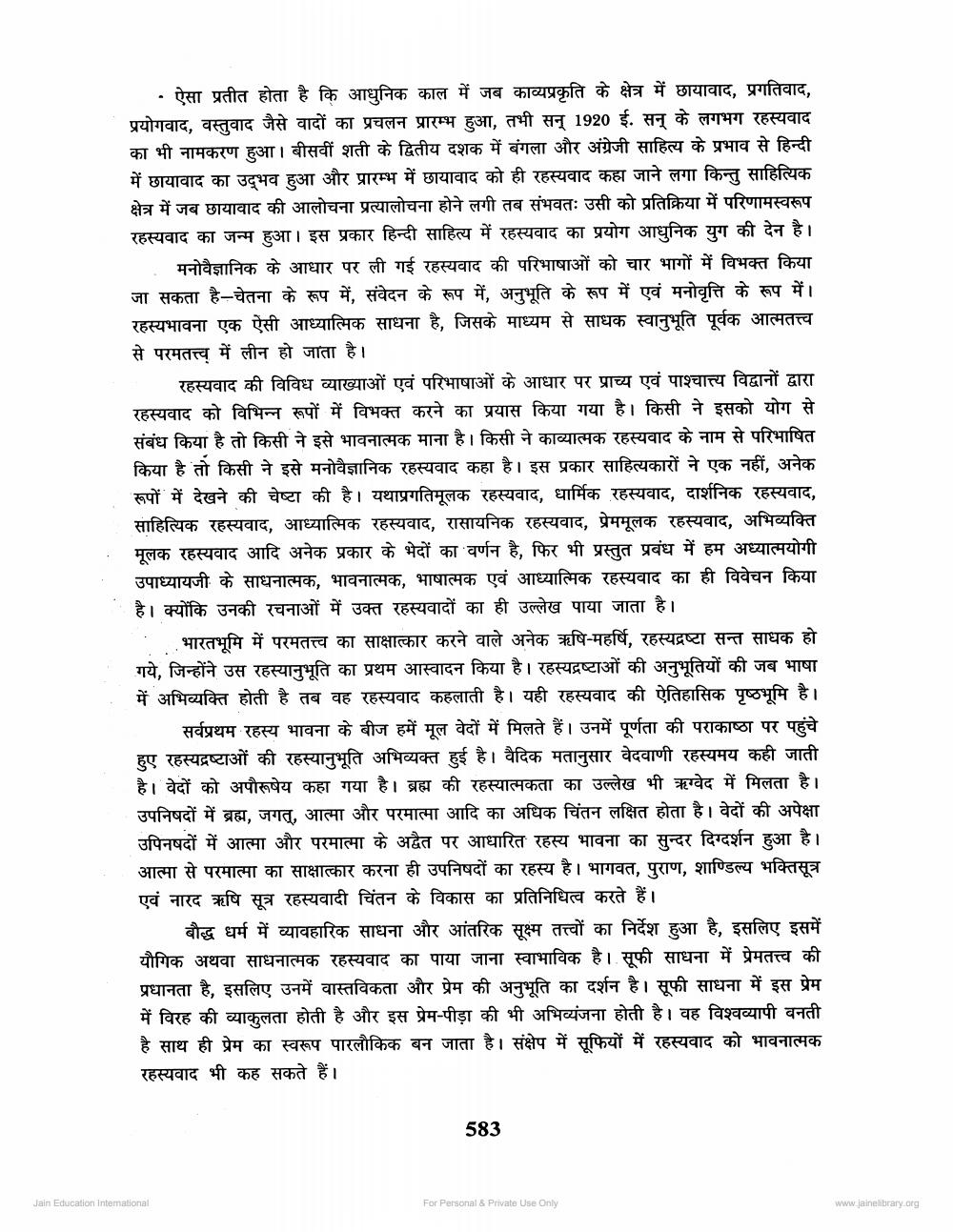________________ * ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक काल में जब काव्यप्रकृति के क्षेत्र में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, वस्तुवाद जैसे वादों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ, तभी सन् 1920 ई. सन् के लगभग रहस्यवाद का भी नामकरण हुआ। बीसवीं शती के द्वितीय दशक में बंगला और अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हिन्दी में छायावाद का उद्भव हुआ और प्रारम्भ में छायावाद को ही रहस्यवाद कहा जाने लगा किन्तु साहित्यिक क्षेत्र में जब छायावाद की आलोचना प्रत्यालोचना होने लगी तब संभवतः उसी को प्रतिक्रिया में परिणामस्वरूप रहस्यवाद का जन्म हुआ। इस प्रकार हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद का प्रयोग आधुनिक युग की देन है। . मनोवैज्ञानिक के आधार पर ली गई रहस्यवाद की परिभाषाओं को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है-चेतना के रूप में, संवेदन के रूप में, अनुभूति के रूप में एवं मनोवृत्ति के रूप में। रहस्यभावना एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है, जिसके माध्यम से साधक स्वानुभूति पूर्वक आत्मतत्त्व से परमतत्त्व में लीन हो जाता है। रहस्यवाद की विविध व्याख्याओं एवं परिभाषाओं के आधार पर प्राच्य एवं पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा रहस्यवाद को विभिन्न रूपों में विभक्त करने का प्रयास किया गया है। किसी ने इसको योग से संबंध किया है तो किसी ने इसे भावनात्मक माना है। किसी ने काव्यात्मक रहस्यवाद के नाम से परिभाषित किया है तो किसी ने इसे मनोवैज्ञानिक रहस्यवाद कहा है। इस प्रकार साहित्यकारों ने एक नहीं, अनेक रूपों में देखने की चेष्टा की है। यथाप्रगतिमूलक रहस्यवाद, धार्मिक रहस्यवाद, दार्शनिक रहस्यवाद, साहित्यिक रहस्यवाद, आध्यात्मिक रहस्यवाद, रासायनिक रहस्यवाद, प्रेममूलक रहस्यवाद, अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद आदि अनेक प्रकार के भेदों का वर्णन है, फिर भी प्रस्तुत प्रबंध में हम अध्यात्मयोगी उपाध्यायजी के साधनात्मक, भावनात्मक, भाषात्मक एवं आध्यात्मिक रहस्यवाद का ही विवेचन किया है। क्योंकि उनकी रचनाओं में उक्त रहस्यवादों का ही उल्लेख पाया जाता है। भारतभूमि में परमतत्त्व का साक्षात्कार करने वाले अनेक ऋषि-महर्षि, रहस्यद्रष्टा सन्त साधक हो गये, जिन्होंने उस रहस्यानुभूति का प्रथम आस्वादन किया है। रहस्यद्रष्टाओं की अनुभूतियों की जब भाषा में अभिव्यक्ति होती है तब वह रहस्यवाद कहलाती है। यही रहस्यवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सर्वप्रथम रहस्य भावना के बीज हमें मूल वेदों में मिलते हैं। उनमें पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए रहस्यद्रष्टाओं की रहस्यानुभूति अभिव्यक्त हुई है। वैदिक मतानुसार वेदवाणी रहस्यमय कही जाती है। वेदों को अपौरूषेय कहा गया है। ब्रह्म की रहस्यात्मकता का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म, जगत्, आत्मा और परमात्मा आदि का अधिक चिंतन लक्षित होता है। वेदों की अपेक्षा उपिनषदों में आत्मा और परमात्मा के अद्वैत पर आधारित रहस्य भावना का सुन्दर दिग्दर्शन हुआ है। आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार करना ही उपनिषदों का रहस्य है। भागवत, पुराण, शाण्डिल्य भक्तिसूत्र एवं नारद ऋषि सूत्र रहस्यवादी चिंतन के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध धर्म में व्यावहारिक साधना और आंतरिक सूक्ष्म तत्त्वों का निर्देश हुआ है, इसलिए इसमें यौगिक अथवा साधनात्मक रहस्यवाद का पाया जाना स्वाभाविक है। सूफी साधना में प्रेमतत्त्व की प्रधानता है, इसलिए उनमें वास्तविकता और प्रेम की अनुभूति का दर्शन है। सूफी साधना में इस प्रेम में विरह की व्याकुलता होती है और इस प्रेम-पीड़ा की भी अभिव्यंजना होती है। वह विश्वव्यापी बनती है साथ ही प्रेम का स्वरूप पारलौकिक बन जाता है। संक्षेप में सूफियों में रहस्यवाद को भावनात्मक रहस्यवाद भी कह सकते हैं। 583 Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org