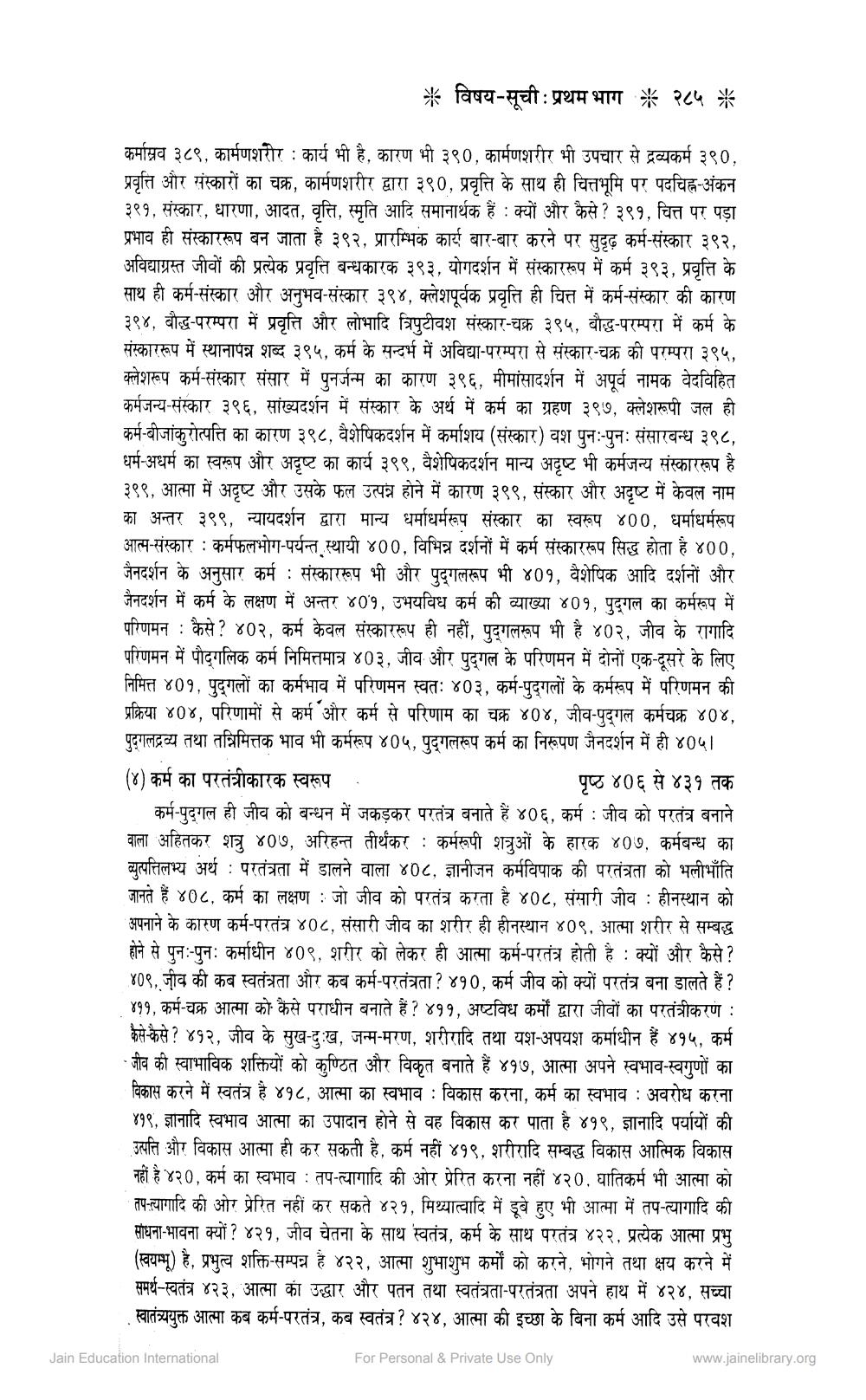________________
* विषय-सूची : प्रथम भाग * २८५ *
कर्मास्रव ३८९, कार्मणशरीर : कार्य भी है, कारण भी ३९0, कार्मणशरीर भी उपचार से द्रव्यकर्म ३९0, प्रवृत्ति और संस्कारों का चक्र, कार्मणशरीर द्वारा ३९०, प्रवृत्ति के साथ ही चित्तभूमि पर पदचिह्न-अंकन ३९१, संस्कार, धारणा, आदत, वृत्ति, स्मृति आदि समानार्थक हैं : क्यों और कैसे ? ३९१, चित्त पर पड़ा प्रभाव ही संस्काररूप बन जाता है ३९२, प्रारम्भिक कार्य बार-बार करने पर सुदृढ़ कर्म-संस्कार ३९२, अविद्याग्रस्त जीवों की प्रत्येक प्रवृत्ति बन्धकारक ३९३, योगदर्शन में संस्काररूप में कर्म ३९३, प्रवृत्ति के साथ ही कर्म-संस्कार और अनुभव-संस्कार ३९४, क्लेशपूर्वक प्रवृत्ति ही चित्त में कर्म-संस्कार की कारण ३९४, बौद्ध-परम्परा में प्रवृत्ति और लोभादि त्रिपुटीवश संस्कार-चक्र ३९५, बौद्ध-परम्परा में कर्म के संस्काररूप में स्थानापन्न शब्द ३९५, कर्म के सन्दर्भ में अविद्या-परम्परा से संस्कार-चक्र की परम्परा ३९५, क्लेशरूप कर्म-संस्कार संसार में पुनर्जन्म का कारण ३९६, मीमांसादर्शन में अपूर्व नामक वेदविहित कर्मजन्य-संस्कार ३९६, सांख्यदर्शन में संस्कार के अर्थ में कर्म का ग्रहण ३९७, क्लेशरूपी जल ही कर्म-बीजांकुरोत्पत्ति का कारण ३९८, वैशेषिकदर्शन में कर्माशय (संस्कार) वश पुनः पुनः संसारबन्ध ३९८, धर्म-अधर्म का स्वरूप और अदृष्ट का कार्य ३९९, वैशेषिकदर्शन मान्य अदृष्ट भी कर्मजन्य संस्काररूप है ३९९, आत्मा में अदृष्ट और उसके फल उत्पन्न होने में कारण ३९९. संस्कार और अदष्ट में केवल नाम का अन्तर ३९९, न्यायदर्शन द्वारा मान्य धर्माधर्मरूप संस्कार का स्वरूप ४00, धर्माधर्मरूप आत्म-संस्कार : कर्मफलभोग-पर्यन्त स्थायी ४00, विभिन्न दर्शनों में कर्म संस्काररूप सिद्ध होता है ४00, जैनदर्शन के अनुसार कर्म : संस्काररूप भी और पुदगलरूप भी ४०१, वैशेषिक आदि दर्शनों और जैनदर्शन में कर्म के लक्षण में अन्तर ४०१. उभयविध कर्म की व्याख्या ४०१. पदगल का कर्मरूप में परिणमन : कैसे? ४०२. कर्म केवल संस्काररूप ही नहीं. पदगलरूप भी है ४०२. जीव के रागादि परिणमन में पौदगलिक कर्म निमित्तमात्र ४०३. जीव और पदगल के परिणमन में दोनों एक-दसरे के लिए निमित्त ४०१. पदगलों का कर्मभाव में परिणमन स्वतः ४०३. कर्म-पदगलों के कर्मरूप में परिणमन की प्रक्रिया ४0४, परिणामों से कर्म और कर्म से परिणाम का चक्र ४०४, जीव-पुद्गल कर्मचक्र ४०४, पुद्गलद्रव्य तथा तनिमित्तक भाव भी कमरूप४०५, पुद्गलरूप कर्म का निरूपण जैनदर्शन में ही ४०५) (४) कर्म का परतंत्रीकारक स्वरूप .
पृष्ठ ४०६ से ४३१ तक कर्म-पुद्गल ही जीव को बन्धन में जकड़कर परतंत्र बनाते हैं ४०६, कर्म : जीव को परतंत्र बनाने वाला अहितकर शत्रु ४०७, अरिहन्त तीर्थंकर : कर्मरूपी शत्रुओं के हारक ४०७, कर्मबन्ध का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ : परतंत्रता में डालने वाला ४०८, ज्ञानीजन कर्मविपाक की परतंत्रता को भलीभाँति जानते हैं ४०८, कर्म का लक्षण : जो जीव को परतंत्र करता है ४०८, संसारी जीव : हीनस्थान को अपनाने के कारण कर्म-परतंत्र ४०८. संसारी जीव का शरीर ही हीनस्थान ४०९. आत्मा शरीर से सम्बद्ध होने से पुनः पुनः कर्माधीन ४०९, शरीर को लेकर ही आत्मा कर्म-परतंत्र होती है : क्यों और कैसे? ४०९, जीव की कब स्वतंत्रता और कब कर्म-परतंत्रता? ४१०, कर्म जीव को क्यों परतंत्र बना डालते हैं ? ४११, कर्म-चक्र आत्मा को कैसे पराधीन बनाते हैं ? ४११, अष्टविध कर्मों द्वारा जीवों का परतंत्रीकरण : कैसे-कैसे? ४१२, जीव के सुख-दुःख, जन्म-मरण, शरीरादि तथा यश-अपयश कर्माधीन हैं ४१५, कर्म - जीव की स्वाभाविक शक्तियों को कुण्ठित और विकृत बनाते हैं ४१७, आत्मा अपने स्वभाव-स्वगुणों का विकास करने में स्वतंत्र है ४१८, आत्मा का स्वभाव : विकास करना, कर्म का स्वभाव : अवरोध करना ४१९, ज्ञानादि स्वभाव आत्मा का उपादान होने से वह विकास कर पाता है ४१९, ज्ञानादि पर्यायों की उत्पत्ति और विकास आत्मा ही कर सकती है, कर्म नहीं ४१९, शरीरादि सम्बद्ध विकास आत्मिक विकास नहीं है ४२०, कर्म का स्वभाव : तप-त्यागादि की ओर प्रेरित करना नहीं ४२0. घातिकर्म भी आत्मा को तप-त्यागादि की ओर प्रेरित नहीं कर सकते ४२१, मिथ्यात्वादि में डूबे हुए भी आत्मा में तप-त्यागादि की साधना-भावना क्यों? ४२१, जीव चेतना के साथ स्वतंत्र, कर्म के साथ परतंत्र ४२२, प्रत्येक आत्मा प्रभु (स्वयम्भू) है, प्रभुत्व शक्ति-सम्पन्न है ४२२, आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करने, भोगने तथा क्षय करने में समर्थ-स्वतंत्र ४२३, आत्मा का उद्धार और पतन तथा स्वतंत्रता-परतंत्रता अपने हाथ में ४२४, सच्चा . स्वातंत्र्ययुक्त आत्मा कब कर्म-परतंत्र, कब स्वतंत्र? ४२४, आत्मा की इच्छा के बिना कर्म आदि उसे परवश
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org