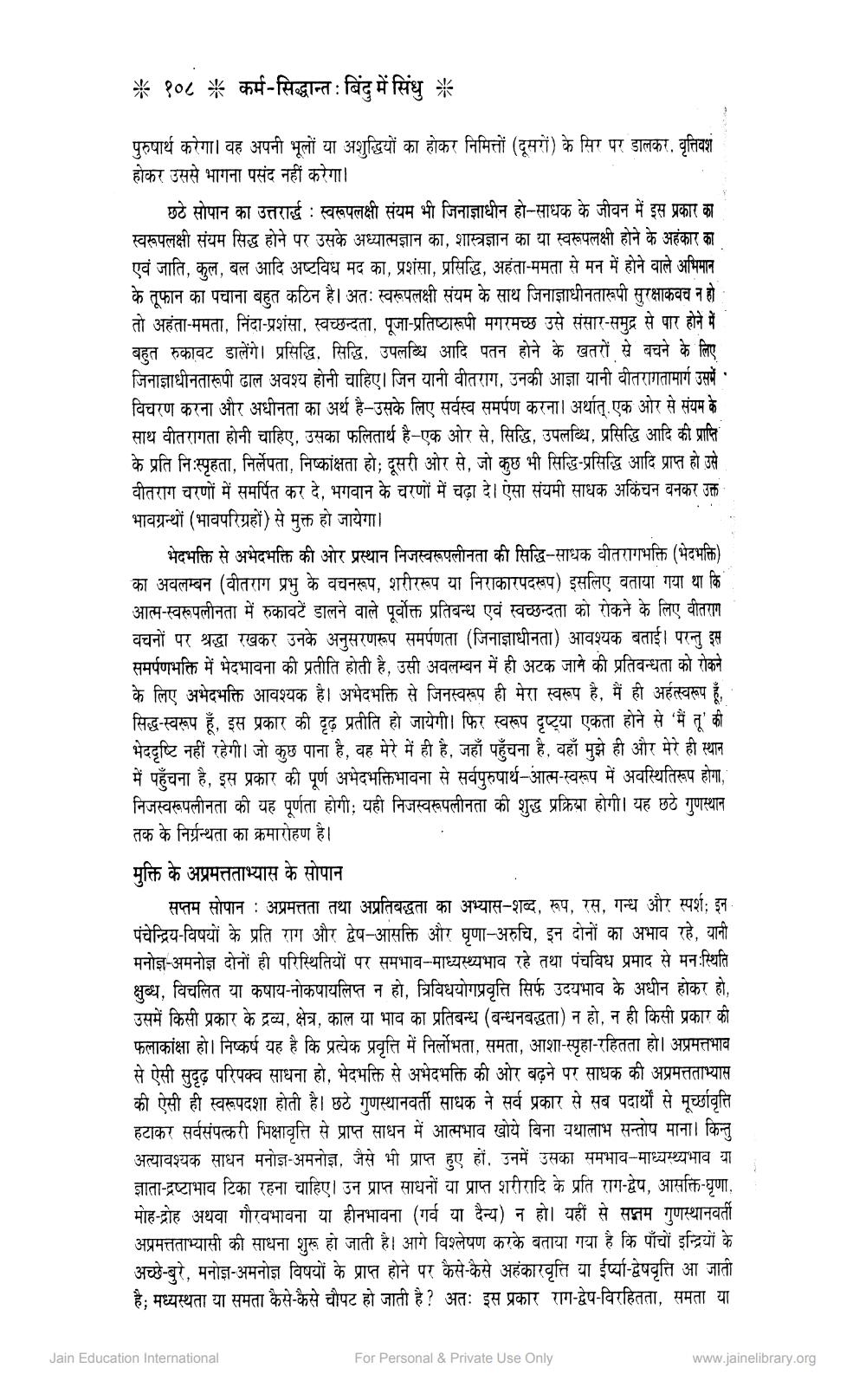________________
* १०८ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
पुरुषार्थ करेगा। वह अपनी भूलों या अशुद्धियों का होकर निमित्तों (दूसरों) के सिर पर डालकर. वृत्तिवश होकर उससे भागना पसंद नहीं करेगा।
छठे सोपान का उत्तरार्द्ध : स्वरूपलक्षी संयम भी जिनाज्ञाधीन हो-साधक के जीवन में इस प्रकार का स्वरूपलक्षी संयम सिद्ध होने पर उसके अध्यात्मज्ञान का, शास्त्रज्ञान का या स्वरूपलक्षी होने के अहंकार का एवं जाति, कुल, बल आदि अष्टविध मद का, प्रशंसा, प्रसिद्धि, अहंता-ममता से मन में होने वाले अभिमान के तूफान का पचाना बहुत कठिन है। अतः स्वरूपलक्षी संयम के साथ जिनाज्ञाधीनतारूपी सुरक्षाकवच न हो तो अहंता-ममता, निंदा-प्रशंसा, स्वच्छन्दता, पूजा-प्रतिष्ठारूपी मगरमच्छ उसे संसार-समुद्र से पार होने में बहुत रुकावट डालेंगे। प्रसिद्धि. सिद्धि, उपलब्धि आदि पतन होने के खतरों से बचने के लिए जिनाज्ञाधीनतारूपी ढाल अवश्य होनी चाहिए। जिन यानी वीतराग, उनकी आज्ञा यानी वीतरागतामार्ग उसमें । विचरण करना और अधीनता का अर्थ है-उसके लिए सर्वस्व समर्पण करना। अर्थात्. एक ओर से संयम के साथ वीतरागता होनी चाहिए, उसका फलितार्थ है-एक ओर से, सिद्धि, उपलब्धि, प्रसिद्धि आदि की प्राप्ति के प्रति निःस्पृहता, निर्लेपता, निष्कांक्षता हो; दूसरी ओर से, जो कुछ भी सिद्धि-प्रसिद्धि आदि प्राप्त हो उसे वीतराग चरणों में समर्पित कर दे, भगवान के चरणों में चढ़ा दे। ऐसा संयमी साधक अकिंचन बनकर उक्त भावग्रन्थों (भावपरिग्रहों) से मुक्त हो जायेगा। ___भेदभक्ति से अभेदभक्ति की ओर प्रस्थान निजस्वरूपलीनता की सिद्धि-साधक वीतरागभक्ति (भेदभक्ति) का अवलम्बन (वीतराग प्रभु के वचनरूप, शरीररूप या निराकारपदस्वप) इसलिए बताया गया था कि आत्म-स्वरूपलीनता में रुकावटें डालने वाले पूर्वोक्त प्रतिबन्ध एवं स्वच्छन्दता को रोकने के लिए वीतराग वचनों पर श्रद्धा रखकर उनके अनुसरणरूप समर्पणता (जिनाज्ञाधीनता) आवश्यक बताई। परन्तु इस समर्पणभक्ति में भेदभावना की प्रतीति होती है, उसी अवलम्बन में ही अटक जाने की प्रतिवन्धता को रोकने के लिए अभेदभक्ति आवश्यक है। अभेदभक्ति से जिनस्वरूप ही मेरा स्वरूप है, मैं ही अर्हत्स्वरूप हूँ, सिद्ध-स्वरूप हूँ, इस प्रकार की दृढ़ प्रतीति हो जायेगी। फिर स्वरूप दृष्ट्या एकता होने से 'मैं तू' की भेददृष्टि नहीं रहेगी। जो कुछ पाना है, वह मेरे में ही है, जहाँ पहुँचना है, वहाँ मुझे ही और मेरे ही स्थान में पहुँचना है, इस प्रकार की पूर्ण अभेदभक्तिभावना से सर्वपुरुषार्थ-आत्म-स्वरूप में अवस्थितिरूप होगा, निजस्वरूपलीनता की यह पूर्णता होगी; यही निजस्वरूपलीनता की शुद्ध प्रक्रिया होगी। यह छठे गुणस्थान तक के निर्ग्रन्थता का क्रमारोहण है। मुक्ति के अप्रमत्तताभ्यास के सोपान
सप्तम सोपान : अप्रमत्तता तथा अप्रतिबद्धता का अभ्यास-शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श: इन पंचेन्द्रिय-विषयों के प्रति राग और द्वेष-आसक्ति और घृणा-अरुचि, इन दोनों का अभाव रहे, यानी मनोज्ञ-अमनोज्ञ दोनों ही परिस्थितियों पर समभाव-माध्यस्थ्यभाव रहे तथा पंचविध प्रमाद से मनःस्थिति क्षुब्ध, विचलित या कषाय-नोकषायलिप्त न हो, त्रिविधयोगप्रवृत्ति सिर्फ उदयभाव के अधीन होकर हो, उसमें किसी प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल या भाव का प्रतिबन्ध (बन्धनबद्धता) न हो, न ही किसी प्रकार की फलाकांक्षा हो। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक प्रवृत्ति में निर्लोभता, समता, आशा-स्पृहा-रहितता हो। अप्रमत्तभाव से ऐसी सुदृढ़ परिपक्व साधना हो, भेदभक्ति से अभेदभक्ति की ओर बढ़ने पर साधक की अप्रमत्तताभ्यास की ऐसी ही स्वरूपदशा होती है। छठे गुणस्थानवर्ती साधक ने सर्व प्रकार से सब पदार्थों से मूर्छावृत्ति हटाकर सर्वसंपत्करी भिक्षावृत्ति से प्राप्त साधन में आत्मभाव खोये बिना यथालाभ सन्तोष माना। किन्तु अत्यावश्यक साधन मनोज्ञ-अमनोज्ञ, जैसे भी प्राप्त हुए हों. उनमें उसका समभाव-माध्यस्थ्यभाव या ज्ञाता-द्रष्टाभाव टिका रहना चाहिए। उन प्राप्त साधनों या प्राप्त शरीरादि के प्रति राग-द्वेष, आसक्ति-घृणा, मोह-द्रोह अथवा गौरवभावना या हीनभावना (गर्व या दैन्य) न हो। यहीं से सप्तम गुणस्थानवर्ती अप्रमत्तताभ्यासी की साधना शुरू हो जाती है। आगे विश्लेषण करके बताया गया है कि पाँचों इन्द्रियों के अच्छे-बुरे, मनोज्ञ-अमनोज्ञ विषयों के प्राप्त होने पर कैसे-कैसे अहंकारवृत्ति या ईर्ष्या-द्वेषवृत्ति आ जाती है; मध्यस्थता या समता कैसे-कैसे चौपट हो जाती है? अतः इस प्रकार राग-द्वेष-विरहितता, समता या
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org