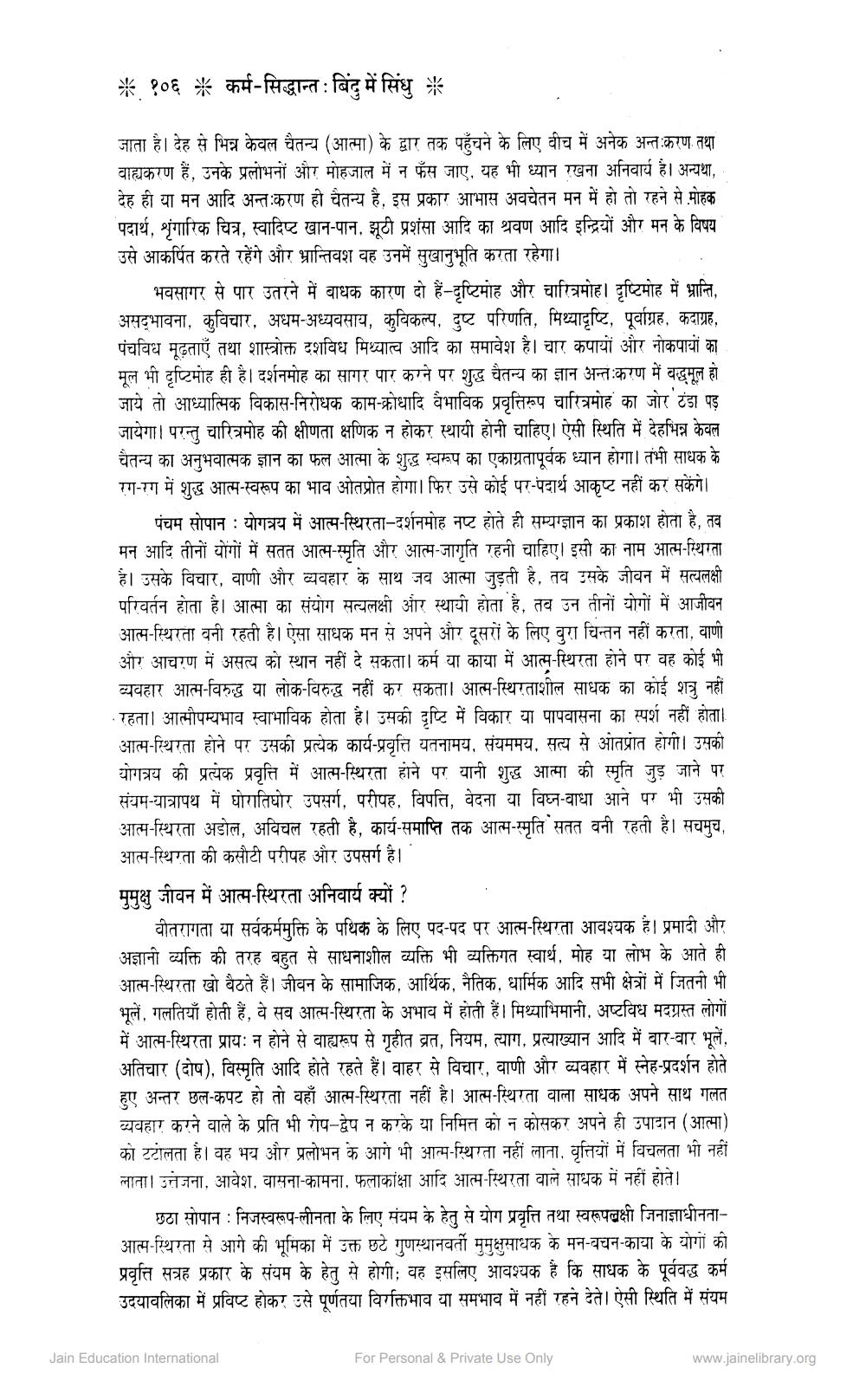________________
* १०६ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
जाता है। देह से भिन्न केवल चैतन्य (आत्मा) के द्वार तक पहुँचने के लिए वीच में अनेक अन्तःकरण तथा वाह्यकरण हैं, उनके प्रलोभनों और मोहजाल में न फँस जाए, यह भी ध्यान रखना अनिवार्य है। अन्यथा, देह ही या मन आदि अन्तःकरण हो चैतन्य है. इस प्रकार आभास अवचेतन मन में हो तो रहने से मोहक पदार्थ, शृंगारिक चित्र, स्वादिष्ट खान-पान, झूठी प्रशंसा आदि का श्रवण आदि इन्द्रियों और मन के विषय उसे आकर्पित करते रहेंगे और भ्रान्तिवश वह उनमें सुखानुभूति करता रहेगा।
__ भवसागर से पार उतरने में बाधक कारण दो हैं-दृष्टिमाह और चारित्रमोह। दृष्टिमोह में भ्रान्ति, असद्भावना, कुविचार, अधम-अध्यवसाय, कुविकल्प, दुष्ट परिणति, मिथ्यादृष्टि, पूर्वाग्रह, कदाग्रह, पंचविध मूढ़ताएँ तथा शास्त्रोक्त दशविध मिथ्यात्व आदि का समावेश है। चार कपायों और नोकपायों का मूल भी दृष्टिमाह ही है। दर्शनमोह का सागर पार करने पर शुद्ध चैतन्य का ज्ञान अन्तःकरण में बद्धमूल हो जाये तो आध्यात्मिक विकास-निरोधक काम-क्रोधादि वैभाविक प्रवृत्तिरूप चारित्रमोह का जोर टंडा पड़ जायेगा। परन्तु चारित्रमोह की क्षीणता क्षणिक न होकर स्थायी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देहभिन्न केवल चैतन्य का अनुभवात्मक ज्ञान का फल आत्मा के शुद्ध स्वरूप का एकाग्रतापूर्वक ध्यान होगा। तभी साधक के रग-रग में शुद्ध आत्म-स्वरूप का भाव ओतप्रोत होगा। फिर उसे कोई पर-पदार्थ आकृष्ट नहीं कर सकेंगे।
पंचम सोपान : योगत्रय में आत्म-स्थिरता-दर्शनमोह नष्ट होते ही सम्यग्ज्ञान का प्रकाश होता है, तब मन आदि तीनों योगों में सतत आत्म-स्मृति और आत्म-जागृति रहनी चाहिए। इसी का नाम आत्म-स्थिरता है। उसके विचार, वाणी और व्यवहार के साथ जब आत्मा जुड़ती है, तब उसके जीवन में सत्यलक्षी परिवर्तन होता है। आत्मा का संयोग सत्यलक्षी और स्थायी होता है, तब उन तीनों योगों में आजीवन आत्म-स्थिरता बनी रहती है। ऐसा साधक मन से अपने और दूसरों के लिए बुरा चिन्तन नहीं करता, वाणी और आचरण में असत्य को स्थान नहीं दे सकता। कर्म या काया में आत्म-स्थिरता होने पर वह कोई भी व्यवहार आत्म-विरुद्ध या लोक-विरुद्ध नहीं कर सकता। आत्म-स्थिरताशील साधक का कोई शत्रु नहीं रहता। आत्मौपम्यभाव स्वाभाविक होता है। उसकी दृष्टि में विकार या पापवासना का स्पर्श नहीं होता।
आत्म-स्थिरता होने पर उसकी प्रत्येक कार्य-प्रवृत्ति यतनामय, संयममय, सत्य से ओतप्रोत होगी। उसकी योगत्रय की प्रत्येक प्रवृत्ति में आत्म-स्थिरता होने पर यानी शुद्ध आत्मा की स्मृति जुड़ जाने पर संयम-यात्रापथ में घोरातिघोर उपसर्ग, परीपह, विपत्ति, वेदना या विघ्न-बाधा आने पर भी उसकी आत्म-स्थिरता अडोल, अविचल रहती है, कार्य-समाप्ति तक आत्म-स्मृति सतत बनी रहती है। सचमुच, आत्म-स्थिरता की कसौटी परीपह और उपसर्ग है। मुमुक्षु जीवन में आत्म-स्थिरता अनिवार्य क्यों ?
वीतरागता या सर्वकर्ममुक्ति के पथिक के लिए पद-पद पर आत्म-स्थिरता आवश्यक है। प्रमादी और अज्ञानी व्यक्ति की तरह बहुत से साधनाशील व्यक्ति भी व्यक्तिगत स्वार्थ, मोह या लोभ के आते ही आत्म-स्थिरता खो बैठते हैं। जीवन के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में जितनी भी भूलें, गलतियाँ होती हैं, वे सब आत्म-स्थिरता के अभाव में होती हैं। मिथ्याभिमानी, अष्टविध मदग्रस्त लोगों में आत्म-स्थिरता प्रायः न होने से वाह्यरूप से गृहीत व्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान आदि में बार-बार भूलें, अतिचार (दोष), विस्मृति आदि होते रहते हैं। वाहर से विचार, वाणी और व्यवहार में स्नेह-प्रदर्शन होते हुए अन्तर छल-कपट हो तो वहाँ आत्म-स्थिरता नहीं है। आत्म-स्थिरता वाला साधक अपने साथ गलत व्यवहार करने वाले के प्रति भी रोप-द्वेप न करके या निमित्त को न कोसकर अपने ही उपादान (आत्मा) को टटोलता है। वह भय और प्रलोभन के आगे भी आत्म-स्थिरता नहीं लाता, वृत्तियों में विचलता भी नहीं लाता। उत्तेजना, आवेश. वासना-कामना. फलाकांक्षा आदि आत्म-स्थिरता वाले साधक में नहीं होते।
छठा सोपान : निजस्वरूप-लीनता के लिए संयम के हेतु से योग प्रवृत्ति तथा स्वरूपलक्षी जिनाज्ञाधीनताआत्म-स्थिरता से आगे की भमिका में उक्त छटे गणस्थानवी ममक्षसाधक के मन-वचन-काया के योगों की प्रवृत्ति सत्रह प्रकार के संयम के हेतु से होगी; वह इसलिए आवश्यक है कि साधक के पूर्ववद्ध कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट होकर उसे पूर्णतया विरक्तिभाव या समभाव में नहीं रहने देते। ऐसी स्थिति में संयम
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org