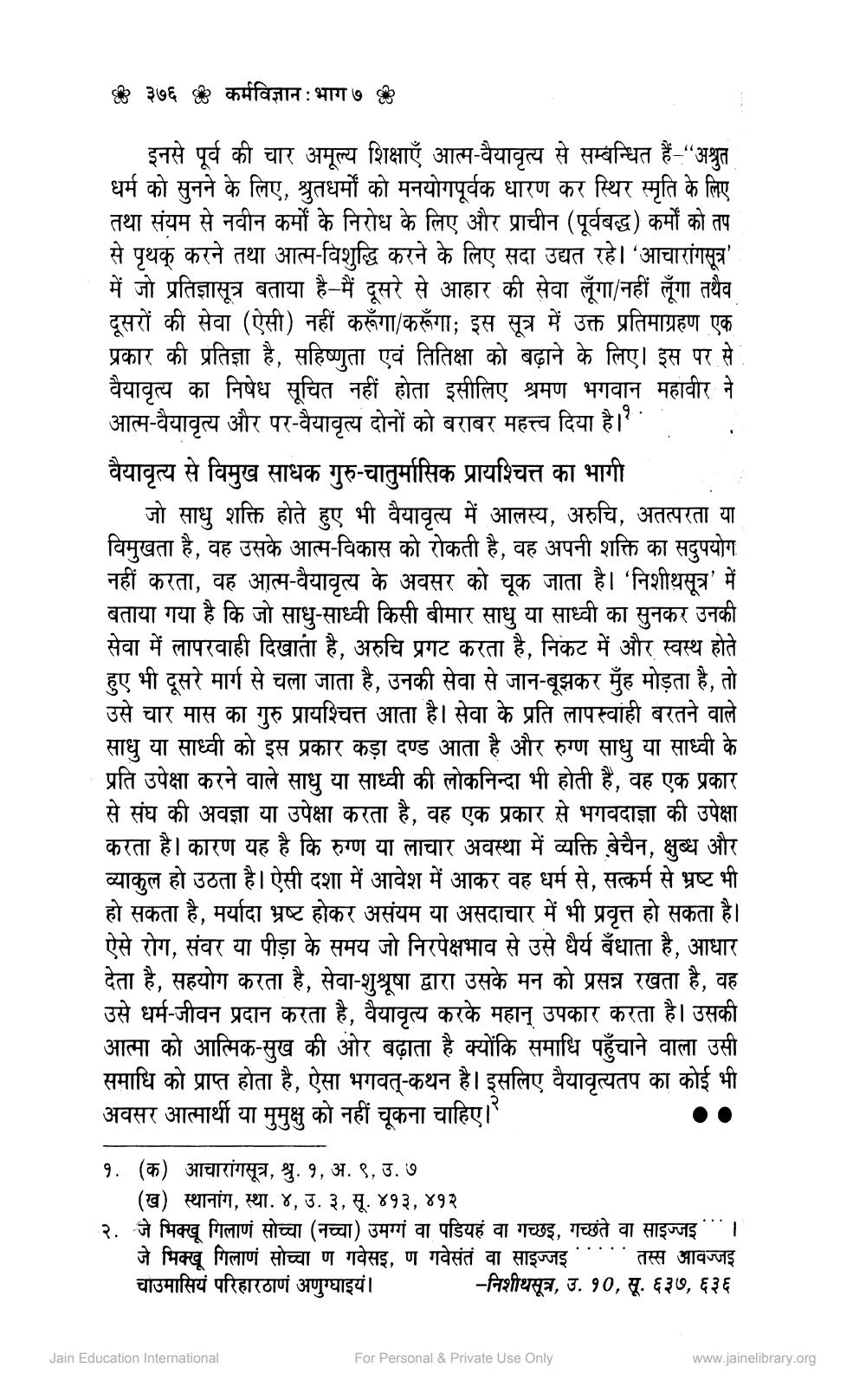________________
8 ३७६ ॐ कर्मविज्ञान : भाग ७ *
इनसे पूर्व की चार अमूल्य शिक्षाएँ आत्म-वैयावृत्य से सम्बन्धित हैं-“अश्रुत धर्म को सुनने के लिए, श्रुतधर्मों को मनयोगपूर्वक धारण कर स्थिर स्मृति के लिए तथा संयम से नवीन कर्मों के निरोध के लिए और प्राचीन (पूर्वबद्ध) कर्मों को तप से पृथक् करने तथा आत्म-विशुद्धि करने के लिए सदा उद्यत रहे। 'आचारांगसूत्र' में जो प्रतिज्ञासूत्र बताया है-मैं दूसरे से आहार की सेवा लूँगा/नहीं लूंगा तथैव दूसरों की सेवा (ऐसी) नहीं करूँगा/करूँगा; इस सूत्र में उक्त प्रतिमाग्रहण एक प्रकार की प्रतिज्ञा है, सहिष्णुता एवं तितिक्षा को बढ़ाने के लिए। इस पर से वैयावृत्य का निषेध सूचित नहीं होता इसीलिए श्रमण भगवान महावीर ने आत्म-वैयावृत्य और पर-वैयावृत्य दोनों को बराबर महत्त्व दिया है।' वैयावृत्य से विमुख साधक गुरु-चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का भागी __ जो साधु शक्ति होते हुए भी वैयावृत्य में आलस्य, अरुचि, अतत्परता या विमुखता है, वह उसके आत्म-विकास को रोकती है, वह अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं करता, वह आत्म-वैयावृत्य के अवसर को चूक जाता है। 'निशीथसूत्र' में बताया गया है कि जो साधु-साध्वी किसी बीमार साधु या साध्वी का सुनकर उनकी सेवा में लापरवाही दिखाता है, अरुचि प्रगट करता है, निकट में और स्वस्थ होते हुए भी दूसरे मार्ग से चला जाता है, उनकी सेवा से जान-बूझकर मुँह मोड़ता है, तो उसे चार मास का गुरु प्रायश्चित्त आता है। सेवा के प्रति लापस्वाही बरतने वाले साधु या साध्वी को इस प्रकार कड़ा दण्ड आता है और रुग्ण साधु या साध्वी के प्रति उपेक्षा करने वाले साधु या साध्वी की लोकनिन्दा भी होती है, वह एक प्रकार से संघ की अवज्ञा या उपेक्षा करता है, वह एक प्रकार से भगवदाज्ञा की उपेक्षा करता है। कारण यह है कि रुग्ण या लाचार अवस्था में व्यक्ति बेचैन, क्षुब्ध और व्याकुल हो उठता है। ऐसी दशा में आवेश में आकर वह धर्म से, सत्कर्म से भ्रष्ट भी हो सकता है, मर्यादा भ्रष्ट होकर असंयम या असदाचार में भी प्रवृत्त हो सकता है। ऐसे रोग, संवर या पीड़ा के समय जो निरपेक्षभाव से उसे धैर्य बँधाता है, आधार देता है, सहयोग करता है, सेवा-शुश्रूषा द्वारा उसके मन को प्रसन्न रखता है, वह उसे धर्म-जीवन प्रदान करता है, वैयावृत्य करके महान् उपकार करता है। उसकी आत्मा को आत्मिक-सुख की ओर बढ़ाता है क्योंकि समाधि पहुँचाने वाला उसी समाधि को प्राप्त होता है, ऐसा भगवत्-कथन है। इसलिए वैयावृत्यतप का कोई भी अवसर आत्मार्थी या मुमुक्षु को नहीं चूकना चाहिए।
१. (क) आचारांगसूत्र, श्रु.१, अ. ९, उ. ७
(ख) स्थानांग, स्था. ४, उ. ३, सू. ४१३, ४१२ २. जे भिक्खू गिलाणं सोच्चा (नच्चा) उमग्गं वा पडियहं वा गच्छइ, गच्छंते वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू गिलाणं सोच्चा ण गवेसइ, ण गवसंतं वा साइज्जइ तस्स आवज्जइ चाउमासियं परिहारठाणं अणुग्घाइयं। -निशीथसूत्र, उ. १०, सू. ६३७, ६३६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org