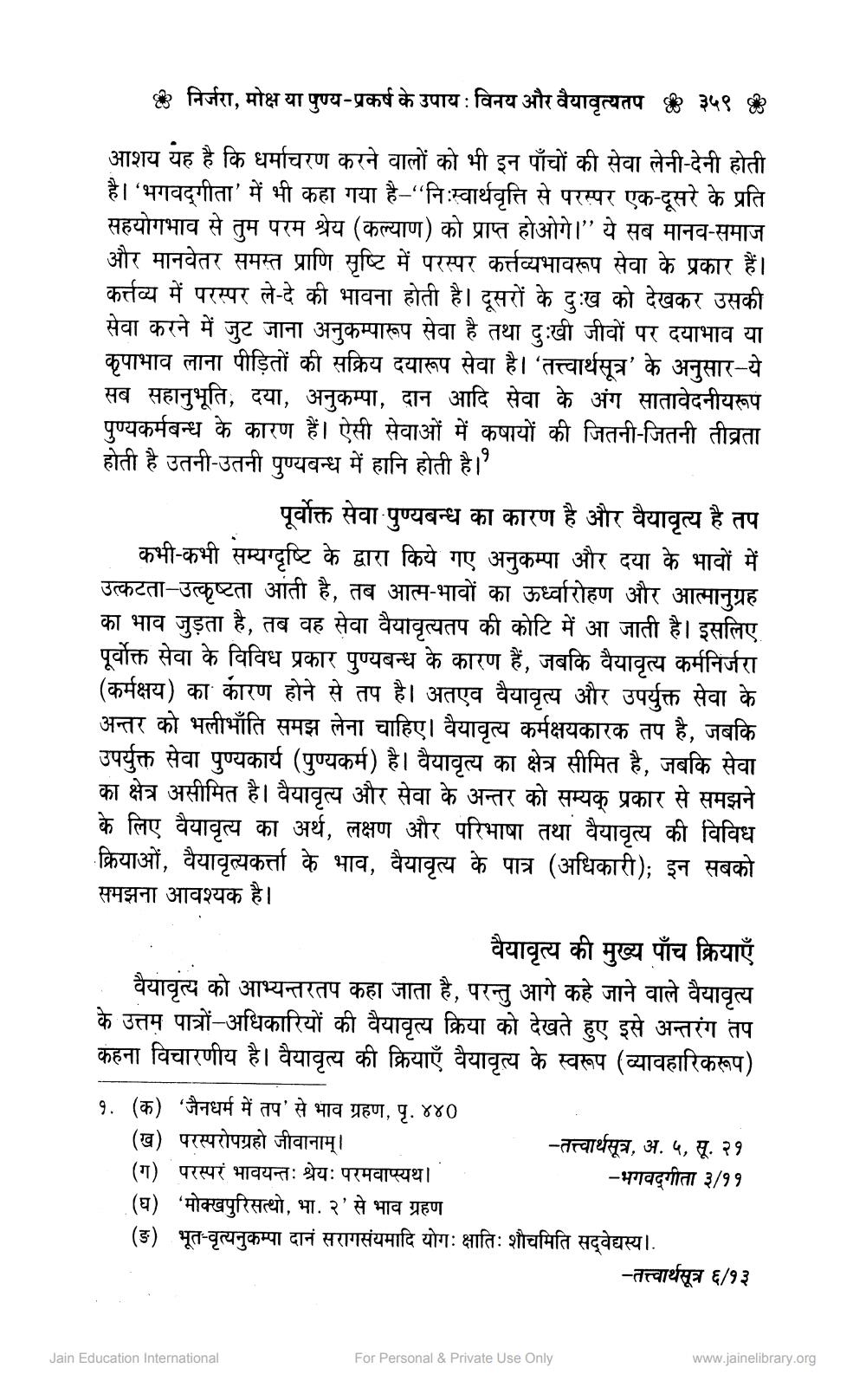________________
8 निर्जरा, मोक्ष या पुण्य-प्रकर्ष के उपाय : विनय और वैयावृत्यतप & ३५९ 8
आशय यह है कि धर्माचरण करने वालों को भी इन पाँचों की सेवा लेनी-देनी होती है। 'भगवद्गीता' में भी कहा गया है-“निःस्वार्थवृत्ति से परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहयोगभाव से तुम परम श्रेय (कल्याण) को प्राप्त होओगे।" ये सब मानव-समाज
और मानवेतर समस्त प्राणि सृष्टि में परस्पर कर्तव्यभावरूप सेवा के प्रकार हैं। कर्तव्य में परस्पर ले-दे की भावना होती है। दूसरों के दुःख को देखकर उसकी सेवा करने में जुट जाना अनुकम्पारूप सेवा है तथा दुःखी जीवों पर दयाभाव या कृपाभाव लाना पीड़ितों की सक्रिय दयारूप सेवा है। 'तत्त्वार्थसूत्र' के अनुसार-ये सब सहानुभूति, दया, अनुकम्पा, दान आदि सेवा के अंग सातावेदनीयरूप पुण्यकर्मबन्ध के कारण हैं। ऐसी सेवाओं में कषायों की जितनी-जितनी तीव्रता होती है उतनी-उतनी पुण्यबन्ध में हानि होती है।'
पूर्वोक्त सेवा पुण्यबन्ध का कारण है और वैयावृत्य है तप कभी-कभी सम्यग्दृष्टि के द्वारा किये गए अनुकम्पा और दया के भावों में उत्कटता-उत्कृष्टता आती है, तब आत्म-भावों का ऊर्ध्वारोहण और आत्मानुग्रह का भाव जुड़ता है, तब वह सेवा वैयावृत्यतप की कोटि में आ जाती है। इसलिए पूर्वोक्त सेवा के विविध प्रकार पुण्यबन्ध के कारण हैं, जबकि वैयावृत्य कर्मनिर्जरा (कर्मक्षय) का कारण होने से तप है। अतएव वैयावृत्य और उपर्युक्त सेवा के अन्तर को भलीभाँति समझ लेना चाहिए। वैयावृत्य कर्मक्षयकारक तप है, जबकि उपर्युक्त सेवा पुण्यकार्य (पुण्यकर्म) है। वैयावृत्य का क्षेत्र सीमित है, जबकि सेवा का क्षेत्र असीमित है। वैयावृत्य और सेवा के अन्तर को सम्यक् प्रकार से समझने के लिए वैयावृत्य का अर्थ, लक्षण और परिभाषा तथा वैयावृत्य की विविध क्रियाओं, वैयावृत्यकर्ता के भाव, वैयावृत्य के पात्र (अधिकारी); इन सबको समझना आवश्यक है।
वैयावृत्य की मुख्य पाँच क्रियाएँ वैयावृत्य को आभ्यन्तरतप कहा जाता है, परन्तु आगे कहे जाने वाले वैयावृत्य के उत्तम पात्रों-अधिकारियों की वैयावृत्य क्रिया को देखते हुए इसे अन्तरंग तप कहना विचारणीय है। वैयावृत्य की क्रियाएँ वैयावृत्य के स्वरूप (व्यावहारिकरूप) १. (क) 'जैनधर्म में तप' से भाव ग्रहण, पृ. ४४० (ख) परस्परोपग्रहो जीवानाम्।
-तत्त्वार्थसूत्र, अ. ५, सू. २१ (ग) परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।
-भगवद्गीता ३/११ (घ) 'मोक्खपुरिसत्थो, भा. २' से भाव ग्रहण (ङ) भूत-वृत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः क्षातिः शौचमिति सद्वेद्यस्य।.
-तत्त्वार्थसूत्र ६/१३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org