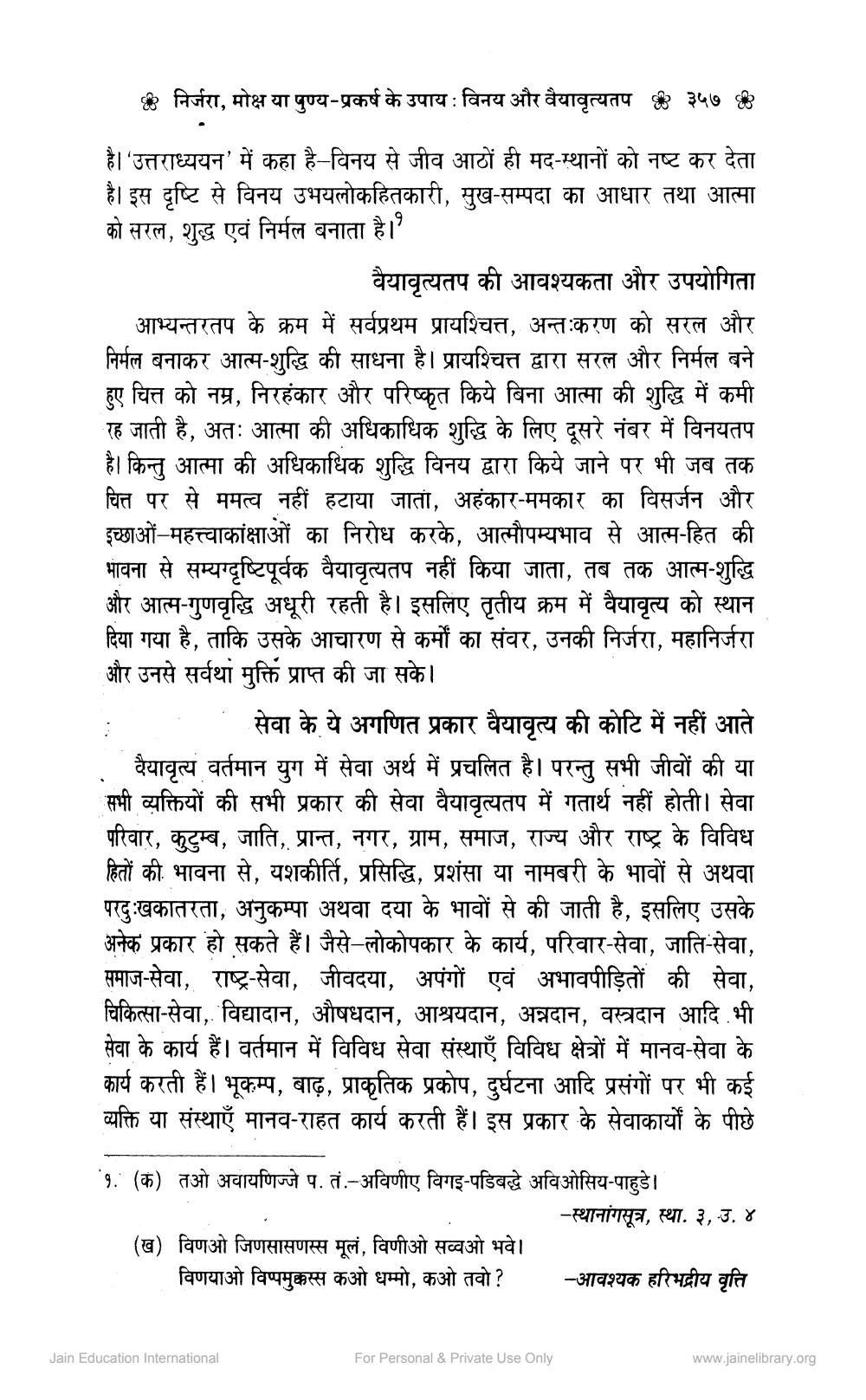________________
8 निर्जरा, मोक्ष या पुण्य-प्रकर्ष के उपाय : विनय और वैयावृत्यतप * ३५७ 8
है। 'उत्तराध्ययन' में कहा है-विनय से जीव आठों ही मद-स्थानों को नष्ट कर देता है। इस दृष्टि से विनय उभयलोकहितकारी, सुख-सम्पदा का आधार तथा आत्मा को सरल, शुद्ध एवं निर्मल बनाता है।'
वैयावृत्यतप की आवश्यकता और उपयोगिता आभ्यन्तरतप के क्रम में सर्वप्रथम प्रायश्चित्त, अन्तःकरण को सरल और निर्मल बनाकर आत्म-शुद्धि की साधना है। प्रायश्चित्त द्वारा सरल और निर्मल बने हुए चित्त को नम्र, निरहंकार और परिष्कृत किये बिना आत्मा की शुद्धि में कमी रह जाती है, अतः आत्मा की अधिकाधिक शुद्धि के लिए दूसरे नंबर में विनयतप है। किन्तु आत्मा की अधिकाधिक शुद्धि विनय द्वारा किये जाने पर भी जब तक चित्त पर से ममत्व नहीं हटाया जाता, अहंकार-ममकार का विसर्जन और इच्छाओं-महत्त्वाकांक्षाओं का निरोध करके, आत्मौपम्यभाव से आत्म-हित की भावना से सम्यग्दृष्टिपूर्वक वैयावृत्यतप नहीं किया जाता, तब तक आत्म-शुद्धि
और आत्म-गुणवृद्धि अधूरी रहती है। इसलिए तृतीय क्रम में वैयावृत्य को स्थान दिया गया है, ताकि उसके आचारण से कर्मों का संवर, उनकी निर्जरा, महानिर्जरा
और उनसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त की जा सके। : सेवा के ये अगणित प्रकार वैयावृत्य की कोटि में नहीं आते
वैयावृत्य वर्तमान युग में सेवा अर्थ में प्रचलित है। परन्तु सभी जीवों की या सभी व्यक्तियों की सभी प्रकार की सेवा वैयावृत्यतप में गतार्थ नहीं होती। सेवा परिवार, कुटुम्ब, जाति, प्रान्त, नगर, ग्राम, समाज, राज्य और राष्ट्र के विविध हितों की भावना से, यशकीर्ति, प्रसिद्धि, प्रशंसा या नामबरी के भावों से अथवा परदुःखकातरता, अनुकम्पा अथवा दया के भावों से की जाती है, इसलिए उसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे-लोकोपकार के कार्य, परिवार-सेवा, जाति-सेवा, समाज-सेवा, राष्ट्र-सेवा, जीवदया, अपंगों एवं अभावपीड़ितों की सेवा, चिकित्सा-सेवा, विद्यादान, औषधदान, आश्रयदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि भी सेवा के कार्य हैं। वर्तमान में विविध सेवा संस्थाएँ विविध क्षेत्रों में मानव-सेवा के कार्य करती हैं। भूकम्प, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना आदि प्रसंगों पर भी कई व्यक्ति या संस्थाएँ मानव-राहत कार्य करती हैं। इस प्रकार के सेवाकार्यों के पीछे
१. (क) तओ अवायणिज्जे प. तं.-अविणीए विगइ-पडिबद्धे अविओसिय-पाहुडे।
-स्थानांगसूत्र, स्था. ३, उ. ४ (ख) विणओ जिणसासणस्स मूलं, विणीओ सव्वओ भवे।
विणयाओ विप्पमुक्कस्स कओ धम्मो, कओ तवो? _ -आवश्यक हरिभद्रीय वृत्ति
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org