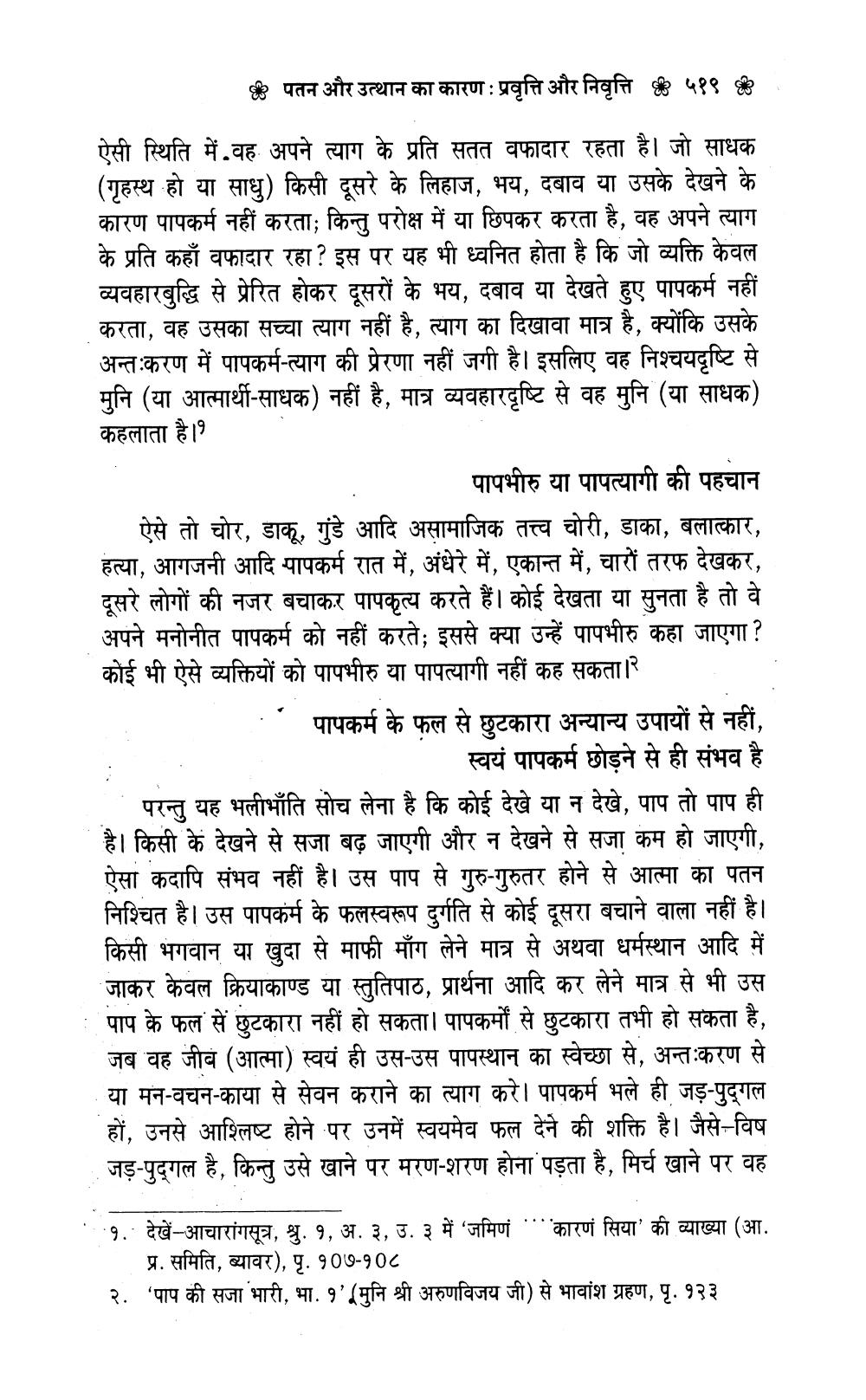________________
पतन और उत्थान का कारण: प्रवृत्ति और निवृत्ति ५१९
ऐसी स्थिति में वह अपने त्याग के प्रति सतत वफादार रहता है। जो साधक ( गृहस्थ हो या साधु) किसी दूसरे के लिहाज, भय, दबाव या उसके देखने के कारण पापकर्म नहीं करता; किन्तु परोक्ष में या छिपकर करता है, वह अपने त्याग के प्रति कहाँ वफादार रहा? इस पर यह भी ध्वनित होता है कि जो व्यक्ति केवल व्यवहारबुद्धि से प्रेरित होकर दूसरों के भय, दबाव या देखते हुए पापकर्म नहीं करता, वह उसका सच्चा त्याग नहीं है, त्याग का दिखावा मात्र है, क्योंकि उसके अन्तःकरण में पापकर्म-त्याग की प्रेरणा नहीं जगी है। इसलिए वह निश्चयदृष्टि से मुनि (या आत्मार्थी-साधक) नहीं है, मात्र व्यवहारदृष्टि से वह मुनि (या साधक) कहलाता है ।"
पापभीरु या पापत्यागी की पहचान
ऐसे तो चोर, डाकू, गुंडे आदि असामाजिक तत्त्व चोरी, डाका, बलात्कार, हत्या, आगजनी आदि पापकर्म रात में, अंधेरे में, एकान्त में, चारों तरफ देखकर, दूसरे लोगों की नजर बचाकर पापकृत्य करते हैं। कोई देखता या सुनता है तो वे अपने मनोनीत पापकर्म को नहीं करते; इससे क्या उन्हें पापभीरु कहा जाएगा ? कोई भी ऐसे व्यक्तियों को पापभीरु या पापत्यागी नहीं कह सकता । २
पापकर्म के फल से छुटकारा अन्यान्य उपायों से नहीं, स्वयं पापकर्म छोड़ने से ही संभव है
परन्तु यह भलीभाँति सोच लेना है कि कोई देखे या न देखे, पाप तो पाप ही है। किसी के देखने से सजा बढ़ जाएगी और न देखने से सजा कम हो जाएगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है । उस पाप से गुरु- गुरुतर होने से आत्मा का पतन निश्चित है। उस पापकर्म के फलस्वरूप दुर्गति से कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है । किसी भगवान या खुदा से माफी माँग लेने मात्र से अथवा धर्मस्थान आदि में जाकर केवल क्रियाकाण्ड या स्तुतिपाठ, प्रार्थना आदि कर लेने मात्र से भी उस पाप के फल से छुटकारा नहीं हो सकता । पापकर्मों से छुटकारा तभी हो सकता है, जब वह जीव (आत्मा) स्वयं ही उस उस पापस्थान का स्वेच्छा से, अन्तःकरण या मन-वचन-काया से सेवन कराने का त्याग करे । पापकर्म भले ही जड़-पुद्गल हों, उनसे आश्लिष्ट होने पर उनमें स्वयमेव फल देने की शक्ति है । जैसे- विष जड़-पुद्गल है, किन्तु उसे खाने पर मरण-शरण होना पड़ता है, मिर्च खाने पर वह
१. देखें - आचारांगसूत्र, श्रु. १, अ. ३, उ. ३ में 'जमिणं 'कारणं सिया' की व्याख्या (आ. प्र. समिति, ब्यावर ), पृ. १०७-१०८
२.
'पाप की सजा भारी, भा. १' (मुनि श्री अरुणविजय जी) से भावांश ग्रहण, पृ. १२३