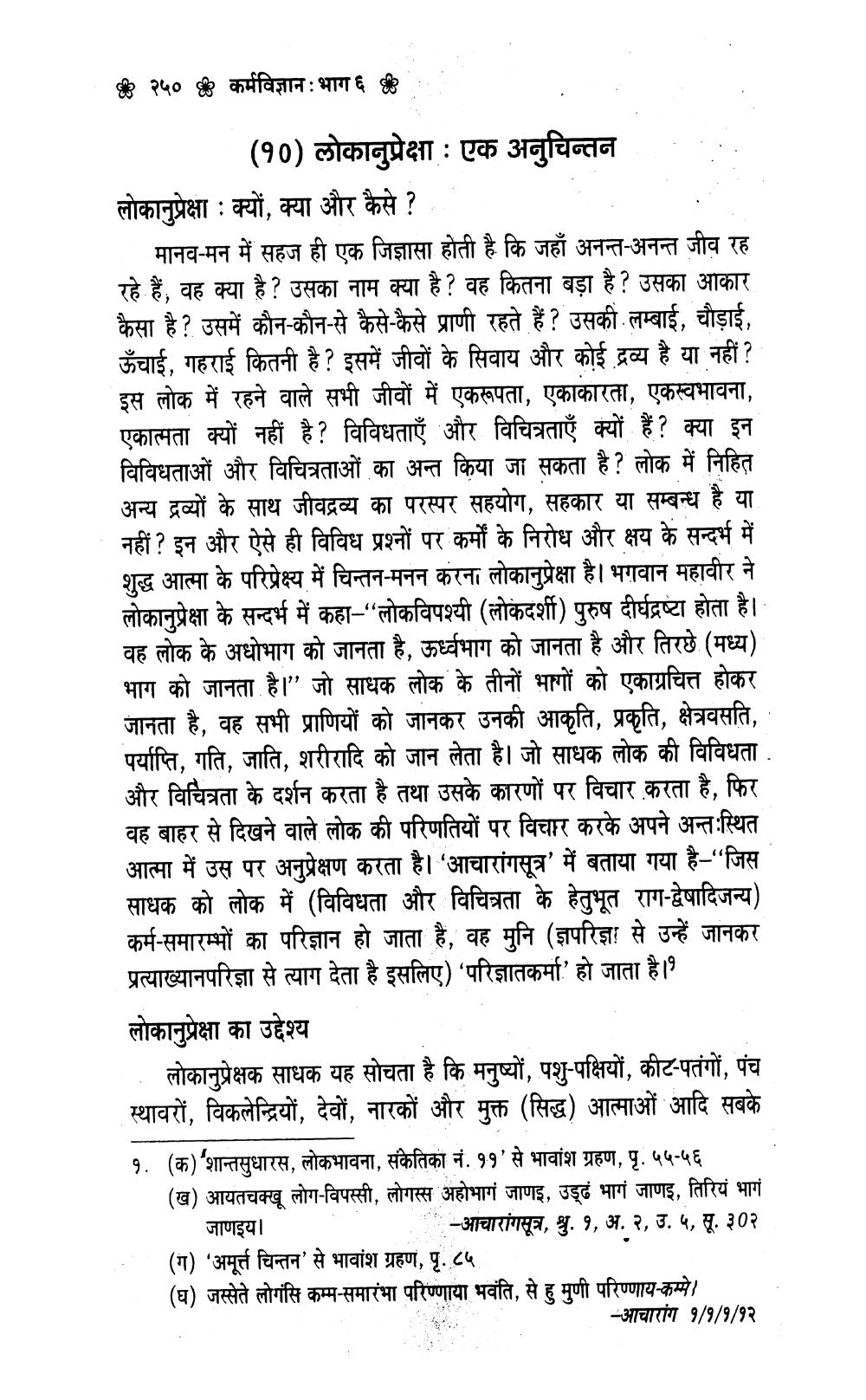________________
* २५० * कर्मविज्ञान : भाग ६ ॐ
(१०) लोकानुप्रेक्षा : एक अनुचिन्तन । लोकानुप्रेक्षा : क्यों, क्या और कैसे ? ____ मानव-मन में सहज ही एक जिज्ञासा होती है कि जहाँ अनन्त-अनन्त जीव रह रहे हैं, वह क्या है? उसका नाम क्या है? वह कितना बड़ा है ? उसका आकार कैसा है? उसमें कौन-कौन-से कैसे-कैसे प्राणी रहते हैं ? उसकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, गहराई कितनी है ? इसमें जीवों के सिवाय और कोई द्रव्य है या नहीं? इस लोक में रहने वाले सभी जीवों में एकरूपता, एकाकारता, एकस्वभावना, एकात्मता क्यों नहीं है? विविधताएँ और विचित्रताएँ क्यों हैं? क्या इन विविधताओं और विचित्रताओं का अन्त किया जा सकता है? लोक में निहित अन्य द्रव्यों के साथ जीवद्रव्य का परस्पर सहयोग, सहकार या सम्बन्ध है या नहीं? इन और ऐसे ही विविध प्रश्नों पर कर्मों के निरोध और क्षय के सन्दर्भ में शुद्ध आत्मा के परिप्रेक्ष्य में चिन्तन-मनन करना लोकानप्रेक्षा है। भगवान महावीर ने लोकानुप्रेक्षा के सन्दर्भ में कहा-“लोकविपश्यी (लोकदर्शी) पुरुष दीर्घद्रष्टा होता है। वह लोक के अधोभाग को जानता है, ऊर्ध्वभाग को जानता है और तिरछे (मध्य) भाग को जानता है।" जो साधक लोक के तीनों भागों को एकाग्रचित्त होकर जानता है, वह सभी प्राणियों को जानकर उनकी आकृति, प्रकृति, क्षेत्रवसति, ' पर्याप्ति, गति, जाति, शरीरादि को जान लेता है। जो साधक लोक की विविधता और विचित्रता के दर्शन करता है तथा उसके कारणों पर विचार करता है, फिर वह बाहर से दिखने वाले लोक की परिणतियों पर विचार करके अपने अन्तःस्थित आत्मा में उस पर अनुप्रेक्षण करता है। 'आचारांगसूत्र' में बताया गया है-"जिस साधक को लोक में (विविधता और विचित्रता के हेतुभूत राग-द्वेषादिजन्य) कर्म-समारम्भों का परिज्ञान हो जाता है, वह मुनि (ज्ञपरिज्ञा से उन्हें जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग देता है इसलिए) परिज्ञातकर्मा' हो जाता है। लोकानुप्रेक्षा का उद्देश्य . लोकानुप्रेक्षक साधक यह सोचता है कि मनुष्यों, पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों, पंच स्थावरों, विकलेन्द्रियों, देवों, नारकों और मुक्त (सिद्ध) आत्माओं आदि सबके १. (क) शान्तसुधारस, लोकभावना, संकेतिका नं. ११' से भावांश ग्रहण, पृ. ५५-५६ (ख) आयतचक्खू लोग-विपस्सी, लोगस्स अहोभागं जाणइ, उड्ढं भागं जाणइ, तिरियं भागं जाणइय।
-आचारांगसूत्र, श्रु. १, अ. २, उ. ५, सू. ३०२ (ग) 'अमूर्त चिन्तन' से भावांश ग्रहण, पृ. ८५ (घ) जस्सेते लोगंसि कम्म-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी परिण्णाय-कम्मे।
-आचारांग १/१/१/१२