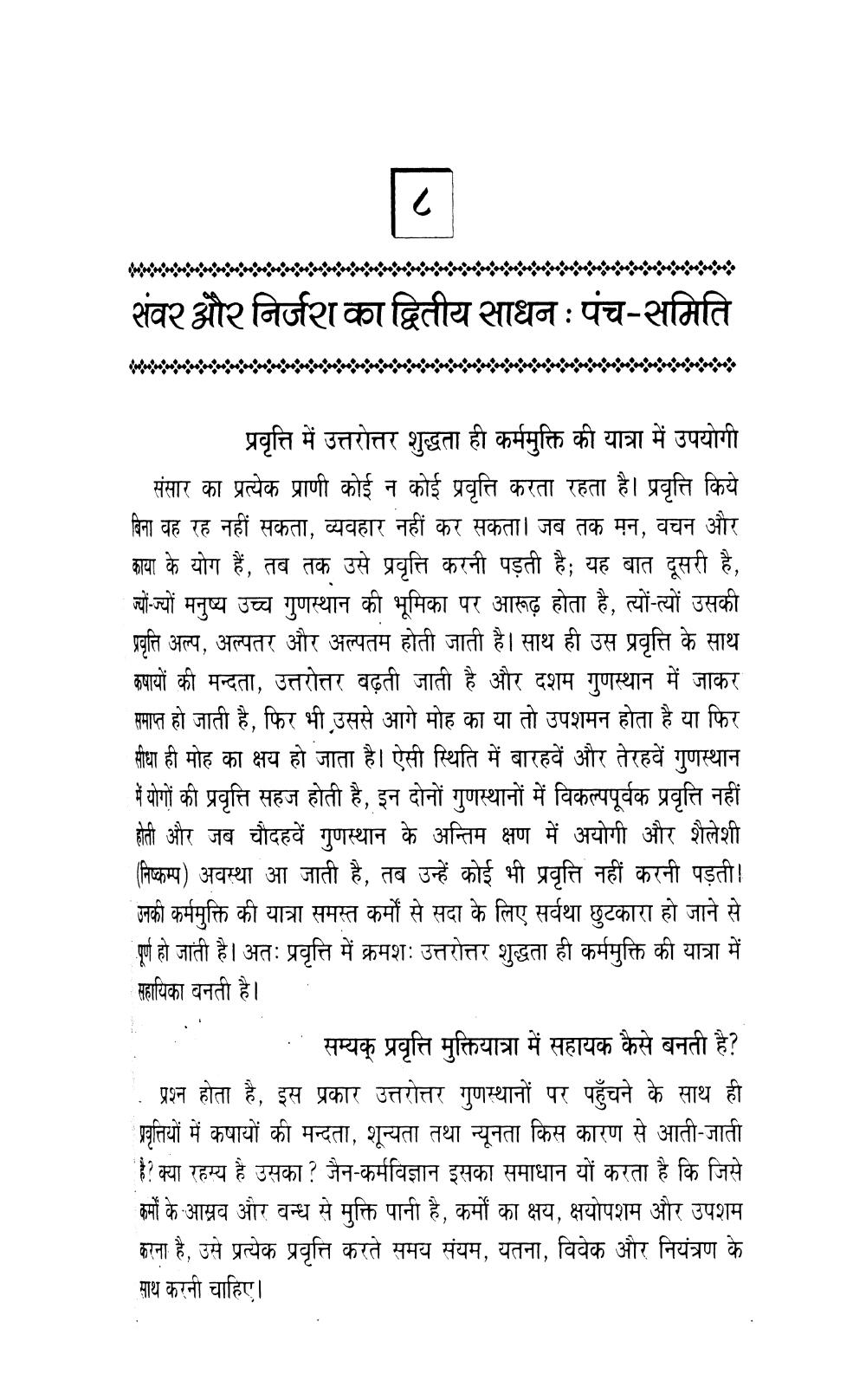________________
८
संवर और निर्जश का द्वितीय साधन : पंच-समिति
प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर शुद्धता ही कर्ममुक्ति की यात्रा में उपयोगी
संसार का प्रत्येक प्राणी कोई न कोई प्रवृत्ति करता रहता है। प्रवृत्ति किये बिना वह रह नहीं सकता, व्यवहार नहीं कर सकता। जब तक मन, वचन और काया के योग हैं, तब तक उसे प्रवृत्ति करनी पड़ती है; यह बात दूसरी है, ज्यों-ज्यों मनुष्य उच्च गुणस्थान की भूमिका पर आरूढ़ होता है, त्यों-त्यों उसकी प्रवृत्ति अल्प, अल्पतर और अल्पतम होती जाती है। साथ ही उस प्रवृत्ति के साथ कषायों की मन्दता, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और दशम गुणस्थान में जाकर समाप्त हो जाती है, फिर भी उससे आगे मोह का या तो उपशमन होता है या फिर सीधा ही मोह का क्षय हो जाता है। ऐसी स्थिति में बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में योगों की प्रवृत्ति सहज होती है, इन दोनों गुणस्थानों में विकल्पपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती और जब चौदहवें गुणस्थान के अन्तिम क्षण में अयोगी और शैलेशी (निष्कम्प) अवस्था आ जाती है, तब उन्हें कोई भी प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती। उनकी कर्ममुक्ति की यात्रा समस्त कर्मों से सदा के लिए सर्वथा छुटकारा हो जाने से पूर्ण हो जाती है। अतः प्रवृत्ति में क्रमशः उत्तरोत्तर शुद्धता ही कर्ममुक्ति की यात्रा में सहायिका बनती है।
सम्यक् प्रवृत्ति मुक्तियात्रा में सहायक कैसे बनती है?
प्रश्न होता है, इस प्रकार उत्तरोत्तर गुणस्थानों पर पहुँचने के साथ ही प्रवृत्तियों में कषायों की मन्दता, शून्यता तथा न्यूनता किस कारण से आती-जाती है? क्या रहस्य है उसका ? जैन- कर्मविज्ञान इसका समाधान यों करता है कि जिसे
कर्मों के आम्रव और बन्ध से मुक्ति पानी है, कर्मों का क्षय, क्षयोपशम और उपशम करना है, उसे प्रत्येक प्रवृत्ति करते समय संयम, यतना, विवेक और नियंत्रण के साथ करनी चाहिए।