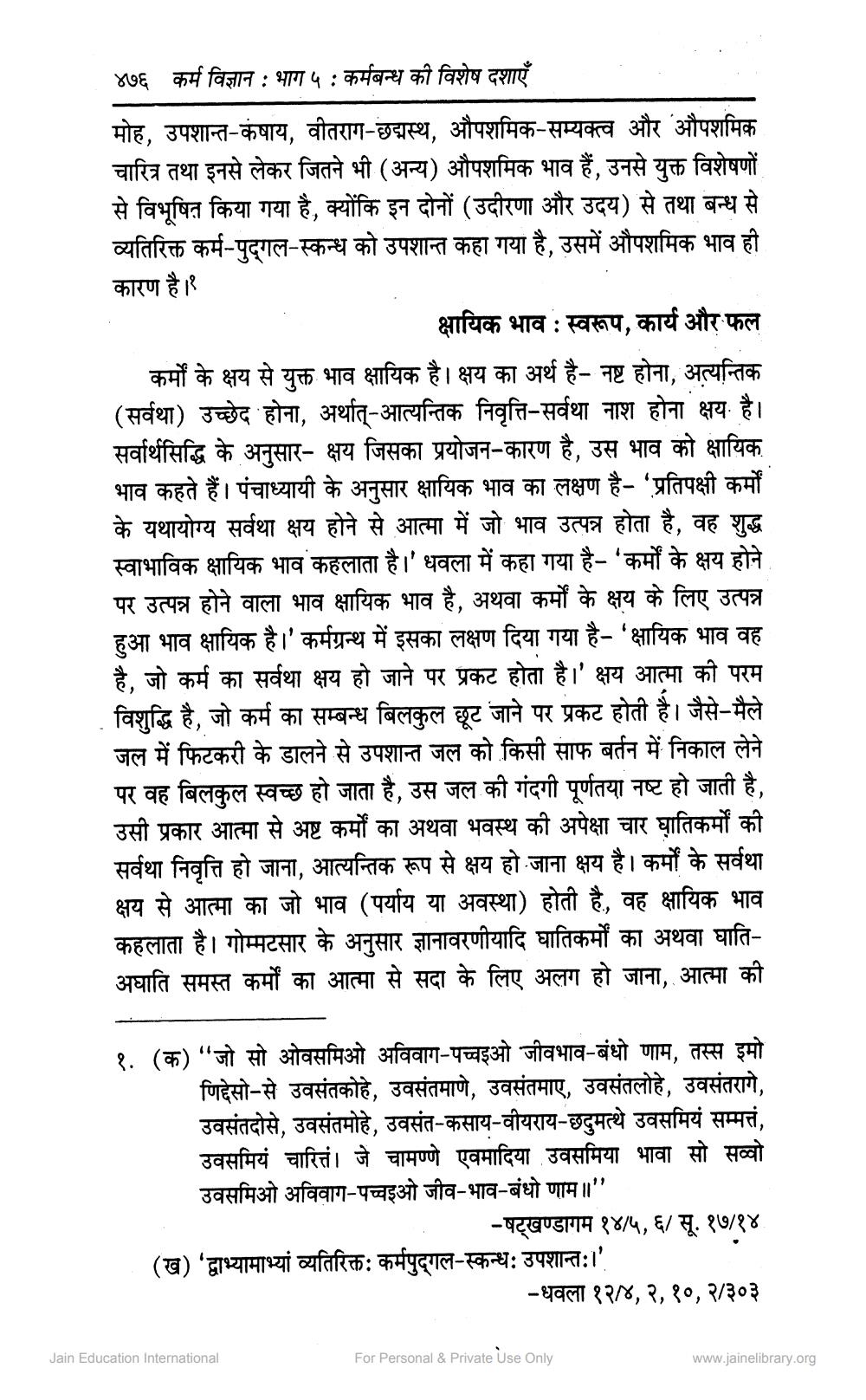________________
४७६ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ मोह, उपशान्त-कषाय, वीतराग-छद्मस्थ, औपशमिक-सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र तथा इनसे लेकर जितने भी (अन्य) औपशमिक भाव हैं, उनसे युक्त विशेषणों से विभूषित किया गया है, क्योंकि इन दोनों (उदीरणा और उदय) से तथा बन्ध से व्यतिरिक्त कर्म-पुद्गल-स्कन्ध को उपशान्त कहा गया है, उसमें औपशमिक भाव ही कारण है।
क्षायिक भाव : स्वरूप, कार्य और फल कर्मों के क्षय से युक्त भाव क्षायिक है। क्षय का अर्थ है- नष्ट होना, अत्यन्तिक (सर्वथा) उच्छेद होना, अर्थात्-आत्यन्तिक निवृत्ति-सर्वथा नाश होना क्षय है। सर्वार्थसिद्धि के अनुसार- क्षय जिसका प्रयोजन-कारण है, उस भाव को क्षायिक भाव कहते हैं। पंचाध्यायी के अनुसार क्षायिक भाव का लक्षण है- 'प्रतिपक्षी कर्मों के यथायोग्य सर्वथा क्षय होने से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होता है, वह शुद्ध स्वाभाविक क्षायिक भाव कहलाता है।' धवला में कहा गया है- 'कर्मों के क्षय होने पर उत्पन्न होने वाला भाव क्षायिक भाव है, अथवा कर्मों के क्षय के लिए उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक है।' कर्मग्रन्थ में इसका लक्षण दिया गया है- 'क्षायिक भाव वह है, जो कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने पर प्रकट होता है।' क्षय आत्मा की परम विशुद्धि है, जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर प्रकट होती है। जैसे-मैले जल में फिटकरी के डालने से उपशान्त जल को किसी साफ बर्तन में निकाल लेने पर वह बिलकुल स्वच्छ हो जाता है, उस जल की गंदगी पूर्णतया नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा से अष्ट कर्मों का अथवा भवस्थ की अपेक्षा चार घातिकर्मों की सर्वथा निवृत्ति हो जाना, आत्यन्तिक रूप से क्षय हो जाना क्षय है। कर्मों के सर्वथा क्षय से आत्मा का जो भाव (पर्याय या अवस्था) होती है, वह क्षायिक भाव कहलाता है। गोम्मटसार के अनुसार ज्ञानावरणीयादि घातिकर्मों का अथवा घातिअघाति समस्त कर्मों का आत्मा से सदा के लिए अलग हो जाना, आत्मा की
१. (क) "जो सो ओवसमिओ अविवाग-पच्चइओ जीवभाव-बंधो णाम, तस्स इमो
णिद्देसो-से उवसंतकोहे, उवसंतमाणे, उवसंतमाए, उवसंतलोहे, उवसंतरागे, उवसंतदोसे, उवसंतमोहे, उवसंत-कसाय-वीयराय-छदुमत्थे उवसमियं सम्मत्तं, उवसमियं चारित्तं। जे चामण्णे एवमादिया उवसमिया भावा सो सव्वो उवसमिओ अविवाग-पच्चइओ जीव-भाव-बंधो णाम॥"
. -षटखण्डागम १४/५, ६/ सू. १७/१४ (ख) 'द्वाभ्यामाभ्यां व्यतिरिक्तः कर्मपुद्गल-स्कन्धः उपशान्तः।'
-धवला १२/४, २, १०, २/३०३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org