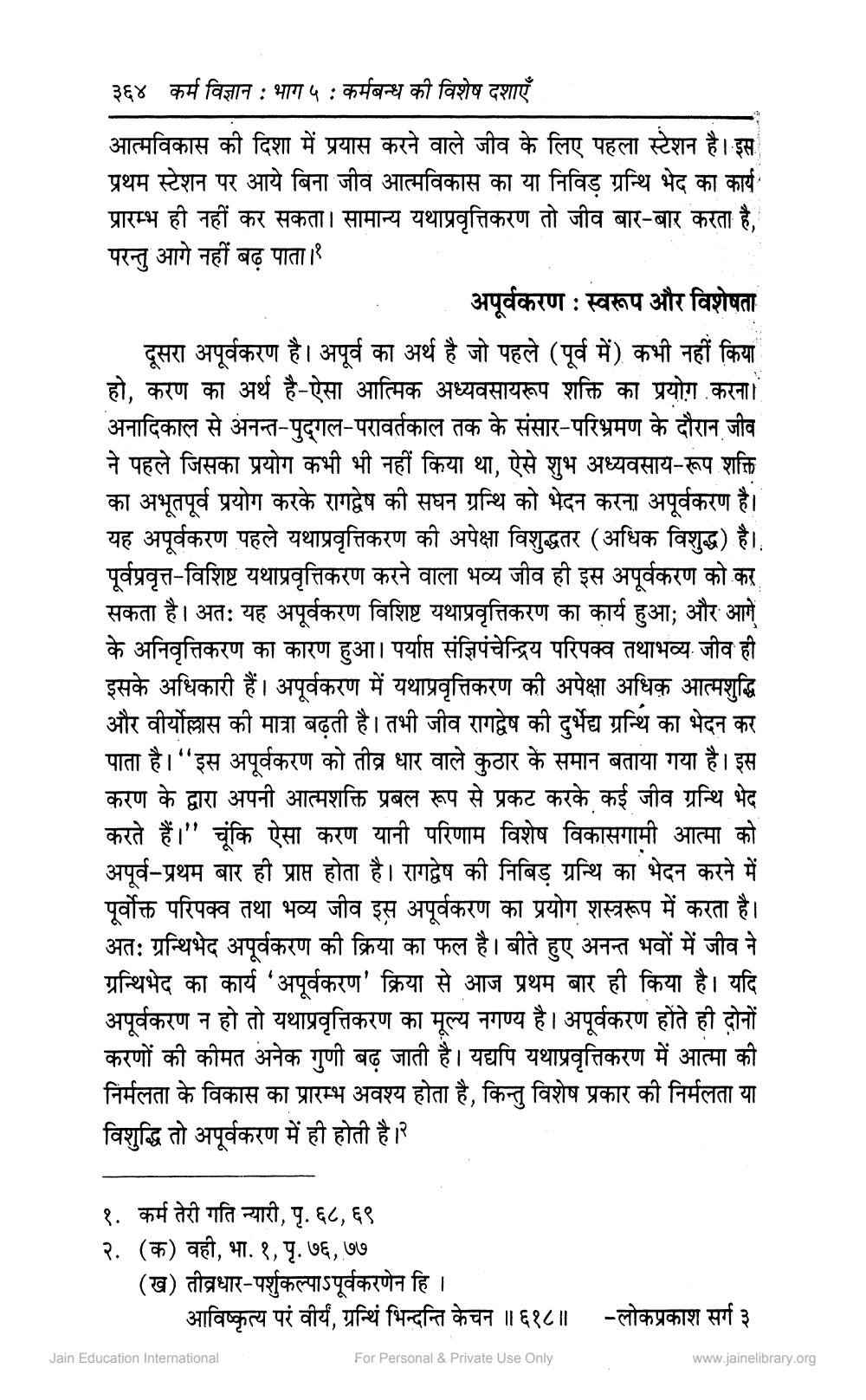________________
३६४ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ आत्मविकास की दिशा में प्रयास करने वाले जीव के लिए पहला स्टेशन है। इस प्रथम स्टेशन पर आये बिना जीव आत्मविकास का या निविड़ ग्रन्थि भेद का कार्य प्रारम्भ ही नहीं कर सकता। सामान्य यथाप्रवृत्तिकरण तो जीव बार-बार करता है, परन्तु आगे नहीं बढ़ पाता।
. अपूर्वकरण : स्वरूप और विशेषता दूसरा अपूर्वकरण है। अपूर्व का अर्थ है जो पहले (पूर्व में) कभी नहीं किया हो, करण का अर्थ है-ऐसा आत्मिक अध्यवसायरूप शक्ति का प्रयोग करना। अनादिकाल से अनन्त-पुद्गल-परावर्तकाल तक के संसार-परिभ्रमण के दौरान जीव ने पहले जिसका प्रयोग कभी भी नहीं किया था, ऐसे शुभ अध्यवसाय-रूप शक्ति का अभूतपूर्व प्रयोग करके रागद्वेष की सघन ग्रन्थि को भेदन करना अपूर्वकरण है। यह अपूर्वकरण पहले यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा विशुद्धतर (अधिक विशुद्ध) है। पूर्वप्रवृत्त-विशिष्ट यथाप्रवृत्तिकरण करने वाला भव्य जीव ही इस अपूर्वकरण को कर सकता है। अतः यह अपूर्वकरण विशिष्ट यथाप्रवृत्तिकरण का कार्य हुआ; और आगे के अनिवृत्तिकरण का कारण हुआ। पर्याप्त संज्ञिपंचेन्द्रिय परिपक्व तथाभव्य जीव ही इसके अधिकारी हैं। अपूर्वकरण में यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अधिक आत्मशुद्धि
और वीर्योल्लास की मात्रा बढ़ती है। तभी जीव रागद्वेष की दुर्भेद्य ग्रन्थि का भेदन कर पाता है। "इस अपूर्वकरण को तीव्र धार वाले कुठार के समान बताया गया है। इस करण के द्वारा अपनी आत्मशक्ति प्रबल रूप से प्रकट करके कई जीव ग्रन्थि भेद करते हैं।" चूंकि ऐसा करण यानी परिणाम विशेष विकासगामी आत्मा को अपूर्व-प्रथम बार ही प्राप्त होता है। रागद्वेष की निबिड़ ग्रन्थि का भेदन करने में पूर्वोक्त परिपक्व तथा भव्य जीव इस अपूर्वकरण का प्रयोग शस्त्ररूप में करता है। अतः ग्रन्थिभेद अपूर्वकरण की क्रिया का फल है। बीते हुए अनन्त भवों में जीव ने ग्रन्थिभेद का कार्य 'अपूर्वकरण' क्रिया से आज प्रथम बार ही किया है। यदि अपूर्वकरण न हो तो यथाप्रवृत्तिकरण का मूल्य नगण्य है। अपूर्वकरण होते ही दोनों करणों की कीमत अनेक गुणी बढ़ जाती है। यद्यपि यथाप्रवृत्तिकरण में आत्मा की निर्मलता के विकास का प्रारम्भ अवश्य होता है, किन्तु विशेष प्रकार की निर्मलता या विशुद्धि तो अपूर्वकरण में ही होती है।
१. कर्म तेरी गति न्यारी, पृ. ६८, ६९ २. (क) वही, भा. १, पृ.७६,७७ ।। (ख) तीव्रधार-पशुकल्पाऽपूर्वकरणेन हि ।
आविष्कृत्य परं वीर्य, ग्रन्थिं भिन्दन्ति केचन ॥ ६१८॥ -लोकप्रकाश सर्ग ३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org