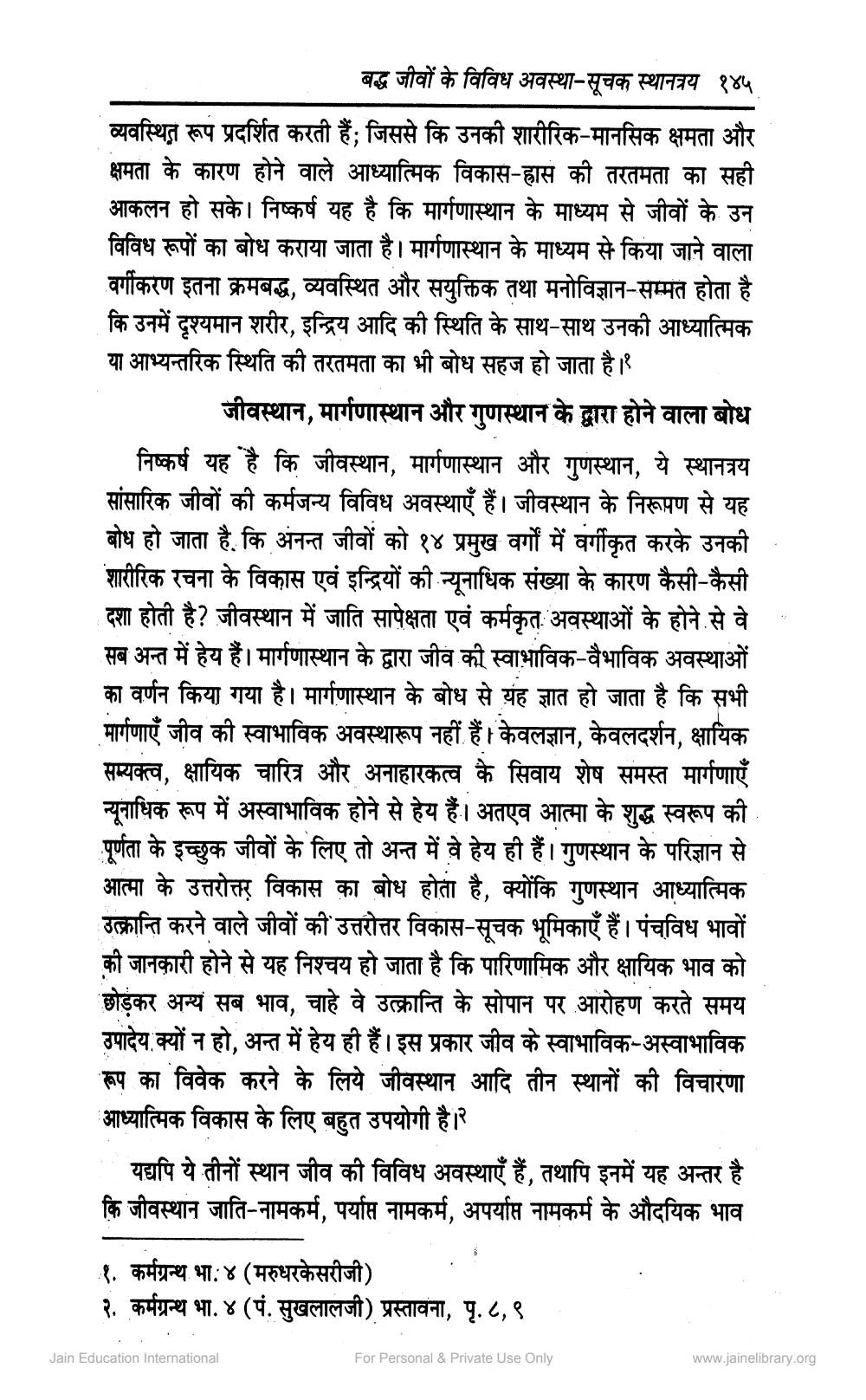________________
बद्ध जीवों के विविध अवस्था-सूचक स्थानत्रय १४५
व्यवस्थित रूप प्रदर्शित करती हैं, जिससे कि उनकी शारीरिक-मानसिक क्षमता और क्षमता के कारण होने वाले आध्यात्मिक विकास-हास की तरतमता का सही आकलन हो सके। निष्कर्ष यह है कि मार्गणास्थान के माध्यम से जीवों के उन विविध रूपों का बोध कराया जाता है। मार्गणास्थान के माध्यम से किया जाने वाला वर्गीकरण इतना क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सयुक्तिक तथा मनोविज्ञान-सम्मत होता है कि उनमें दृश्यमान शरीर, इन्द्रिय आदि की स्थिति के साथ-साथ उनकी आध्यात्मिक या आभ्यन्तरिक स्थिति की तरतमता का भी बोध सहज हो जाता है।
जीवस्थान, मार्गणास्थान और गुणस्थान के द्वारा होने वाला बोध निष्कर्ष यह है कि जीवस्थान, मार्गणास्थान और गुणस्थान, ये स्थानत्रय सांसारिक जीवों की कर्मजन्य विविध अवस्थाएँ हैं। जीवस्थान के निरूपण से यह बोध हो जाता है, कि अनन्त जीवों को १४ प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत करके उनकी शारीरिक रचना के विकास एवं इन्द्रियों की न्यूनाधिक संख्या के कारण कैसी-कैसी दशा होती है? जीवस्थान में जाति सापेक्षता एवं कर्मकृतः अवस्थाओं के होने से वे सब अन्त में हेय हैं। मार्गणास्थान के द्वारा जीव की स्वाभाविक-वैभाविक अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। मार्गणास्थान के बोध से यह ज्ञात हो जाता है कि सभी मार्गणाएँ जीव की स्वाभाविक अवस्थारूप नहीं हैं। केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और अनाहारकत्व के सिवाय शेष समस्त मार्गणाएँ न्यूनाधिक रूप में अस्वाभाविक होने से हेय हैं। अतएव आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पूर्णता के इच्छुक जीवों के लिए तो अन्त में वे हेय ही हैं। गुणस्थान के परिज्ञान से आत्मा के उत्तरोत्तर विकास का बोध होता है, क्योंकि गुणस्थान आध्यात्मिक उत्क्रान्ति करने वाले जीवों की उत्तरोत्तर विकास-सूचक भूमिकाएँ हैं। पंचविध भावों की जानकारी होने से यह निश्चय हो जाता है कि पारिणामिक और क्षायिक भाव को छोड़कर अन्यं सब भाव, चाहे वे उत्क्रान्ति के सोपान पर आरोहण करते समय उपादेय क्यों न हो, अन्त में हेय ही हैं। इस प्रकार जीव के स्वाभाविक-अस्वाभाविक रूप का विवेक करने के लिये जीवस्थान आदि तीन स्थानों की विचारणा आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
यद्यपि ये तीनों स्थान जीव की विविध अवस्थाएँ हैं, तथापि इनमें यह अन्तर है कि जीवस्थान जाति-नामकर्म, पर्याप्त नामकर्म, अपर्याप्त नामकर्म के औदयिक भाव
१. कर्मग्रन्थ भा: ४ (मरुधरकेसरीजी) २. कर्मग्रन्थ भा. ४ (पं. सुखलालजी) प्रस्तावना, पृ.८, ९
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org