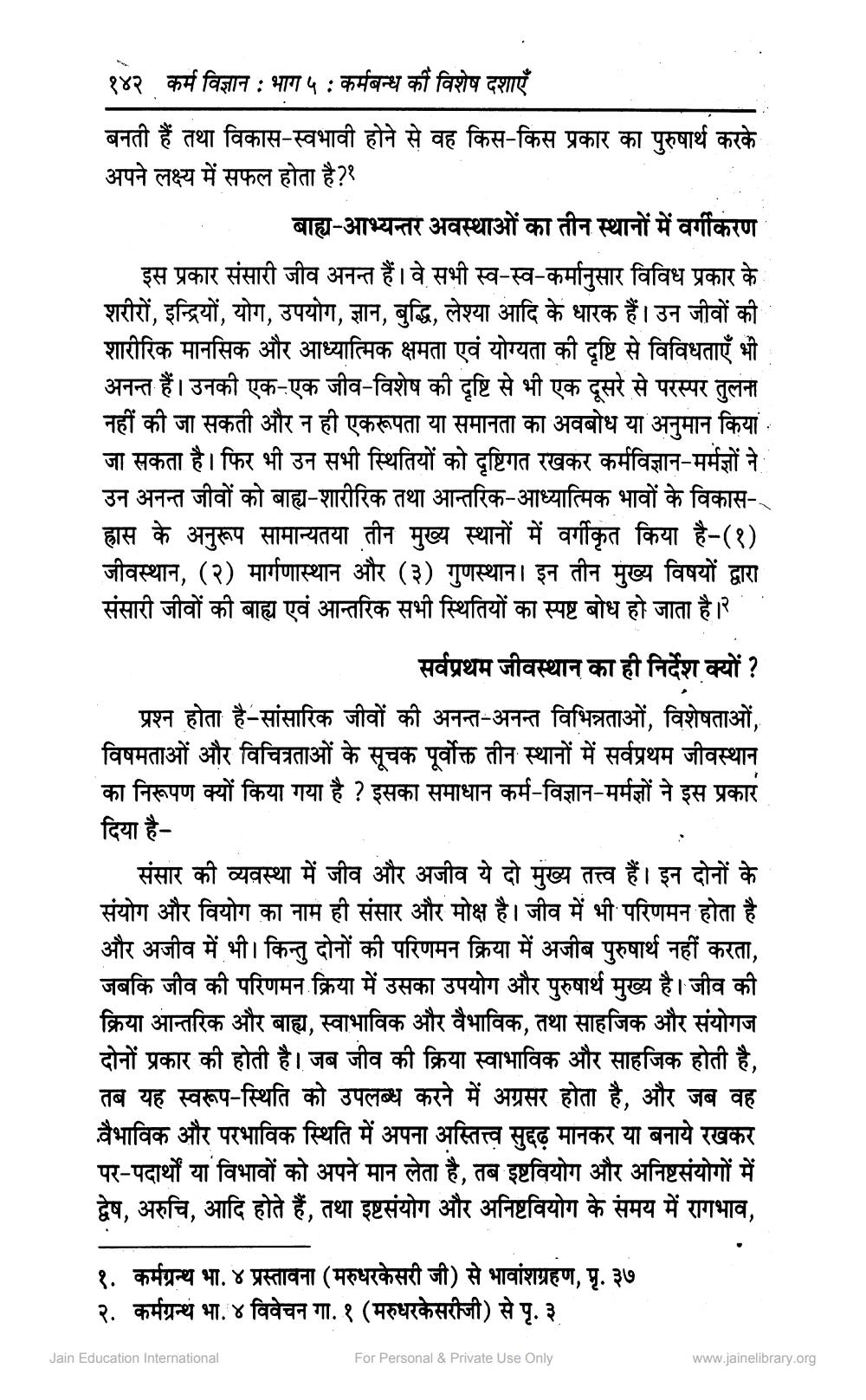________________
१४२ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ बनती हैं तथा विकास-स्वभावी होने से वह किस-किस प्रकार का पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य में सफल होता है??
. बाह्य-आभ्यन्तर अवस्थाओं का तीन स्थानों में वर्गीकरण इस प्रकार संसारी जीव अनन्त हैं। वे सभी स्व-स्व-कर्मानुसार विविध प्रकार के शरीरों, इन्द्रियों, योग, उपयोग, ज्ञान, बुद्धि, लेश्या आदि के धारक हैं। उन जीवों की शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता एवं योग्यता की दृष्टि से विविधताएँ भी अनन्त हैं। उनकी एक-एक जीव-विशेष की दृष्टि से भी एक दूसरे से परस्पर तुलना नहीं की जा सकती और न ही एकरूपता या समानता का अवबोध या अनुमान किया . जा सकता है। फिर भी उन सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखकर कर्मविज्ञान-मर्मज्ञों ने उन अनन्त जीवों को बाह्य-शारीरिक तथा आन्तरिक-आध्यात्मिक भावों के विकासह्रास के अनुरूप सामान्यतया तीन मुख्य स्थानों में वर्गीकृत किया है-(१) जीवस्थान, (२) मार्गणास्थान और (३) गुणस्थान। इन तीन मुख्य विषयों द्वारा संसारी जीवों की बाह्य एवं आन्तरिक सभी स्थितियों का स्पष्ट बोध हो जाता है।
सर्वप्रथम जीवस्थान का ही निर्देश क्यों ? प्रश्न होता है-सांसारिक जीवों की अनन्त-अनन्त विभिन्नताओं, विशेषताओं, विषमताओं और विचित्रताओं के सूचक पूर्वोक्त तीन स्थानों में सर्वप्रथम जीवस्थान का निरूपण क्यों किया गया है ? इसका समाधान कर्म-विज्ञान-मर्मज्ञों ने इस प्रकार दिया है
संसार की व्यवस्था में जीव और अजीव ये दो मुख्य तत्त्व हैं। इन दोनों के संयोग और वियोग का नाम ही संसार और मोक्ष है। जीव में भी परिणमन होता है और अजीव में भी। किन्तु दोनों की परिणमन क्रिया में अजीब पुरुषार्थ नहीं करता, जबकि जीव की परिणमन क्रिया में उसका उपयोग और पुरुषार्थ मुख्य है। जीव की क्रिया आन्तरिक और बाह्य, स्वाभाविक और वैभाविक, तथा साहजिक और संयोगज दोनों प्रकार की होती है। जब जीव की क्रिया स्वाभाविक और साहजिक होती है, तब यह स्वरूप-स्थिति को उपलब्ध करने में अग्रसर होता है, और जब वह वैभाविक और परभाविक स्थिति में अपना अस्तित्त्व सुद्दढ़ मानकर या बनाये रखकर पर-पदार्थों या विभावों को अपने मान लेता है, तब इष्टवियोग और अनिष्टसंयोगों में द्वेष, अरुचि, आदि होते हैं, तथा इष्टसंयोग और अनिष्टवियोग के समय में रागभाव,
१. कर्मग्रन्थ भा. ४ प्रस्तावना (मरुधरकेसरी जी) से भावांशग्रहण, प्र. ३७ २. कर्मग्रन्थ भा. ४ विवेचन गा. १ (मरुधरकेसरीजी) से पृ. ३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org