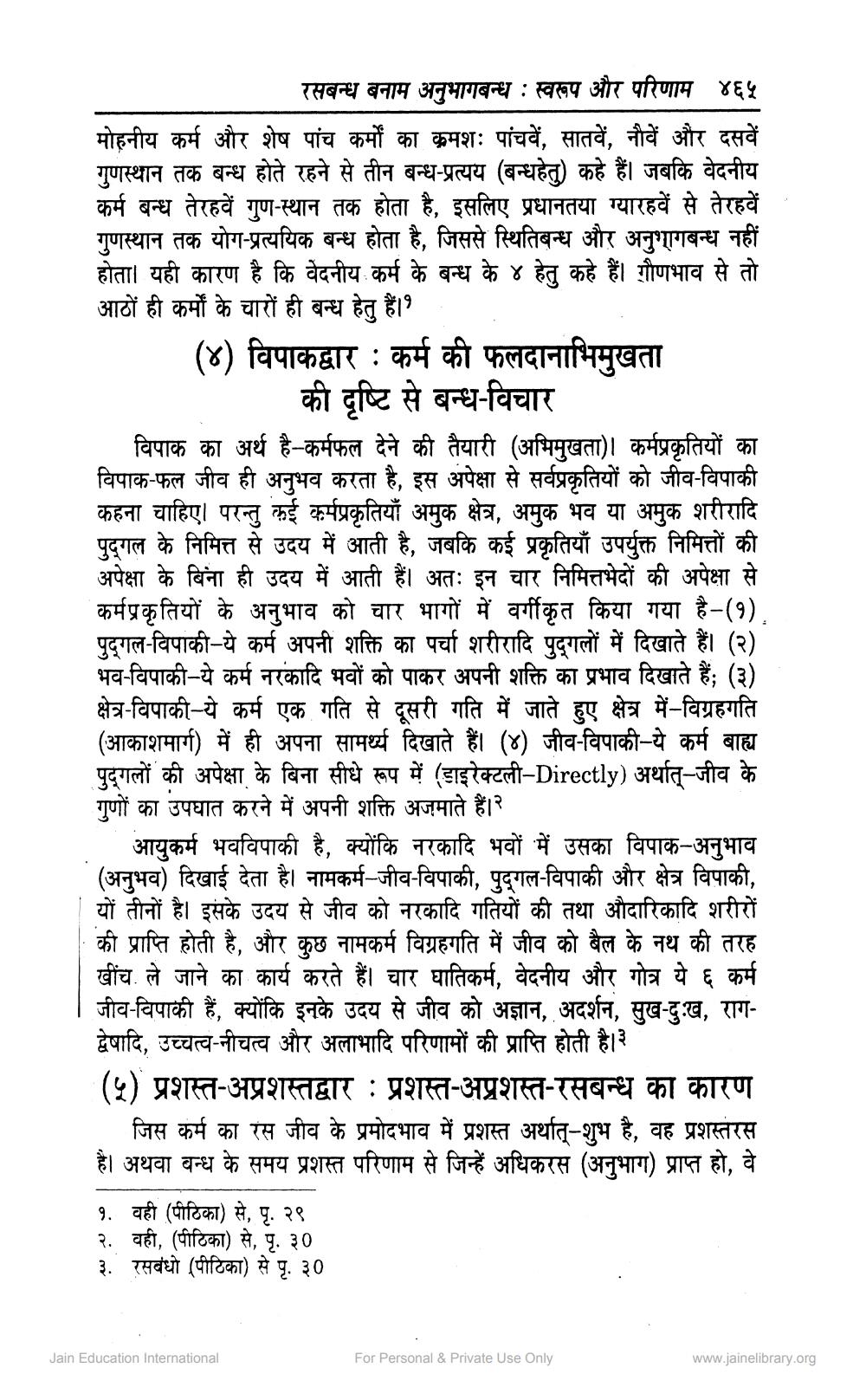________________
रसबन्ध बनाम अनुभागबन्ध : स्वरूप और परिणाम ४६५ मोहनीय कर्म और शेष पांच कर्मों का क्रमशः पांचवें, सातवें, नौवें और दसवें गुणस्थान तक बन्ध होते रहने से तीन बन्ध-प्रत्यय ( बन्धहेतु) कहे हैं। जबकि वेदनीय कर्मबन्ध तेरहवें गुण-स्थान तक होता है, इसलिए प्रधानतया ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान तक योग-प्रत्ययिक बन्ध होता है, जिससे स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध नहीं होता। यही कारण है कि वेदनीय कर्म के बन्ध के ४ हेतु कहे हैं। गौणभाव से तो आठों ही कर्मों के चारों ही बन्ध हेतु हैं । '
(४) विपाकद्वार : कर्म की फलदानाभिमुखता की दृष्टि से बन्ध-विचार
विपाक का अर्थ है-कर्मफल देने की तैयारी ( अभिमुखता)। कर्मप्रकृतियों का विपाक - फल जीव ही अनुभव करता है, इस अपेक्षा से सर्वप्रकृतियों को जीव - विपाकी कहना चाहिए। परन्तु कई कर्मप्रकृतियाँ अमुक क्षेत्र, अमुक भव या अमुक शरीरादि पुद्गल के निमित्त से उदय में आती है, जबकि कई प्रकृतियाँ उपर्युक्त निमित्तों की अपेक्षा के बिना ही उदय में आती हैं। अतः इन चार निमित्तभेदों की अपेक्षा से कर्म प्रकृतियों के अनुभाव को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है - (१), पुद्गल - विपाकी - ये कर्म अपनी शक्ति का पर्चा शरीरादि पुद्गलों में दिखाते हैं । (२) भव- विपाकी-ये कर्म नरकादि भवों को पाकर अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाते हैं; (३) क्षेत्र - विपाकी-ये कर्म एक गति से दूसरी गति में जाते हुए क्षेत्र में विग्रहगति (आकाशमार्ग) में ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। (४) जीव - विपाकी - ये कर्म बाह्य पुद्गलों की अपेक्षा के बिना सीधे रूप में ( डाइरेक्टली - Directly) अर्थात् - जीव के गुणों का उपघात करने में अपनी शक्ति अजमाते हैं । २
आयुकर्म भवविपाकी है, क्योंकि नरकादि भवों में उसका विपाक - अनुभाव ( अनुभव) दिखाई देता है। नामकर्म - जीव विपाकी, पुद्गल - विपाकी और क्षेत्र विपाकी, यों तीनों है। इसके उदय से जीव को नरकादि गतियों की तथा औदारिकादि शरीरों
प्राप्ति होती है, और कुछ नामकर्म विग्रहगति में जीव को बैल के नथ की तरह खींच ले जाने का कार्य करते हैं। चार घातिकर्म, वेदनीय और गोत्र ये ६ कर्म जीव - विपाकी हैं, क्योंकि इनके उदय से जीव को अज्ञान, अदर्शन, सुख-दुःख, रागद्वेषादि, उच्चत्व-नीचत्व और अलाभादि परिणामों की प्राप्ति होती है । ३
(५) प्रशस्त - अप्रशस्तद्वार : प्रशस्त - अप्रशस्त - रसबन्ध का कारण
जिस कर्म का रस जीव के प्रमोदभाव में प्रशस्त अर्थात् - शुभ है, वह प्रशस्तरस है। अथवा बन्ध के समय प्रशस्त परिणाम से जिन्हें अधिकरस (अनुभाग) प्राप्त हो, वे
१. वही (पीठिका) से, पृ. २९ २. वही, (पीठिका) से, पृ. ३० ३. रसबंधी (पीठिका) से
पृ. ३०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org