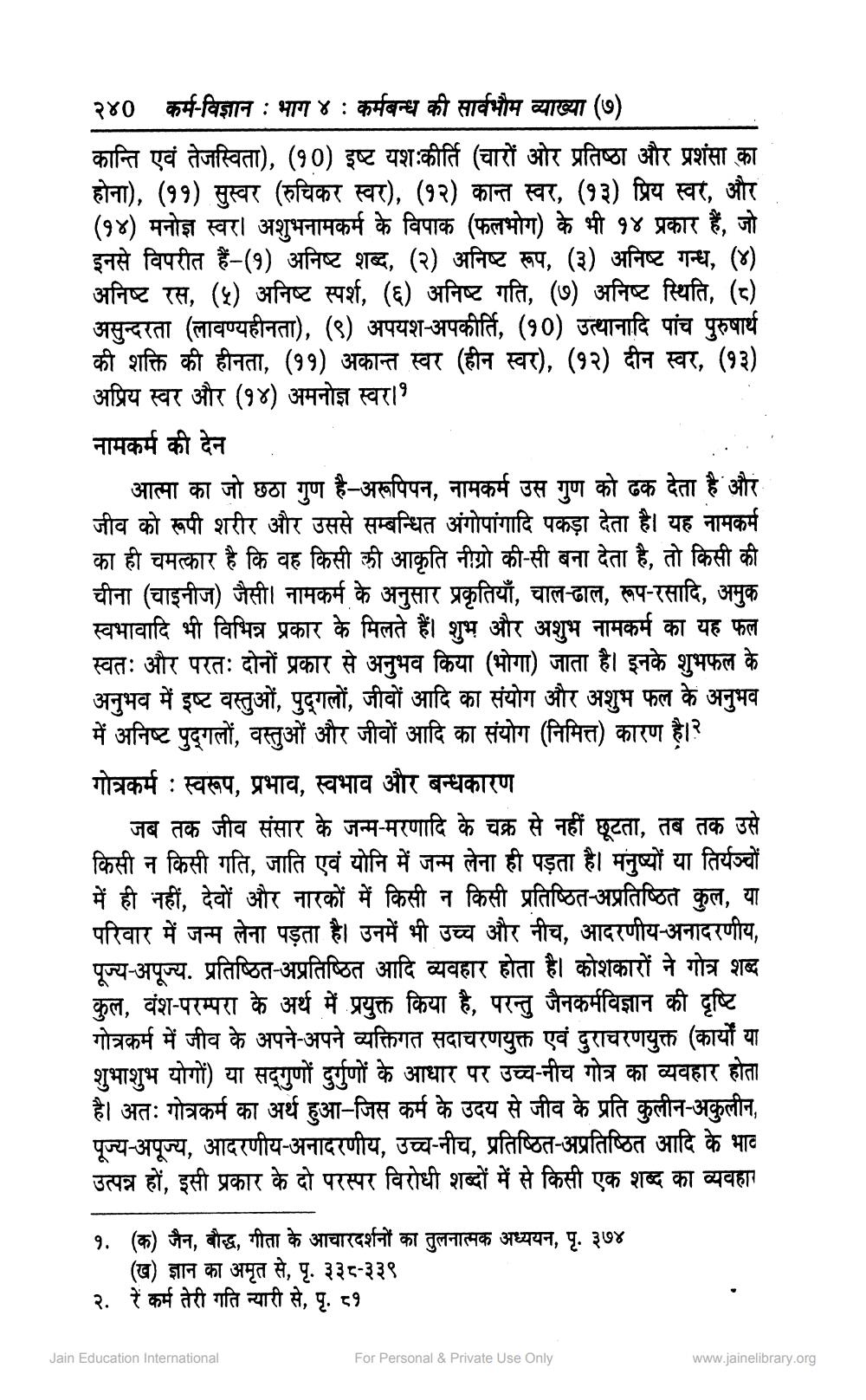________________
२४० कर्म-विज्ञान : भाग ४ : कर्मबन्ध की सार्वभौम व्याख्या (७) कान्ति एवं तेजस्विता), (१०) इष्ट यशःकीर्ति (चारों ओर प्रतिष्ठा और प्रशंसा का होना), (११) सुस्वर (रुचिकर स्वर), (१२) कान्त स्वर, (१३) प्रिय स्वर, और (१४) मनोज्ञ स्वर। अशुभनामकर्म के विपाक (फलभोग) के भी १४ प्रकार हैं, जो इनसे विपरीत हैं-(१) अनिष्ट शब्द, (२) अनिष्ट रूप, (३) अनिष्ट गन्ध, (४) अनिष्ट रस, (५) अनिष्ट स्पर्श, (६) अनिष्ट गति, (७) अनिष्ट स्थिति, (८) असुन्दरता (लावण्यहीनता), (९) अपयश-अपकीर्ति, (१०) उत्थानादि पांच पुरुषार्थ की शक्ति की हीनता, (११) अकान्त स्वर (हीन स्वर), (१२) दीन स्वर, (१३) अप्रिय स्वर और (१४) अमनोज्ञ स्वर।' नामकर्म की देन
आत्मा का जो छठा गुण है-अरूपिपन, नामकर्म उस गुण को ढक देता है और जीव को रूपी शरीर और उससे सम्बन्धित अंगोपांगादि पकड़ा देता है। यह नामकर्म का ही चमत्कार है कि वह किसी की आकृति नीग्रो की-सी बना देता है, तो किसी की चीना (चाइनीज) जैसी। नामकर्म के अनुसार प्रकृतियाँ, चाल-ढाल, रूप-रसादि, अमुक स्वभावादि भी विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। शुभ और अशुभ नामकर्म का यह फल स्वतः और परतः दोनों प्रकार से अनुभव किया (भोगा) जाता है। इनके शुभफल के अनुभव में इष्ट वस्तुओं, पुद्गलों, जीवों आदि का संयोग और अशुभ फल के अनुभव में अनिष्ट पुद्गलों, वस्तुओं और जीवों आदि का संयोग (निमित्त) कारण है। गोत्रकर्म : स्वरूप, प्रभाव, स्वभाव और बन्धकारण
जब तक जीव संसार के जन्म-मरणादि के चक्र से नहीं छूटता, तब तक उसे किसी न किसी गति, जाति एवं योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। मनुष्यों या तिर्यञ्चों में ही नहीं, देवों और नारकों में किसी न किसी प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित कुल, या परिवार में जन्म लेना पड़ता है। उनमें भी उच्च और नीच, आदरणीय-अनादरणीय, पूज्य-अपूज्य. प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित आदि व्यवहार होता है। कोशकारों ने गोत्र शब्द कुल, वंश-परम्परा के अर्थ में प्रयुक्त किया है, परन्तु जैनकर्मविज्ञान की दृष्टि गोत्रकर्म में जीव के अपने-अपने व्यक्तिगत सदाचरणयुक्त एवं दुराचरणयुक्त (कार्यों या शुभाशुभ योगों) या सद्गुणों दुर्गुणों के आधार पर उच्च-नीच गोत्र का व्यवहार होता है। अतः गोत्रकर्म का अर्थ हुआ-जिस कर्म के उदय से जीव के प्रति कुलीन-अकुलीन, पूज्य-अपूज्य, आदरणीय-अनादरणीय, उच्च-नीच, प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित आदि के भाव उत्पन्न हों, इसी प्रकार के दो परस्पर विरोधी शब्दों में से किसी एक शब्द का व्यवहार
१. (क) जैन, बौद्ध, गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन, पृ. ३७४
(ख) ज्ञान का अमृत से, पृ. ३३८-३३९ २. रे कर्म तेरी गति न्यारी से, पृ. ८१
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org