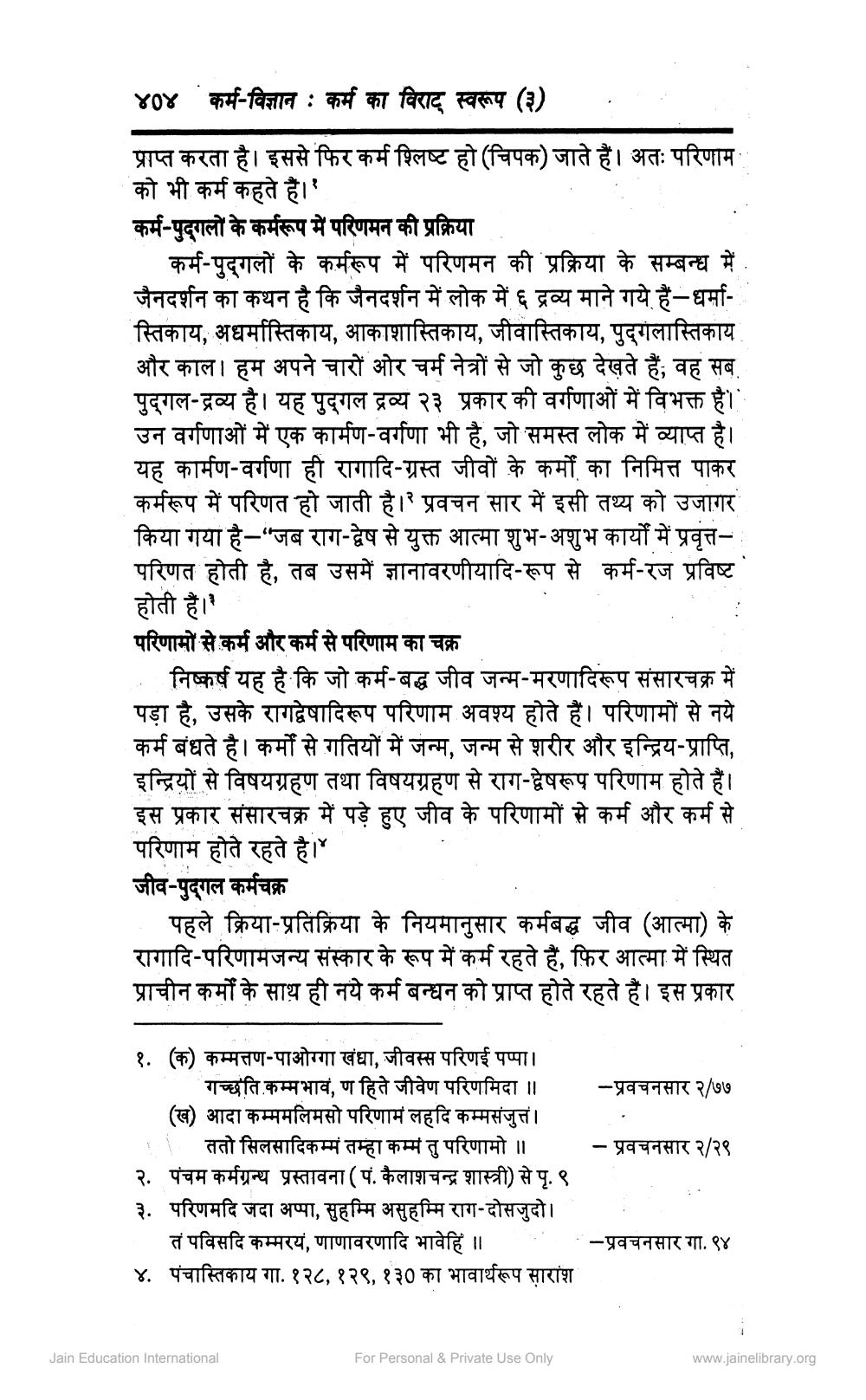________________
४०४
कर्म - विज्ञान : कर्म का विराट् स्वरूप (३)
प्राप्त करता है। इससे फिर कर्म श्लिष्ट हो (चिपक) जाते हैं। अतः परिणाम: को भी कर्म कहते हैं । '
कर्म- पुद्गलों के कर्मरूप में परिणमन की प्रक्रिया
कर्म-पुद्गलों के कर्मरूप में परिणमन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जैनदर्शन का कथन है कि जैनदर्शन में लोक में ६ द्रव्य माने गये हैं- धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल । हम अपने चारों ओर चर्म नेत्रों से जो कुछ देखते हैं, वह सब. पुद्गल-द्रव्य है। यह पुद्गल द्रव्य २३ प्रकार की वर्गणाओं में विभक्त है। उन वर्गणाओं में एक कार्मण वर्गणा भी है, जो समस्त लोक में व्याप्त है। यह कार्मण-वर्गणा ही रागादि-ग्रस्त जीवों के कर्मों का निमित्त पाकर कर्मरूप में परिणत हो जाती है। " प्रवचन सार में इसी तथ्य को उजागर किया गया है- “जब राग-द्वेष से युक्त आत्मा शुभ - अशुभ कार्यों में प्रवृत्तपरिणत होती है, तब उसमें ज्ञानावरणीयादि - रूप से कर्म-रज प्रविष्ट होती हैं। "
३
परिणामों से कर्म और कर्म से परिणाम का चक्र
निष्कर्ष यह है कि जो कर्म बद्ध जीव जन्म-मरणादिरूप संसारचक्र में पड़ा है, उसके रागद्वेषादिरूप परिणाम अवश्य होते हैं। परिणामों से नये कर्म बंधते है। कर्मों से गतियों में जन्म, जन्म से शरीर और इन्द्रिय-प्राप्ति, इन्द्रियों से विषयग्रहण तथा विषयग्रहण से राग-द्वेषरूप परिणाम होते हैं। इस प्रकार संसारचक्र में पड़े हुए जीव के परिणामों से कर्म और कर्म से परिणाम होते रहते है। * जीव- पुद्गल कर्मचक्र
पहले क्रिया-प्रतिक्रिया के नियमानुसार कर्मबद्ध जीव (आत्मा) के रागादि-परिणामजन्य संस्कार के रूप में कर्म रहते हैं, फिर आत्मा में स्थित प्राचीन कर्मों के साथ ही नये कर्म बन्धन को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार
१. (क) कम्मत्तण- पाओग्गा खंधा, जीवस्स परिणई पप्पा । गच्छति कम्मभाव, णहिते जीवेण परिणमिदा || (ख) आदा कम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मसंजुत्तं । ततो सिलसादिकम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ २. पंचम कर्मग्रन्थ प्रस्तावना (पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री) से पृ. ९ ३. परिणमदि जदा अप्पा, सुहम्मि असुहम्मि राग - दोसजुदो । तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादि भावेहिं || ४. पंचास्तिकाय गा. १२८, १२९, १३० का भावार्थरूप सारांश
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
- प्रवचनसार २ / ७७
प्रवचनसार २/२९
-प्रवचनसार गा. ९४
www.jainelibrary.org