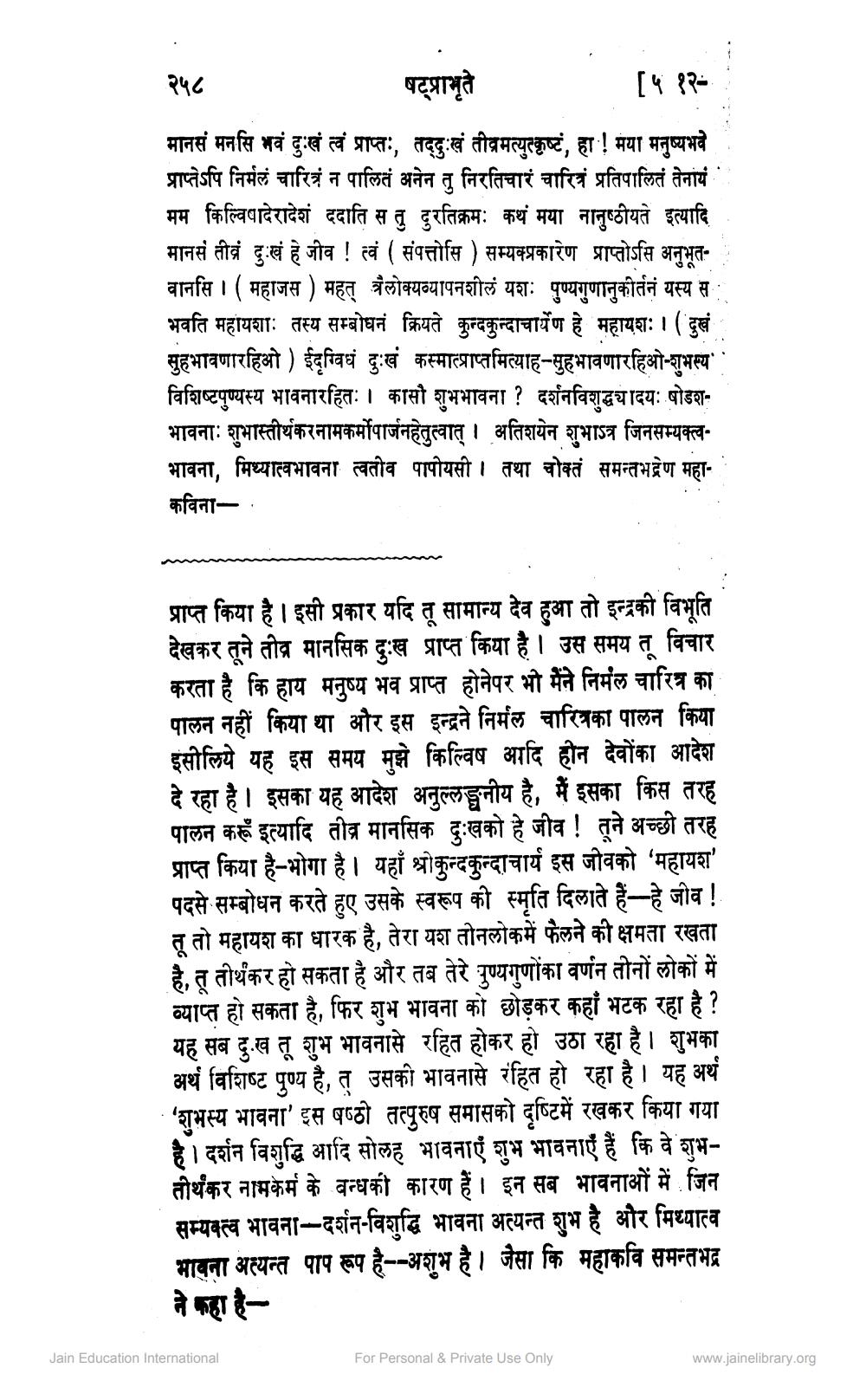________________
२५८
षट्प्राभृते
[५१२
मानसं मनसि भवं दुःखं त्वं प्राप्तः, तद्दुःखं तीव्रमत्युत्कृष्टं, हा ! मया मनुष्यभवे प्राप्तेऽपि निर्मलं चारित्रं न पालितं अनेन तू निरतिचारं चारित्रं प्रतिपालितं तेनायं मम किल्विषादेरादेशं ददाति स तु दुरतिक्रमः कथं मया नानुष्ठीयते इत्यादि मानसं तीव्रं दुःखं हे जीव ! त्वं ( संपत्तोसि ) सम्यक्प्रकारेण प्राप्तोऽसि अनुभूतवासि । ( महास) महत् त्रैलोक्यव्यापनशीलं यशः पुण्यगुणानुकीर्तनं यस्य स भवति महायशाः तस्य सम्बोधनं क्रियते कुन्दकुन्दाचार्येण हे महायशः । ( दुखं सुहभावणार हिओ ) ईदृग्विधं दुःखं कस्मात्प्राप्तमित्याह - सुहभावणार हिओ-शुभस्य विशिष्टपुण्यस्य भावनारहितः । कासी शुभभावना ? दर्शनविशुद्धयादयः षोडश - भावनाः शुभास्तीर्थकर नामकर्मोपार्जनहेतुत्वात् । अतिशयेन शुभात्र जिनसम्यक्त्व - भावना, मिथ्यात्वभावना त्वतीव पापीयसी । तथा चोक्तं समन्तभद्रेण महाकविना
प्राप्त किया है। इसी प्रकार यदि तू सामान्य देव हुआ तो इन्द्रकी विभूति देखकर तूने तीव्र मानसिक दुःख प्राप्त किया है। उस समय तू विचार करता है कि हाय मनुष्य भव प्राप्त होनेपर भी मैंने निर्मल चारित्र का पालन नहीं किया था और इस इन्द्रने निर्मल चारित्रका पालन किया इसीलिये यह इस समय मुझे किल्विष आदि होन देवोंका आदेश दे रहा है । इसका यह आदेश अनुल्लङ्घनीय है, मैं इसका किस तरह पालन करूँ इत्यादि तीव्र मानसिक दुःखको हे जीव ! तूने अच्छी तरह प्राप्त किया है - भोगा है । यहाँ श्रोकुन्दकुन्दाचार्य इस जीवको 'महायश' पदसे सम्बोधन करते हुए उसके स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं - हे जीव !! तू तो महायश का धारक है, तेरा यश तोनलोक में फैलने की क्षमता रखता है, तू तीर्थंकर हो सकता है और तब तेरे पुण्यगुणों का वर्णन तीनों लोकों में व्याप्त हो सकता है, फिर शुभ भावना को छोड़कर कहाँ भटक रहा है ? यह सब दुःख तू शुभ भावनासे रहित होकर हो उठा रहा है। शुभका अर्थं विशिष्ट पुण्य है, तु उसकी भावनासे रहित हो रहा है । यह अर्थ 'शुभस्य भावना' इस षष्ठी तत्पुरुष समासको दृष्टिमें रखकर किया गया है। दर्शन विशुद्धि आदि सोलह भावनाएं शुभ भावनाएं हैं कि वे शुभतीर्थंकर नामकर्म के बन्धकी कारण हैं। इन सब भावनाओं में जिन सम्यक्त्व भावना - दर्शन-विशुद्धि भावना अत्यन्त शुभ है और मिथ्यात्व भावना अत्यन्त पाप रूप है--अशुभ है। जैसा कि महाकवि समन्तभद्र ने कहा है
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org