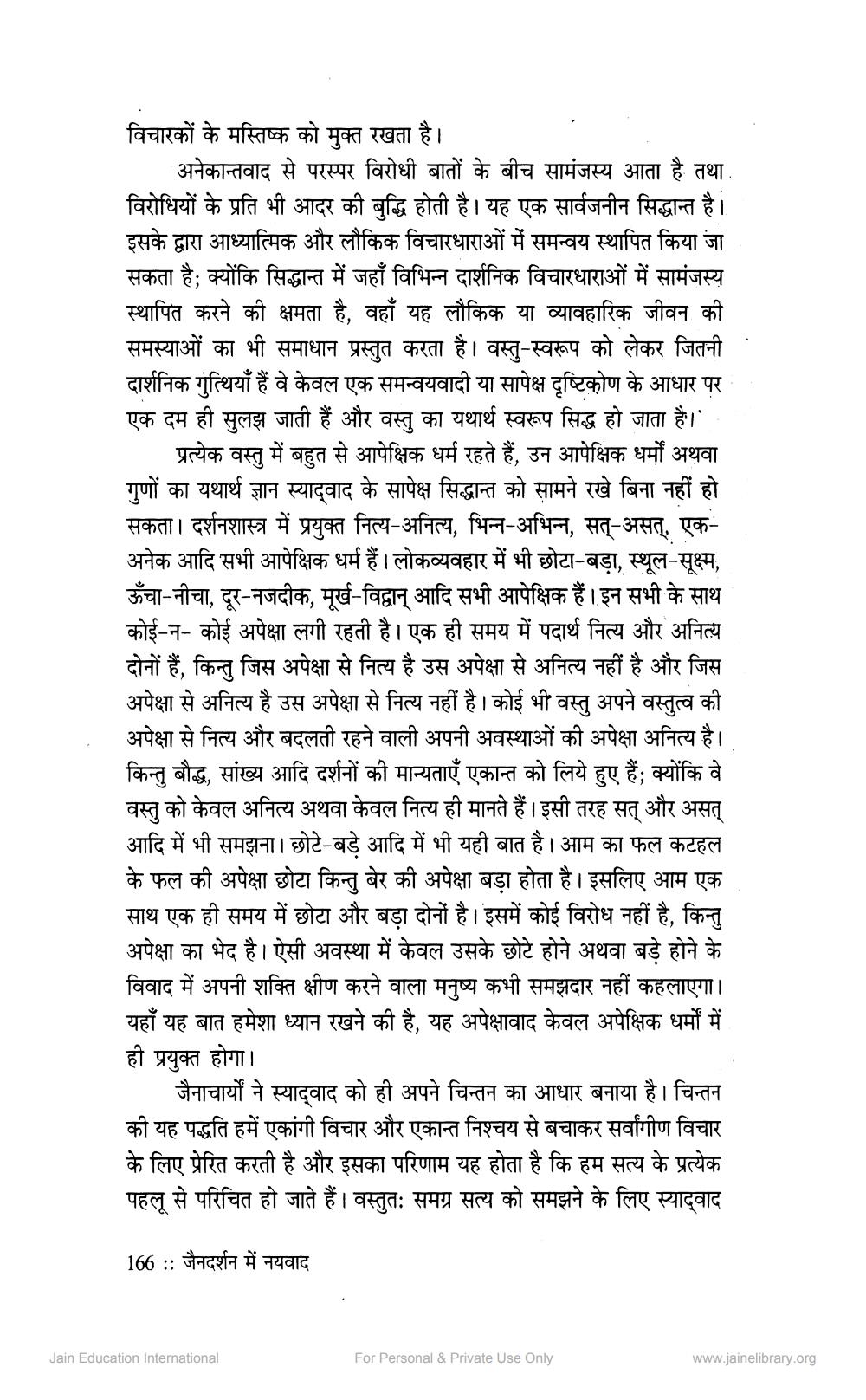________________
विचारकों के मस्तिष्क को मुक्त रखता है।
अनेकान्तवाद से परस्पर विरोधी बातों के बीच सामंजस्य आता है तथा विरोधियों के प्रति भी आदर की बुद्धि होती है। यह एक सार्वजनीन सिद्धान्त है। इसके द्वारा आध्यात्मिक और लौकिक विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया जा सकता है; क्योंकि सिद्धान्त में जहाँ विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है, वहाँ यह लौकिक या व्यावहारिक जीवन की समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करता है। वस्तु-स्वरूप को लेकर जितनी दार्शनिक गुत्थियाँ हैं वे केवल एक समन्वयवादी या सापेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर एक दम ही सुलझ जाती हैं और वस्तु का यथार्थ स्वरूप सिद्ध हो जाता है।
__ प्रत्येक वस्तु में बहुत से आपेक्षिक धर्म रहते हैं, उन आपेक्षिक धर्मों अथवा गुणों का यथार्थ ज्ञान स्याद्वाद के सापेक्ष सिद्धान्त को सामने रखे बिना नहीं हो सकता। दर्शनशास्त्र में प्रयुक्त नित्य-अनित्य, भिन्न-अभिन्न, सत्-असत्, एकअनेक आदि सभी आपेक्षिक धर्म हैं। लोकव्यवहार में भी छोटा-बड़ा, स्थूल-सूक्ष्म, ऊँचा-नीचा, दूर-नजदीक, मूर्ख-विद्वान् आदि सभी आपेक्षिक हैं। इन सभी के साथ कोई-न- कोई अपेक्षा लगी रहती है। एक ही समय में पदार्थ नित्य और अनित्य दोनों हैं, किन्तु जिस अपेक्षा से नित्य है उस अपेक्षा से अनित्य नहीं है और जिस अपेक्षा से अनित्य है उस अपेक्षा से नित्य नहीं है। कोई भी वस्तु अपने वस्तुत्व की अपेक्षा से नित्य और बदलती रहने वाली अपनी अवस्थाओं की अपेक्षा अनित्य है। किन्तु बौद्ध, सांख्य आदि दर्शनों की मान्यताएँ एकान्त को लिये हुए हैं; क्योंकि वे वस्तु को केवल अनित्य अथवा केवल नित्य ही मानते हैं। इसी तरह सत् और असत् आदि में भी समझना। छोटे-बड़े आदि में भी यही बात है। आम का फल कटहल के फल की अपेक्षा छोटा किन्तु बेर की अपेक्षा बड़ा होता है। इसलिए आम एक साथ एक ही समय में छोटा और बड़ा दोनों है। इसमें कोई विरोध नहीं है, किन्तु अपेक्षा का भेद है। ऐसी अवस्था में केवल उसके छोटे होने अथवा बड़े होने के विवाद में अपनी शक्ति क्षीण करने वाला मनुष्य कभी समझदार नहीं कहलाएगा। यहाँ यह बात हमेशा ध्यान रखने की है, यह अपेक्षावाद केवल अपेक्षिक धर्मों में ही प्रयुक्त होगा।
जैनाचार्यों ने स्याद्वाद को ही अपने चिन्तन का आधार बनाया है। चिन्तन की यह पद्धति हमें एकांगी विचार और एकान्त निश्चय से बचाकर सर्वांगीण विचार के लिए प्रेरित करती है और इसका परिणाम यह होता है कि हम सत्य के प्रत्येक पहलू से परिचित हो जाते हैं। वस्तुतः समग्र सत्य को समझने के लिए स्याद्वाद
166 :: जैनदर्शन में नयवाद
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org