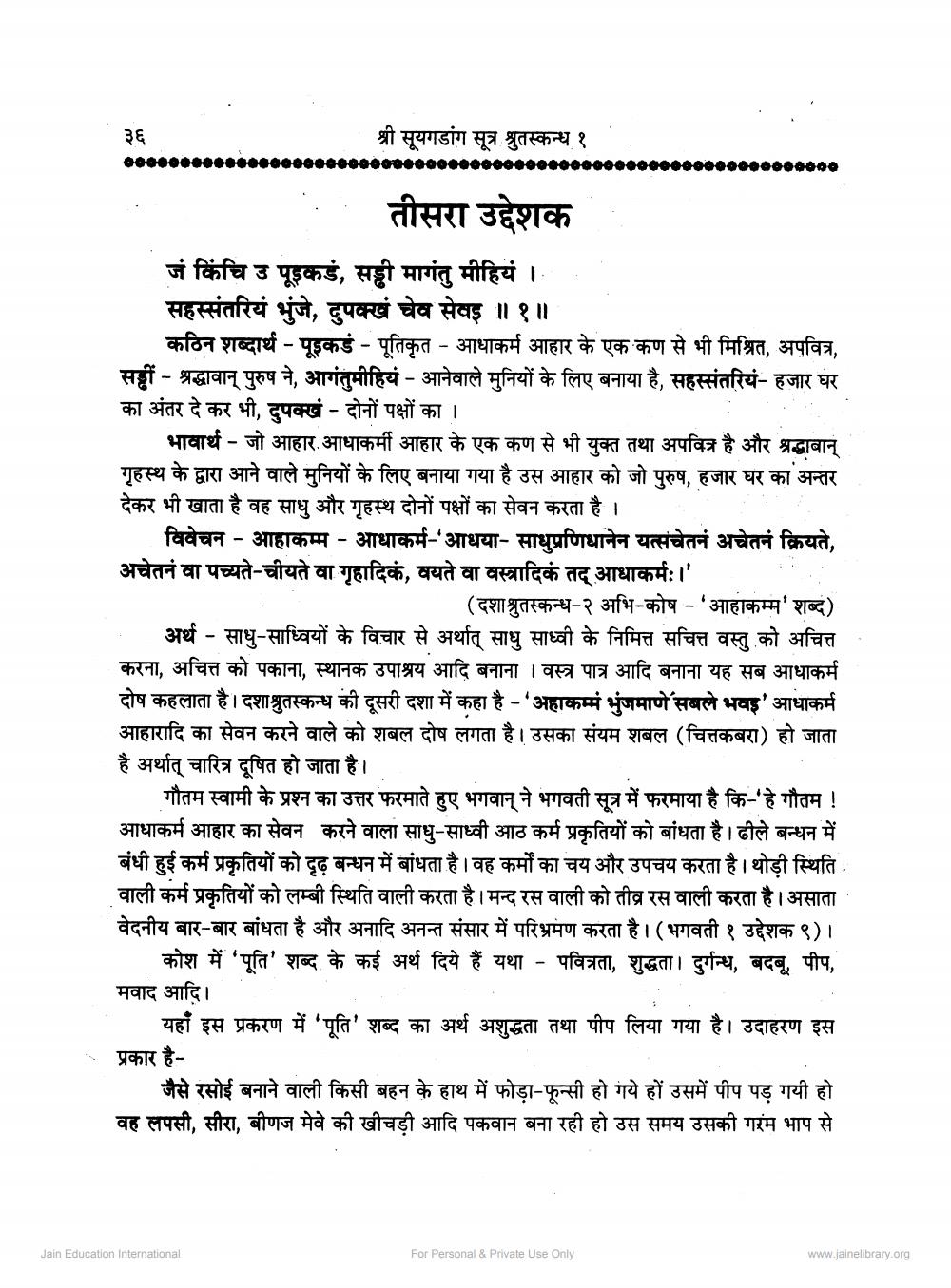________________
श्री सूयगडांग सूत्र श्रुतस्कन्ध १
तीसरा उद्देशक
जं किंचि उ पूइकडं, सड्डी मागंतु मीहियं । सहस्संतरियं भुंजे, दुपक्खं चेव सेवइ ॥ १॥ कठिन शब्दार्थ - पूइकडं पूतिकृत आधाकर्म आहार एक कण से भी मिश्रित, अपवित्र, सड्डी - श्रद्धावान् पुरुष ने, आगंतुमीहियं - आनेवाले मुनियों के लिए बनाया है, सहस्संतरियं - हजार घर का अंतर दे कर भी, दुपक्खं दोनों पक्षों का ।
भावार्थ - जो आहार आधाकर्मी आहार एक कण भी युक्त तथा अपवित्र है और श्रद्धान् गृहस्थ के द्वारा आने वाले मुनियों के लिए बनाया गया है उस आहार को जो पुरुष, हजार घर का अन्तर देकर भी खाता है वह साधु और गृहस्थ दोनों पक्षों का सेवन करता है ।
३६
-
विवेचन - आहाकम्म - आधाकर्म- 'आधया- साधुप्रणिधानेन यत्संचेतनं अचेतनं क्रियते, अचेतनं वा पच्यते- चीयते वा गृहादिकं, वयते वा वस्त्रादिकं तद् आधाकर्मः ।'
(दशा श्रुतस्कन्ध-२ अभि-कोष - 'आहाकम्म' शब्द ) अर्थ - साधु-साध्वियों के विचार से अर्थात् साधु साध्वी के निमित्त सचित्त वस्तु को अचित्त करना, अचित्त को पकाना, स्थानक उपाश्रय आदि बनाना । वस्त्र पात्र आदि बनाना यह सब आधाकर्म दोष कहलाता है। दशाश्रुतस्कन्ध की दूसरी दशा में कहा है- 'अहाकम्मं भुंजमाणे सबले भवइ' आधाकर्म आहारादि का सेवन करने वाले को शबल दोष लगता है। उसका संयम शबल (चित्तकबरा) हो जाता है अर्थात् चारित्र दूषित हो जाता है।
गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर फरमाते हुए भगवान् ने भगवती सूत्र में फरमाया है कि-'हे गौतम ! आधाकर्म आहार का सेवन करने वाला साधु-साध्वी आठ कर्म प्रकृतियों को बांधता है। ढीले बन्धन में कर्म प्रकृतियों को दृढ़ बन्धन में बांधता है। वह कर्मों का चय और उपचय करता है। थोड़ी स्थिति वाली कर्म प्रकृतियों को लम्बी स्थिति वाली करता है । मन्द रस वाली को तीव्र रस वाली करता है । असाता वेदनीय बार-बार बांधता है और अनादि अनन्त संसार में परिभ्रमण करता है। (भगवती १ उद्देशक ९) । कोश में 'पूति' शब्द के कई अर्थ दिये हैं यथा पवित्रता, शुद्धता । दुर्गन्ध, बदबू, पीप,
मवाद आदि ।
यहाँ इस प्रकरण में 'पूति' शब्द का अर्थ अशुद्धता तथा पीप लिया गया है। उदाहरण इस प्रकार है
जैसे रसोई बनाने वाली किसी बहन के हाथ में फोड़ा-फून्सी हो गये हों उसमें पीप पड़ गयी हो वह लपसी, सीरा, बीणज मेवे की खीचड़ी आदि पकवान बना रही हो उस समय उसकी गरंम भाप से
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org