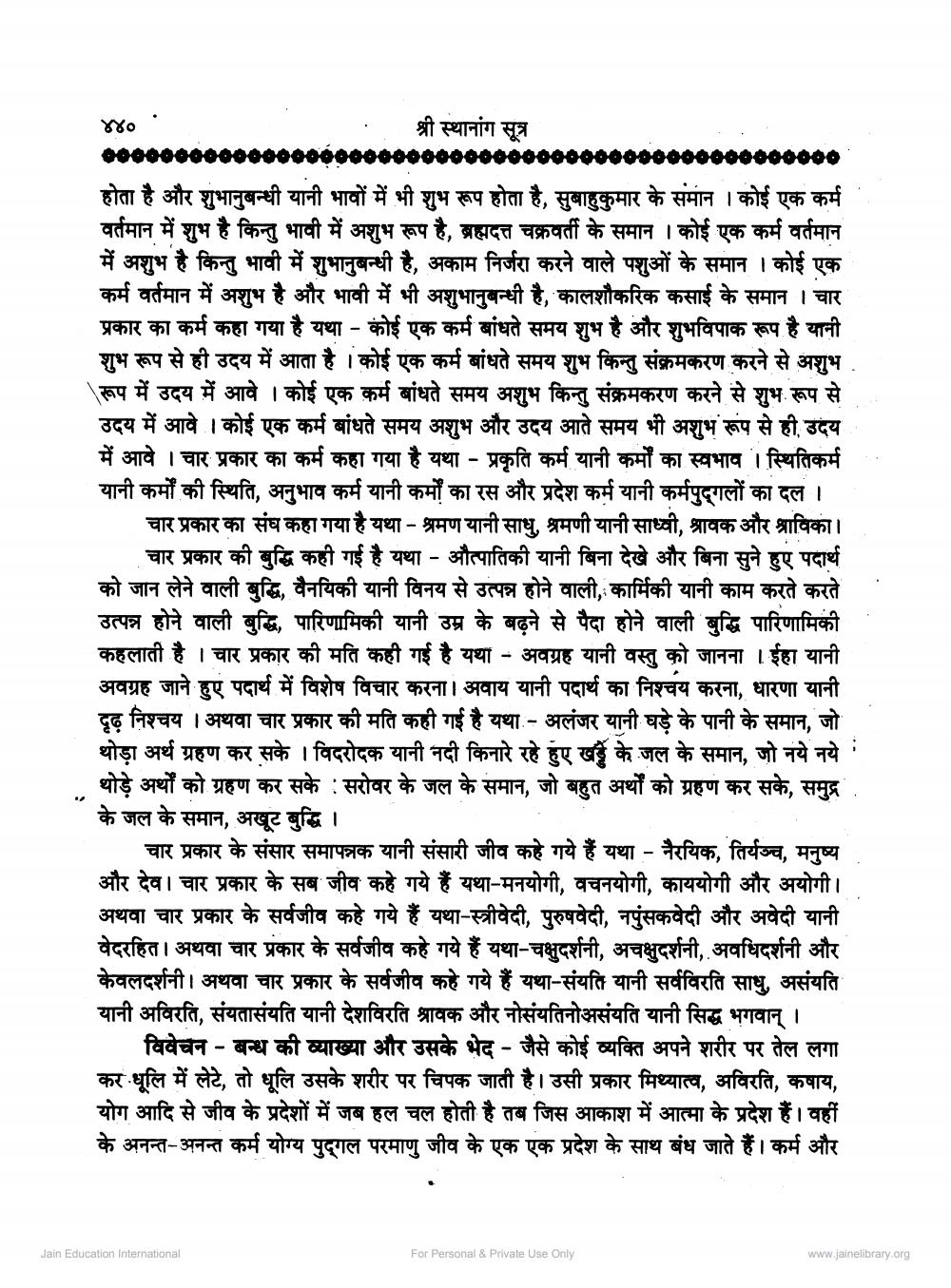________________
४४०
. श्री स्थानांग सूत्र 000000000000000000000000000000000000000000000000000 होता है और शुभानुबन्धी यानी भावों में भी शुभ रूप होता है, सुबाहुकुमार के समान । कोई एक कर्म वर्तमान में शुभ है किन्तु भावी में अशुभ रूप है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के समान । कोई एक कर्म वर्तमान में अशुभ है किन्तु भावी में शुभानुबन्धी है, अकाम निर्जरा करने वाले पशुओं के समान । कोई एक कर्म वर्तमान में अशुभ है और भावी में भी अशुभानुबन्धी है, कालशौकरिक कसाई के समान । चार प्रकार का कर्म कहा गया है यथा - कोई एक कर्म बांधते समय शुभ है और शुभविपाक रूप है यानी शुभ रूप से ही उदय में आता है । कोई एक कर्म बांधते समय शुभ किन्तु संक्रमकरण करने से अशुभ रूप में उदय में आवे । कोई एक कर्म बांधते समय अशुभ किन्तु संक्रमकरण करने से शुभ रूप से उदय में आवे । कोई एक कर्म बांधते समय अशुभ और उदय आते समय भी अशुभ रूप से ही, उदय में आवे । चार प्रकार का कर्म कहा गया है यथा - प्रकृति कर्म यानी कर्मों का स्वभाव । स्थितिकर्म यानी कर्मों की स्थिति, अनुभाव कर्म यानी कर्मों का रस और प्रदेश कर्म यानी कर्मपुद्गलों का दल ।
चार प्रकार का संघ कहा गया है यथा - श्रमण यानी साधु, श्रमणी यानी साध्वी, श्रावक और श्राविका।
चार प्रकार की बुद्धि कही गई है यथा - औत्पातिकी यानी बिना देखे और बिना सुने हुए पदार्थ को जान लेने वाली बुद्धि, वैनयिकी यानी विनय से उत्पन्न होने वाली, कार्मिकी यानी काम करते करते उत्पन्न होने वाली बुद्धि, पारिणामिकी यानी उम्र के बढ़ने से पैदा होने वाली बुद्धि पारिणामिकी कहलाती है । चार प्रकार की मति कही गई है यथा - अवग्रह यानी वस्तु को जानना । ईहा यानी अवग्रह जाने हुए पदार्थ में विशेष विचार करना। अवाय यानी पदार्थ का निश्चय करना, धारणा यानी दृढ़ निश्चय । अथवा चार प्रकार की मति कही गई है यथा - अलंजर यानी घड़े के पानी के समान, जो थोड़ा अर्थ ग्रहण कर सके । विदरोदक यानी नदी किनारे रहे हुए खडे के जल के समान, जो नये नये । थोड़े अर्थों को ग्रहण कर सके : सरोवर के जल के समान, जो बहुत अर्थों को ग्रहण कर सके, समुद्र . के जल के समान, अखूट बुद्धि । ___ चार प्रकार के संसार समापनक यानी संसारी जीव कहे गये हैं यथा - नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव। चार प्रकार के सब जीव कहे गये हैं यथा-मनयोगी, वचनयोगी, काययोगी और अयोगी। अथवा चार प्रकार के सर्वजीव कहे गये हैं यथा-स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी और अवेदी यानी वेदरहित। अथवा चार प्रकार के सर्वजीव कहे गये हैं यथा-चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी और केवलदर्शनी। अथवा चार प्रकार के सर्वजीव कहे गये हैं यथा-संयति यानी सर्वविरति साधु, असंयति यानी अविरति, संयतासंयति यानी देशविरति श्रावक और नोसंयतिनोअसंयति यानी सिद्ध भगवान् ।
विवेचन - बन्ध की व्याख्या और उसके भेद - जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर पर तेल लगा कर धूलि में लेटे, तो धूलि उसके शरीर पर चिपक जाती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग आदि से जीव के प्रदेशों में जब हल चल होती है तब जिस आकाश में आत्मा के प्रदेश हैं। वहीं के अनन्त-अनन्त कर्म योग्य पुद्गल परमाणु जीव के एक एक प्रदेश के साथ बंध जाते हैं। कर्म और
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org