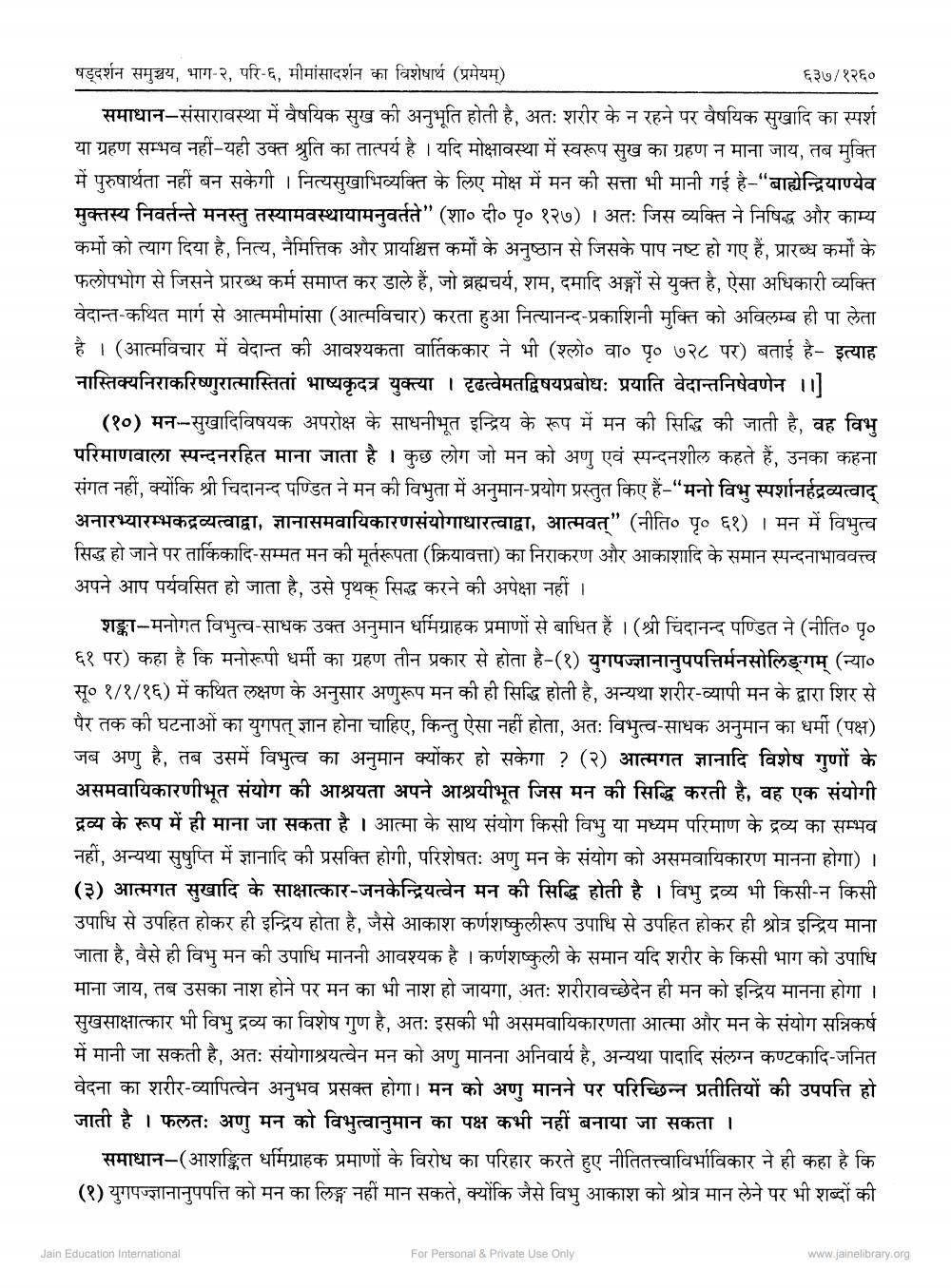________________
षड्दर्शन समुच्चय, भाग-२, परि-६, मीमांसादर्शन का विशेषार्थ (प्रमेयम्)
६३७/१२६० समाधान-संसारावस्था में वैषयिक सुख की अनुभूति होती है, अतः शरीर के न रहने पर वैषयिक सुखादि का स्पर्श या ग्रहण सम्भव नहीं-यही उक्त श्रुति का तात्पर्य है । यदि मोक्षावस्था में स्वरूप सुख का ग्रहण न माना जाय, तब मुक्ति में पुरुषार्थता नहीं बन सकेगी । नित्यसुखाभिव्यक्ति के लिए मोक्ष में मन की सत्ता भी मानी गई है-"बाह्येन्द्रियाण्येव मुक्तस्य निवर्तन्ते मनस्तु तस्यामवस्थायामनुवर्तते" (शा० दी० पृ० १२७) । अतः जिस व्यक्ति ने निषिद्ध और काम्य कर्मो को त्याग दिया है, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त कर्मों के अनुष्ठान से जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, प्रारब्ध कर्मों के फलोपभोग से जिसने प्रारब्ध कर्म समाप्त कर डाले हैं, जो ब्रह्मचर्य, शम, दमादि अङ्गों से युक्त है, ऐसा अधिकारी व्यक्ति वेदान्त-कथित मार्ग से आत्ममीमांसा (आत्मविचार) करता हुआ नित्यानन्द-प्रकाशिनी मुक्ति को अविलम्ब ही पा लेता है । (आत्मविचार में वेदान्त की आवश्यकता वार्तिककार ने भी (श्लो० वा० ए० ७२८ पर) बताई है- इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदन युक्त्या । दृढत्वेमतद्विषयप्रबोध: प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ।।] ___ (१०) मन-सुखादिविषयक अपरोक्ष के साधनीभूत इन्द्रिय के रूप में मन की सिद्धि की जाती है, वह विभु परिमाणवाला स्पन्दनरहित माना जाता है । कुछ लोग जो मन को अणु एवं स्पन्दनशील कहते हैं, उनका कहना संगत नहीं, क्योंकि श्री चिदानन्द पण्डित ने मन की विभुता में अनुमान-प्रयोग प्रस्तुत किए हैं-"मनो विभु स्पर्शानर्हद्रव्यत्वाद् अनारभ्यारम्भकद्रव्यत्वाद्वा, ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाधारत्वाद्वा, आत्मवत्" (नीति० पृ० ६१) । मन में विभुत्व सिद्ध हो जाने पर तार्किकादि-सम्मत मन की मूर्तरूपता (क्रियावत्ता) का निराकरण और आकाशादि के समान स्पन्दनाभाववत्त्व अपने आप पर्यवसित हो जाता है, उसे पृथक् सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं ।
शङ्का-मनोगत विभुत्व-साधक उक्त अनुमान मिग्राहक प्रमाणों से बाधित हैं । (श्री चिंदानन्द पण्डित ने (नीति० पृ० ६१ पर) कहा है कि मनोरूपी धर्मी का ग्रहण तीन प्रकार से होता है-(१) युगपज्ज्ञानानुपपत्तिर्मनसोलिङ्गम् (न्या० स०१/१/१६) में कथित लक्षण के अनसार अणरूप मन की ही सिद्धि होती है. अन्यथा शरीर-व्यापी मन के द्वारा शिर से पैर तक की घटनाओं का युगपत् ज्ञान होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता, अत: विभुत्व-साधक अनुमान का धर्मी (पक्ष) जब अणु है, तब उसमें विभुत्व का अनुमान क्योंकर हो सकेगा ? (२) आत्मगत ज्ञानादि विशेष गुणों के असमवायिकारणीभूत संयोग की आश्रयता अपने आश्रयीभूत जिस मन की सिद्धि करती है, वह एक संयोगी द्रव्य के रूप में ही माना जा सकता है । आत्मा के साथ संयोग किसी विभु या मध्यम परिमाण के द्रव्य का सम्भव नहीं, अन्यथा सुषुप्ति में ज्ञानादि की प्रसक्ति होगी, परिशेषतः अणु मन के संयोग को असमवायिकारण मानना होगा)। (३) आत्मगत सखादि के साक्षात्कार-जनकेन्द्रियत्वेन मन की सिद्धि होती है। विभ द्रव्य भी किसी-न किसी उपाधि से उपहित होकर ही इन्द्रिय होता है, जैसे आकाश कर्णशष्कुलीरूप उपाधि से उपहित होकर ही श्रोत्र इन्द्रिय माना जाता है, वैसे ही विभु मन की उपाधि माननी आवश्यक है । कर्णशष्कुली के समान यदि शरीर के किसी भाग को उपाधि माना जाय, तब उसका नाश होने पर मन का भी नाश हो जायगा, अतः शरीरावच्छेदेन ही मन को इन्द्रिय मानना होगा । सुखसाक्षात्कार भी विभु द्रव्य का विशेष गुण है, अत: इसकी भी असमवायिकारणता आत्मा और मन के संयोग सन्निकर्ष में मानी जा सकती है, अतः संयोगाश्रयत्वेन मन को अणु मानना अनिवार्य है, अन्यथा पादादि संलग्न कण्टकादि-जनित वेदना का शरीर-व्यापित्वेन अनुभव प्रसक्त होगा। मन को अणु मानने पर परिच्छिन्न प्रतीतियों की उपपत्ति हो जाती है । फलतः अणु मन को विभुत्वानुमान का पक्ष कभी नहीं बनाया जा सकता ।
समाधान-(आशङ्कित धर्मिग्राहक प्रमाणों के विरोध का परिहार करते हुए नीतितत्त्वाविर्भाविकार ने ही कहा है कि (१) युगपज्ज्ञानानुपपत्ति को मन का लिङ्ग नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे विभु आकाश को श्रोत्र मान लेने पर भी शब्दों की
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org