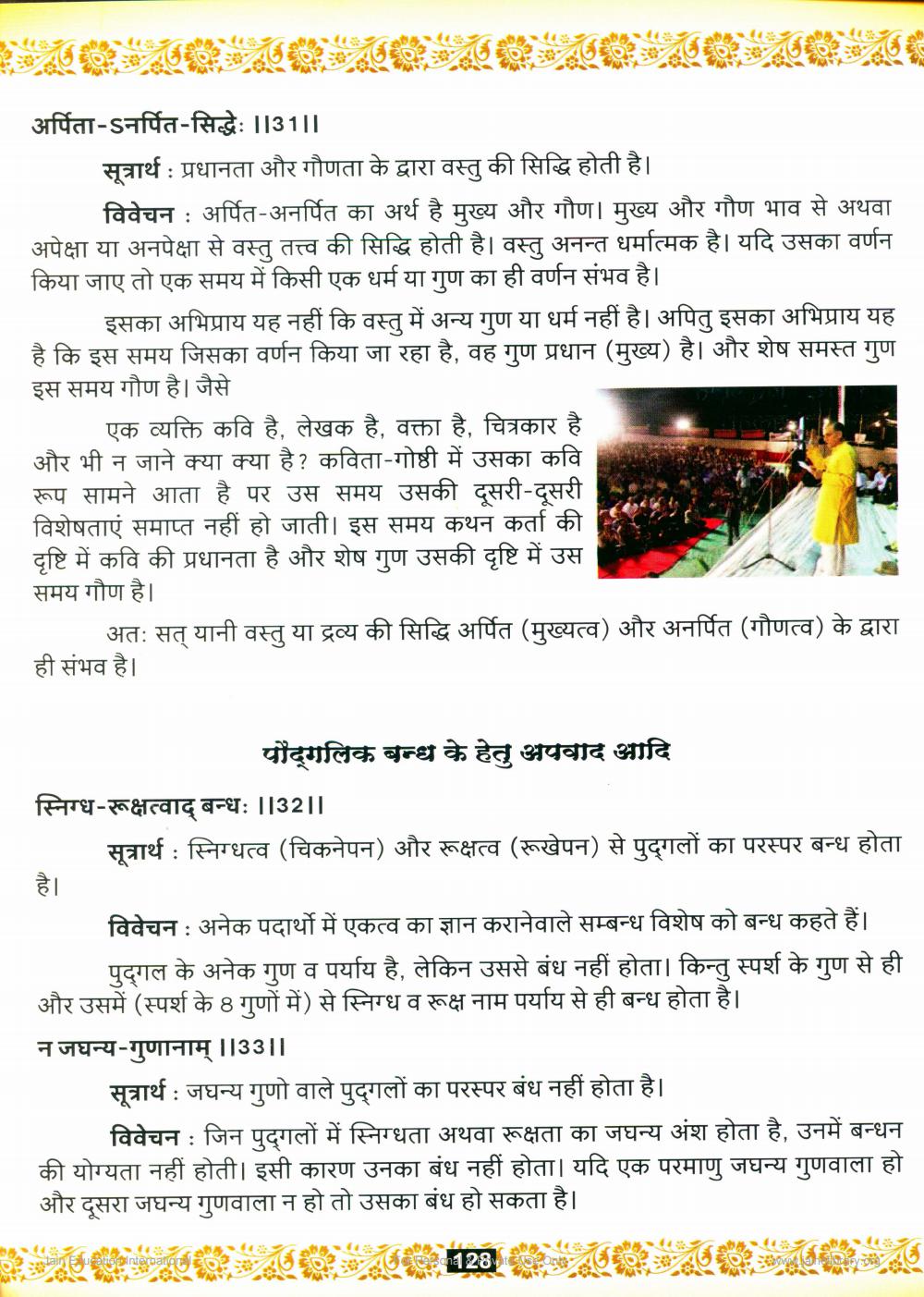________________
अर्पिता-ऽनर्पित-सिद्धेः ।।31।।
सूत्रार्थ : प्रधानता और गौणता के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है।
विवेचन : अर्पित-अनर्पित का अर्थ है मुख्य और गौण। मुख्य और गौण भाव से अथवा अपेक्षा या अनपेक्षा से वस्तु तत्त्व की सिद्धि होती है। वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। यदि उसका वर्णन किया जाए तो एक समय में किसी एक धर्म या गुण का ही वर्णन संभव है।
इसका अभिप्राय यह नहीं कि वस्तु में अन्य गुण या धर्म नहीं है। अपितु इसका अभिप्राय यह है कि इस समय जिसका वर्णन किया जा रहा है, वह गुण प्रधान (मुख्य) है। और शेष समस्त गुण इस समय गौण है। जैसे
एक व्यक्ति कवि है, लेखक है, वक्ता है, चित्रकार है और भी न जाने क्या क्या है? कविता-गोष्ठी में उसका कवि रूप सामने आता है पर उस समय उसकी दूसरी-दूसरी विशेषताएं समाप्त नहीं हो जाती। इस समय कथन कर्ता की दृष्टि में कवि की प्रधानता है और शेष गुण उसकी दृष्टि में उस समय गौण है।
अत: सत् यानी वस्तु या द्रव्य की सिद्धि अर्पित (मुख्यत्व) और अनर्पित (गौणत्व) के द्वारा ही संभव है।
पौद्गलिक बन्ध के हेतु अपवाद आदि स्निग्ध-रूक्षत्वाद् बन्धः ||32||
सूत्रार्थ : स्निग्धत्व (चिकनेपन) और रूक्षत्व (रूखेपन) से पुद्गलों का परस्पर बन्ध होता है।
विवेचन : अनेक पदार्थो में एकत्व का ज्ञान करानेवाले सम्बन्ध विशेष को बन्ध कहते हैं।
पुद्गल के अनेक गुण व पर्याय है, लेकिन उससे बंध नहीं होता। किन्तु स्पर्श के गुण से ही और उसमें (स्पर्श के 8 गुणों में) से स्निग्ध व रूक्ष नाम पर्याय से ही बन्ध होता है। न जघन्य-गुणानाम् ।।33||
सूत्रार्थ : जघन्य गुणो वाले पुद्गलों का परस्पर बंध नहीं होता है।
विवेचन : जिन पुद्गलों में स्निग्धता अथवा रूक्षता का जघन्य अंश होता है, उनमें बन्धन की योग्यता नहीं होती। इसी कारण उनका बंध नहीं होता। यदि एक परमाणु जघन्य गुणवाला हो और दूसरा जघन्य गुणवाला न हो तो उसका बंध हो सकता है।