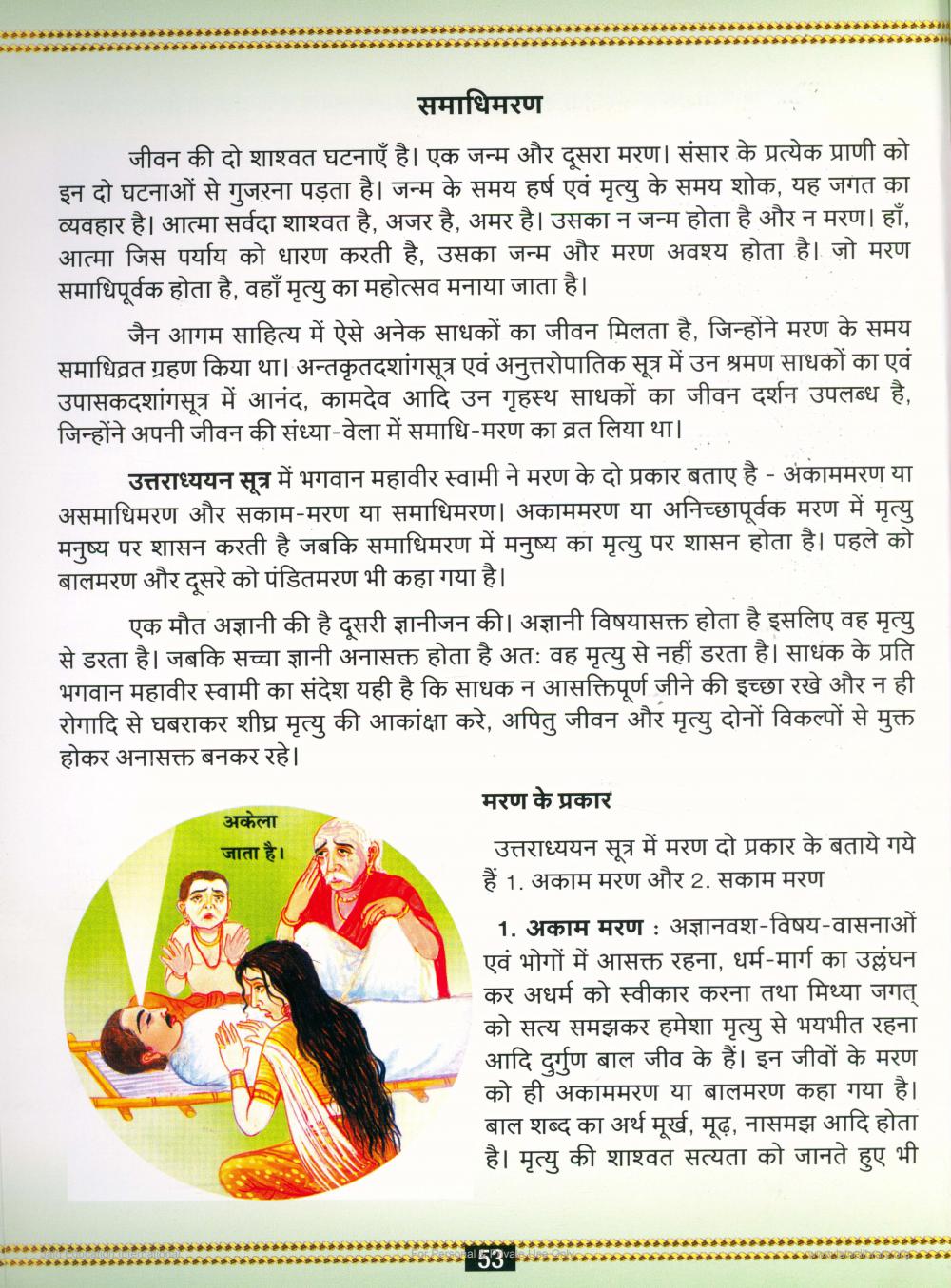________________
समाधिमरण जीवन की दो शाश्वत घटनाएँ है। एक जन्म और दूसरा मरण। संसार के प्रत्येक प्राणी को इन दो घटनाओं से गुजरना पड़ता है। जन्म के समय हर्ष एवं मृत्यु के समय शोक, यह जगत का व्यवहार है। आत्मा सर्वदा शाश्वत है, अजर है, अमर है। उसका न जन्म होता है और न मरण। हाँ, आत्मा जिस पर्याय को धारण करती है, उसका जन्म और मरण अवश्य होता है। जो मरण समाधिपूर्वक होता है, वहाँ मृत्यु का महोत्सव मनाया जाता है।
जैन आगम साहित्य में ऐसे अनेक साधकों का जीवन मिलता है, जिन्होंने मरण के समय समाधिव्रत ग्रहण किया था। अन्तकृतदशांगसूत्र एवं अनुत्तरोपातिक सूत्र में उन श्रमण साधकों का एवं उपासकदशांगसूत्र में आनंद, कामदेव आदि उन गृहस्थ साधकों का जीवन दर्शन उपलब्ध है, जिन्होंने अपनी जीवन की संध्या-वेला में समाधि-मरण का व्रत लिया था।
उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने मरण के दो प्रकार बताए है - अंकाममरण या असमाधिमरण और सकाम-मरण या समाधिमरण। अकाममरण या अनिच्छापूर्वक मरण में मृत्यु मनुष्य पर शासन करती है जबकि समाधिमरण में मनुष्य का मृत्यु पर शासन होता है। पहले को बालमरण और दूसरे को पंडितमरण भी कहा गया है।
एक मौत अज्ञानी की है दूसरी ज्ञानीजन की। अज्ञानी विषयासक्त होता है इसलिए वह मृत्यु से डरता है। जबकि सच्चा ज्ञानी अनासक्त होता है अत: वह मृत्यु से नहीं डरता है। साधक के प्रति भगवान महावीर स्वामी का संदेश यही है कि साधक न आसक्तिपूर्ण जीने की इच्छा रखे और न ही रोगादि से घबराकर शीघ्र मृत्यु की आकांक्षा करे, अपितु जीवन और मृत्यु दोनों विकल्पों से मुक्त होकर अनासक्त बनकर रहे।
मरण के प्रकार अकेला जाता है।
उत्तराध्ययन सूत्र में मरण दो प्रकार के बताये गये हैं 1. अकाम मरण और 2. सकाम मरण
1. अकाम मरण : अज्ञानवश-विषय-वासनाओं एवं भोगों में आसक्त रहना, धर्म-मार्ग का उल्लंघन कर अधर्म को स्वीकार करना तथा मिथ्या जगत् को सत्य समझकर हमेशा मृत्यु से भयभीत रहना आदि दुर्गुण बाल जीव के हैं। इन जीवों के मरण को ही अकाममरण या बालमरण कहा गया है। बाल शब्द का अर्थ मूर्ख, मूढ़, नासमझ आदि होता है। मृत्यु की शाश्वत सत्यता को जानते हुए भी
al53val