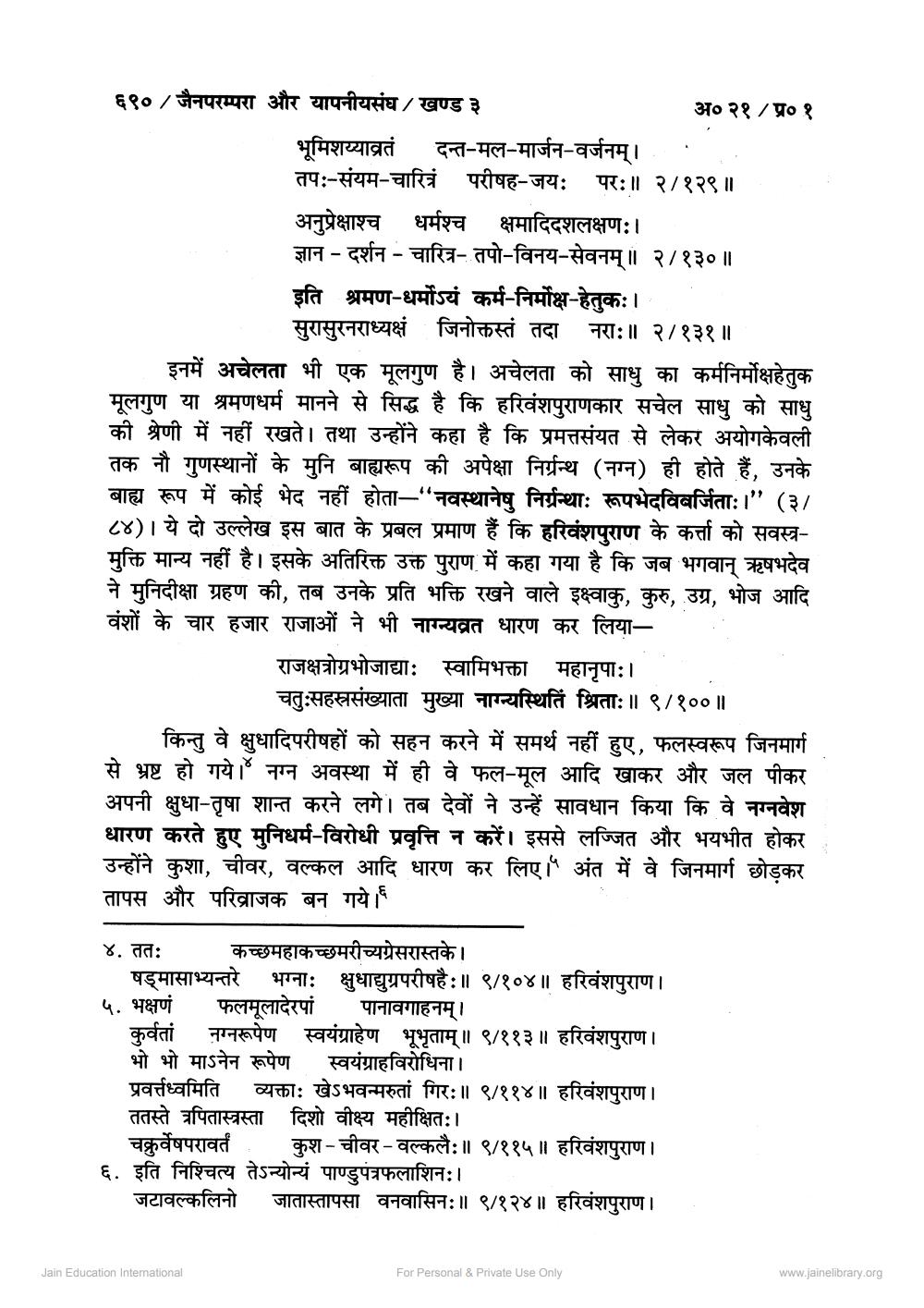________________
६९० / जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड ३
अ०२१/प्र०१ भूमिशय्याव्रतं दन्त-मल-मार्जन-वर्जनम्। तपः-संयम-चारित्रं परीषह-जयः परः॥ २/१२९ ॥ अनुप्रेक्षाश्च धर्मश्च क्षमादिदशलक्षणः। ज्ञान - दर्शन - चारित्र- तपो-विनय-सेवनम्॥ २/१३० ॥ इति श्रमण-धर्मोऽयं कर्म-निर्मोक्ष-हेतकः।
सुरासुरनराध्यक्षं जिनोक्तस्तं तदा नराः॥ २/१३१॥ इनमें अचेलता भी एक मूलगुण है। अचेलता को साधु का कर्मनिर्मोक्षहेतुक मूलगुण या श्रमणधर्म मानने से सिद्ध है कि हरिवंशपुराणकार सचेल साधु को साधु की श्रेणी में नहीं रखते। तथा उन्होंने कहा है कि प्रमत्तसंयत से लेकर अयोगकेवली तक नौ गुणस्थानों के मुनि बाह्यरूप की अपेक्षा निर्ग्रन्थ (नग्न) ही होते हैं, उनके बाह्य रूप में कोई भेद नहीं होता-"नवस्थानेषु निर्ग्रन्थाः रूपभेदविवर्जिताः।" (३/ ८४)। ये दो उल्लेख इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि हरिवंशपुराण के कर्ता को सवस्त्रमुक्ति मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त पुराण में कहा गया है कि जब भगवान् ऋषभदेव ने मुनिदीक्षा ग्रहण की, तब उनके प्रति भक्ति रखने वाले इक्ष्वाकु, कुरु, उग्र, भोज आदि वंशों के चार हजार राजाओं ने भी नाग्न्यव्रत धारण कर लिया
राजक्षत्रोग्रभोजाद्याः स्वामिभक्ता महानृपाः।
चतुःसहस्रसंख्याता मुख्या नाग्न्यस्थितिं श्रिताः॥ ९/१०० ॥ किन्तु वे क्षुधादिपरीषहों को सहन करने में समर्थ नहीं हुए, फलस्वरूप जिनमार्ग से भ्रष्ट हो गये। नग्न अवस्था में ही वे फल-मूल आदि खाकर और जल पीकर अपनी क्षुधा-तृषा शान्त करने लगे। तब देवों ने उन्हें सावधान किया कि वे नग्नवेश धारण करते हुए मुनिधर्म-विरोधी प्रवृत्ति न करें। इससे लज्जित और भयभीत होकर उन्होंने कुशा, चीवर, वल्कल आदि धारण कर लिए। अंत में वे जिनमार्ग छोड़कर तापस और परिव्राजक बन गये।
४. ततः कच्छमहाकच्छमरीच्यग्रेसरास्तके। __ षड्मासाभ्यन्तरे भग्नाः क्षुधाधुग्रपरीषहै:॥ ९/१०४॥ हरिवंशपुराण। ५. भक्षणं फलमूलादेरपां पानावगाहनम्।
कुर्वतां नग्नरूपेण स्वयंग्राहेण भूभृताम्॥ ९/११३॥ हरिवंशपुराण। भो भो माऽनेन रूपेण स्वयंग्राहविरोधिना। प्रवर्तध्वमिति व्यक्ताः खेऽभवन्मरुतां गिरः॥ ९/११४ ॥ हरिवंशपुराण। ततस्ते त्रपितास्त्रस्ता दिशो वीक्ष्य महीक्षितः।
चक्रुर्वेषपरावर्तं कुश-चीवर - वल्कलैः॥ ९/११५॥ हरिवंशपुराण। ६. इति निश्चित्य तेऽन्योन्यं पाण्डुपंत्रफलाशिनः।
जटावल्कलिनो जातास्तापसा वनवासिनः॥ ९/१२४॥ हरिवंशपुराण।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org