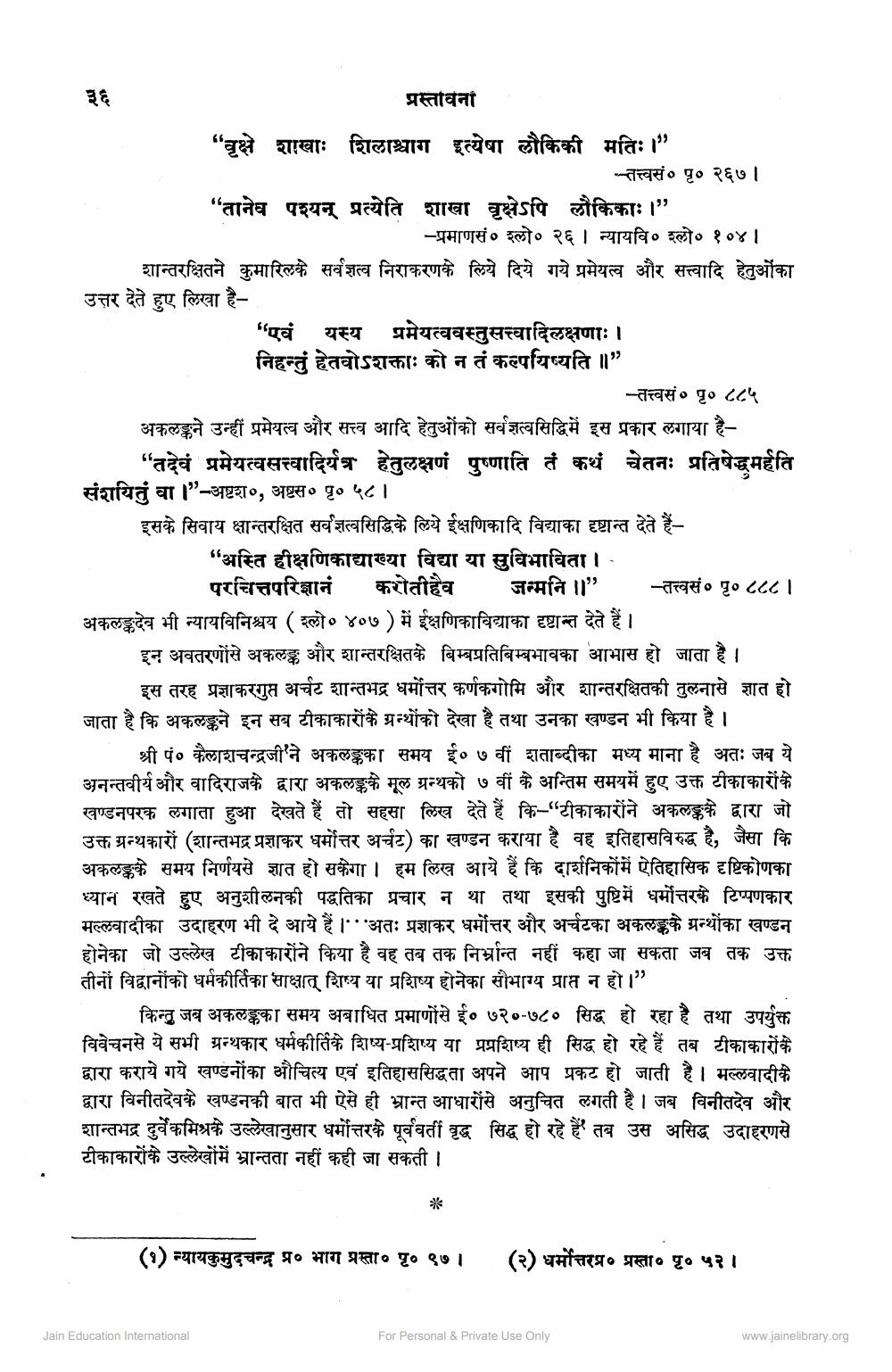________________
३६
प्रस्तावना
"वृक्षे शाखाः शिलाश्चाग इत्येषा लौकिकी मतिः ।"
-तत्त्वसं० पृ० २६७ । " तानेव पश्यन् प्रत्येति शाखा वृक्षेऽपि लौकिकाः । " - प्रमाणसं ० श्लो० २६ । न्यायवि० श्लो० १०४ । शान्तरक्षितने कुमारिलके सर्वज्ञत्व निराकरणके लिये दिये गये प्रमेयत्व और सत्त्वादि हेतुओंका उत्तर देते हुए लिखा है
"एवं यस्य प्रमेयत्ववस्तुसत्त्वादिलक्षणाः । निहन्तुं तवोऽशक्ताः को न तं कल्पयिष्यति ॥ "
- तत्त्वसं ० पृ० ८८५
अकलङ्कने उन्हीं प्रमेयत्व और सत्त्व आदि हेतुओंको सर्वज्ञत्वसिद्धि में इस प्रकार लगाया है“तदेवं प्रमेयत्वसत्त्वादिर्यत्र हेतुलक्षणं पुष्णाति तं कथं चेतनः प्रतिषेद्धुमर्हति संशयितुं वा । " - अष्टश०, अष्टस० पृ० ५८ ।
इसके सिवाय क्षान्तरक्षित सर्वज्ञत्वसिद्धिके लिये ईक्षणिकादि विद्याका दृष्टान्त देते हैं"अस्ति ही क्षणिकाद्याख्या विद्या या सुविभाविता । - परचित्तपरिज्ञानं करोतीहैव जन्मनि ॥ "
अकलङ्कदेव भी न्यायविनिश्चय ( श्लो० ४०७ ) में ईक्षणिकाविद्याका दृष्टान्त देते हैं ।
इन अवतरणोंसे अकलङ्क और शान्तरक्षितके बिम्बप्रतिबिम्बभावका आभास हो जाता है । इस तरह प्रज्ञाकरगुप्त अर्चट शान्तभद्र धर्मोत्तर कर्णकगोमि और शान्तरक्षितकी तुलनासे ज्ञात हो जाता है कि अलङ्कने इन सब टीकाकारों के ग्रन्थोंको देखा है तथा उनका खण्डन भी किया है।
1
श्री पं० कैलाशचन्द्रजी' ने अकलङ्कका समय ई० ७ वीं शताब्दीका मध्य माना है अतः जब ये अनन्तवीर्य और वादिराजके द्वारा अकलङ्कके मूल ग्रन्थको ७ वीं के अन्तिम समय में हुए उक्त टीकाकारों के खण्डनपरक लगाता हुआ देखते हैं तो सहसा लिख देते हैं कि - " टीकाकारोंने अकलङ्कके द्वारा जो उक्त ग्रन्थकारों (शान्तभद्र प्रज्ञाकर धर्मोत्तर अर्चट ) का खण्डन कराया है वह इतिहासविरुद्ध है, जैसा कि अकलङ्कके समय निर्णय से ज्ञात हो सकेगा । हम लिख आये हैं कि दार्शनिकों में ऐतिहासिक दृष्टिकोणका ध्यान रखते हुए अनुशीलनकी पद्धतिका प्रचार न था तथा इसकी पुष्टि में धर्मोत्तरके टिप्पणकार मल्लवादीका उदाहरण भी दे आये हैं । अतः प्रज्ञाकर धर्मोत्तर और अर्चटका अकलङ्कके ग्रन्थोंका खण्डन होनेका जो उल्लेख टीकाकारोंने किया है वह तब तक निर्भ्रान्त नहीं कहा जा सकता जब तक उक्त तीनों विद्वानोंको धर्मकीर्तिका साक्षात् शिष्य या प्रशिष्य होनेका सौभाग्य प्राप्त न हो ।”
Jain Education International
-तत्त्वसं० पृ० ८८८ ।
किन्तु जब अकलङ्कका समय अबाधित प्रमाणोंसे ई० ७२०-७८० सिद्ध रहा है तथा उपर्युक्त विवेचनसे ये सभी ग्रन्थकार धर्मकीर्तिके शिष्य-प्रशिष्य या प्रप्रशिष्य ही सिद्ध हो रहे हैं तब टीकाकारों के द्वारा कराये गये खण्डनोंका औचित्य एवं इतिहाससिद्धता अपने आप प्रकट हो जाती है । मल्लवादीके द्वारा विनीतदेवके खण्डनकी बात भी ऐसे ही भ्रान्त आधारोंसे अनुचित लगती है । जब विनीतदेव और शान्तभद्र दुर्वेकमिश्रके उल्लेखानुसार धर्मोत्तर के पूर्ववर्ती वृद्ध सिद्ध हो रहे हैं तब उस असिद्ध उदाहरणसे टीकाकारों के उल्लेखों में भ्रान्तता नहीं कही जा सकती ।
(१) न्यायकुमुदचन्द्र प्र० भाग प्रस्ता० पृ० ९७ ।
(२) धर्मोत्तर प्र० प्रस्ता० पृ० ५२ ।
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org