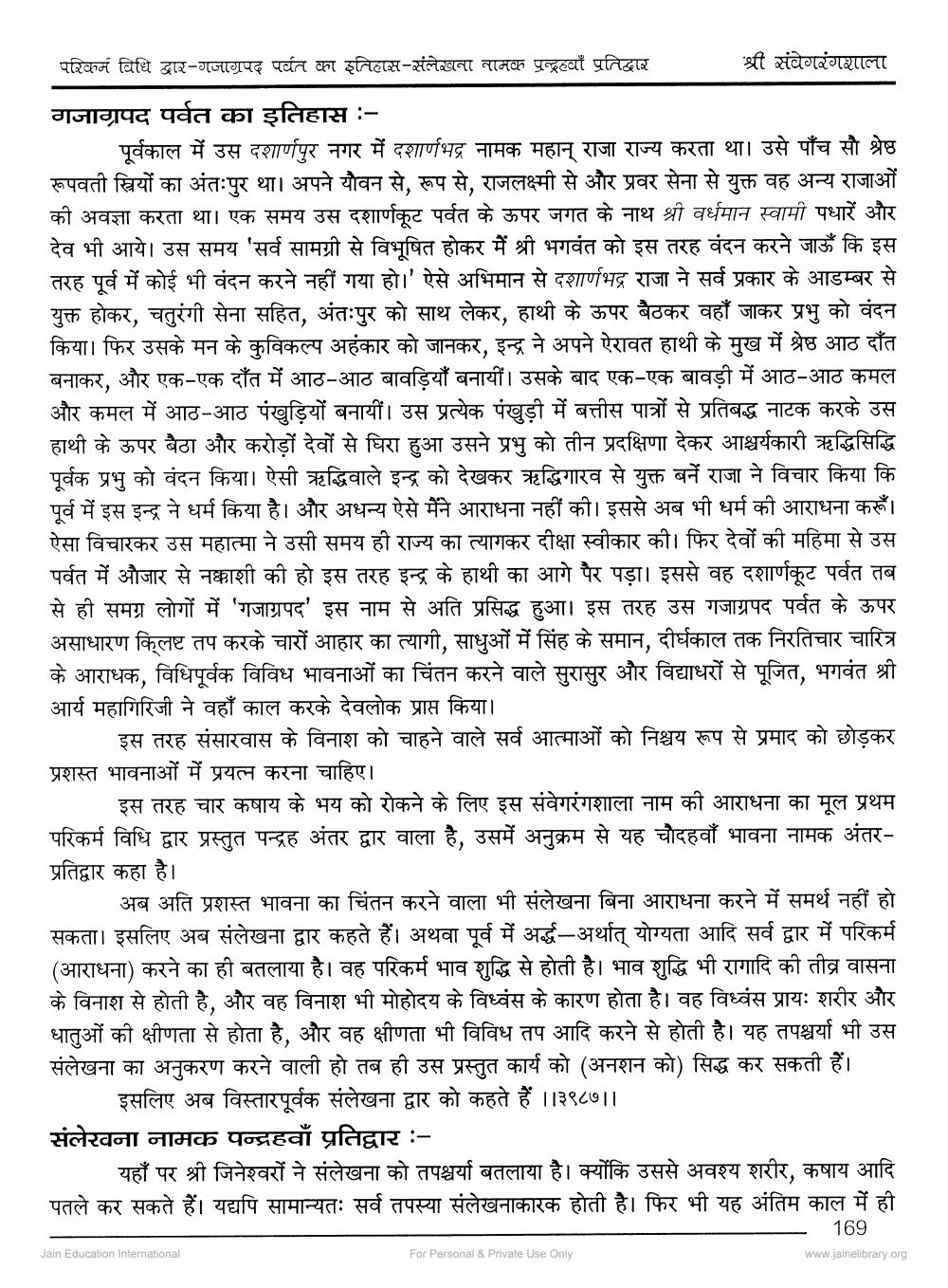________________
परिकम विधि द्वार-गजाग्रपद पर्वत का इतिहास-संलेखना नामक प्रन्द्रहवाँ प्रतिद्धार
श्री संवेगरंगशाला
गजाग्रपद पर्वत का इतिहास :
पूर्वकाल में उस दशार्णपुर नगर में दशार्णभद्र नामक महान् राजा राज्य करता था। उसे पाँच सौ श्रेष्ठ रूपवती स्त्रियों का अंतःपुर था। अपने यौवन से, रूप से, राजलक्ष्मी से और प्रवर सेना से युक्त वह अन्य राजाओं की अवज्ञा करता था। एक समय उस दशार्णकूट पर्वत के ऊपर जगत के नाथ श्री वर्धमान स्वामी पधारें और देव भी आये। उस समय 'सर्व सामग्री से विभूषित होकर मैं श्री भगवंत को इस तरह वंदन करने जाऊँ कि इस तरह पूर्व में कोई भी वंदन करने नहीं गया हो।' ऐसे अभिमान से दशार्णभद्र राजा ने सर्व प्रकार के आडम्बर से युक्त होकर, चतुरंगी सेना सहित, अंतःपुर को साथ लेकर, हाथी के ऊपर बैठकर वहाँ जाकर प्रभु को वंदन किया। फिर उसके मन के कुविकल्प अहंकार को जानकर, इन्द्र ने अपने ऐरावत हाथी के मुख में श्रेष्ठ आठ दाँत बनाकर, और एक-एक दाँत में आठ-आठ बावड़ियाँ बनायीं। उसके बाद एक-एक बावड़ी में आठ-आठ कमल
और कमल में आठ-आठ पंखुड़ियों बनायीं। उस प्रत्येक पंखुड़ी में बत्तीस पात्रों से प्रतिबद्ध नाटक करके उस हाथी के ऊपर बैठा और करोड़ों देवों से घिरा हुआ उसने प्रभु को तीन प्रदक्षिणा देकर आश्चर्यकारी ऋद्धिसिद्धि पूर्वक प्रभु को वंदन किया। ऐसी ऋद्धिवाले इन्द्र को देखकर ऋद्धिगारव से युक्त बनें राजा ने विचार किया कि पूर्व में इस इन्द्र ने धर्म किया है। और अधन्य ऐसे मैंने आराधना नहीं की। इससे अब भी धर्म की आराधना करूँ। ऐसा विचारकर उस महात्मा ने उसी समय ही राज्य का त्यागकर दीक्षा स्वीकार की। फिर देवों की महिमा से उस पर्वत में औजार से नक्काशी की हो इस तरह इन्द्र के हाथी का आगे पैर पड़ा। इससे वह दशार्णकूट पर्वत तब से ही समग्र लोगों में 'गजाग्रपद' इस नाम से अति प्रसिद्ध हुआ। इस तरह उस गजाग्रपद पर्वत के ऊपर असाधारण क्लिष्ट तप करके चारों आहार का त्यागी, साधुओं में सिंह के समान, दीर्घकाल तक निरतिचार चारित्र के आराधक, विधिपूर्वक विविध भावनाओं का चिंतन करने वाले सुरासुर और विद्याधरों से पूजित, भगवंत श्री आर्य महागिरिजी ने वहाँ काल करके देवलोक प्राप्त किया।
इस तरह संसारवास के विनाश को चाहने वाले सर्व आत्माओं को निश्चय रूप से प्रमाद को छोड़कर प्रशस्त भावनाओं में प्रयत्न करना चाहिए।
इस तरह चार कषाय के भय को रोकने के लिए इस संवेगरंगशाला नाम की आराधना का मूल प्रथम परिकर्म विधि द्वार प्रस्तुत पन्द्रह अंतर द्वार वाला है, उसमें अनुक्रम से यह चौदहवाँ भावना नामक अंतरप्रतिद्वार कहा है।
अब अति प्रशस्त भावना का चिंतन करने वाला भी संलेखना बिना आराधना करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए अब संलेखना द्वार कहते हैं। अथवा पूर्व में अर्द्ध-अर्थात् योग्यता आदि सर्व द्वार में परिकर्म (आराधना) करने का ही बतलाया है। वह परिकर्म भाव शुद्धि से होती है। भाव शुद्धि भी रागादि की तीव्र वासना के विनाश से होती है, और वह विनाश भी मोहोदय के विध्वंस के कारण होता है। वह विध्वंस प्रायः शरीर और धातुओं की क्षीणता से होता है, और वह क्षीणता भी विविध तप आदि करने से होती है। यह तपश्चर्या भी उस संलेखना का अनुकरण करने वाली हो तब ही उस प्रस्तुत कार्य को (अनशन को) सिद्ध कर सकती हैं।
इसलिए अब विस्तारपूर्वक संलेखना द्वार को कहते हैं ।।३९८७।। संलेखना नामक पन्द्रहवाँ प्रतिद्वार :
यहाँ पर श्री जिनेश्वरों ने संलेखना को तपश्चर्या बतलाया है। क्योंकि उससे अवश्य शरीर, कषाय आदि पतले कर सकते हैं। यद्यपि सामान्यतः सर्व तपस्या संलेखनाकारक होती है। फिर भी यह अंतिम काल में ही
169
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org