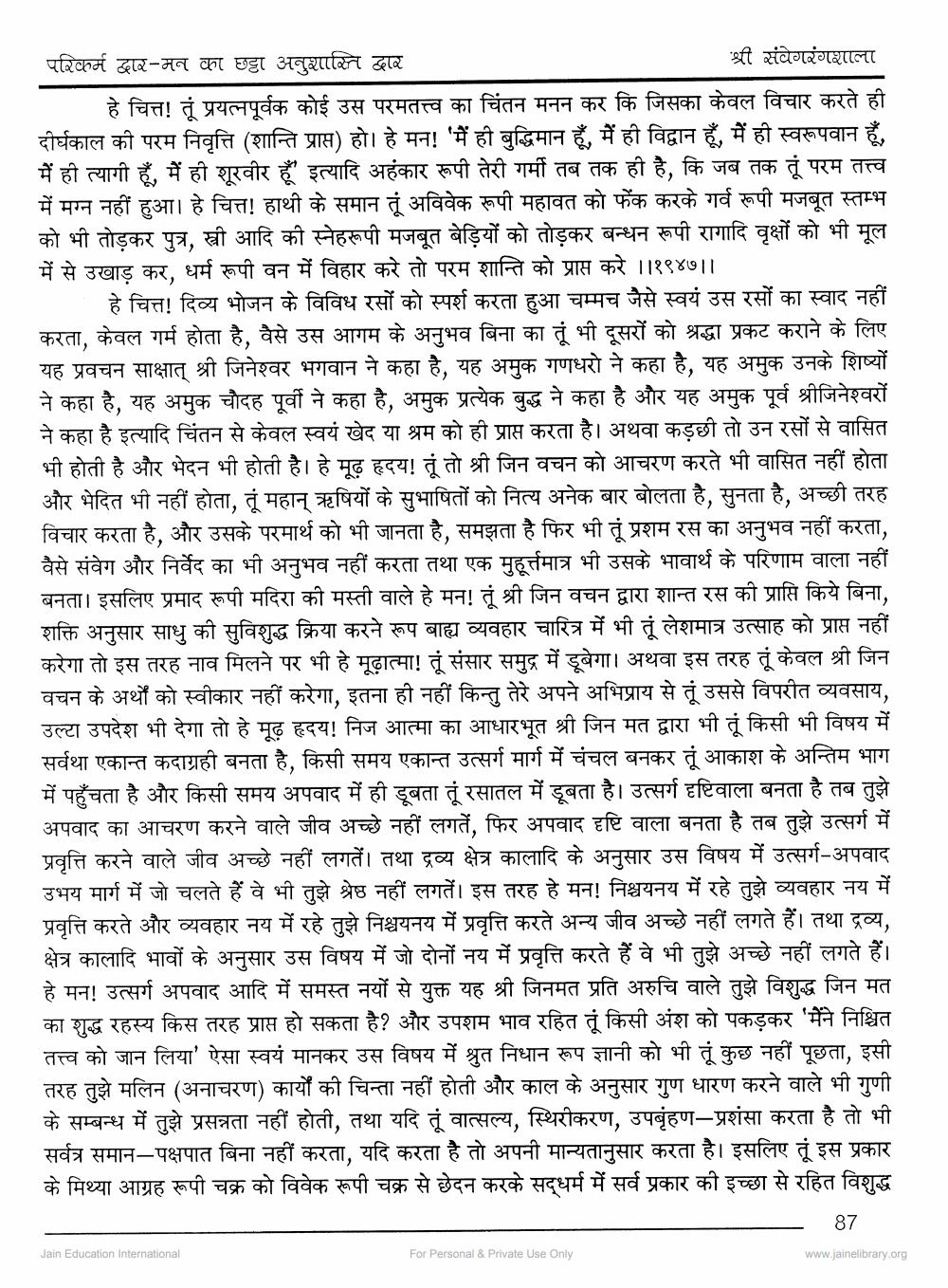________________
परिकर्म द्वार - मन का छट्टा अनुशास्ति द्वार
श्री संवेगरंगशाला
हे चित्त! तूं प्रयत्नपूर्वक कोई उस परमतत्त्व का चिंतन मनन कर कि जिसका केवल विचार करते ही दीर्घकाल की परम निवृत्ति (शान्ति प्राप्त) हो । हे मन ! 'मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही स्वरूपवान हूँ, मैं ही त्यागी हूँ, मैं ही शूरवीर हूँ' इत्यादि अहंकार रूपी तेरी गर्मी तब तक ही है, कि जब तक तूं परम तत्त्व में मग्न नहीं हुआ। हे चित्त ! हाथी के समान तूं अविवेक रूपी महावत को फेंक करके गर्व रूपी मजबूत स्तम्भ को भी तोड़कर पुत्र, स्त्री आदि की स्नेहरूपी मजबूत बेड़ियों को तोड़कर बन्धन रूपी रागादि वृक्षों को भी मूल में से उखाड़ कर, धर्म रूपी वन में विहार करे तो परम शान्ति को प्राप्त करे । । १९४७ ।।
हे चित्त ! दिव्य भोजन के विविध रसों को स्पर्श करता हुआ चम्मच जैसे स्वयं उस रसों का स्वाद नहीं करता, केवल गर्म होता है, वैसे उस आगम के अनुभव बिना का तूं भी दूसरों को श्रद्धा प्रकट कराने के लिए यह प्रवचन साक्षात् श्री जिनेश्वर भगवान ने कहा है, यह अमुक गणधरो ने कहा है, यह अमुक उनके शिष्यों ने कहा है, यह अमुक चौदह पूर्वी ने कहा है, अमुक प्रत्येक बुद्ध ने कहा है और यह अमुक पूर्व श्रीजिनेश्वरों ने कहा है इत्यादि चिंतन से केवल स्वयं खेद या श्रम को ही प्राप्त करता है। अथवा कड़छी तो उन रसों से वासित भी होती है और भेदन भी होती है। हे मूढ़ हृदय ! तूं तो श्री जिन वचन को आचरण करते भी वासित नहीं होता और भेदित भी नहीं होता, तूं महान् ऋषियों के सुभाषितों को नित्य अनेक बार बोलता है, सुनता है, अच्छी तरह विचार करता है, और उसके परमार्थ को भी जानता है, समझता है फिर भी तूं प्रशम रस का अनुभव नहीं करता, वैसे संवेग और निर्वेद का भी अनुभव नहीं करता तथा एक मुहूर्त्तमात्र भी उसके भावार्थ के परिणाम वाला नहीं बनता। इसलिए प्रमाद रूपी मदिरा की मस्ती वाले हे मन! तूं श्री जिन वचन द्वारा शान्त रस की प्राप्ति किये बिना, शक्ति अनुसार साधु की सुविशुद्ध क्रिया करने रूप बाह्य व्यवहार चारित्र में भी तूं लेशमात्र उत्साह को प्राप्त नहीं करेगा तो इस तरह नाव मिलने पर भी हे मूढात्मा ! तूं संसार समुद्र में डूबेगा । अथवा इस तरह तूं केवल श्री जिन वचन के अर्थों को स्वीकार नहीं करेगा, इतना ही नहीं किन्तु तेरे अपने अभिप्राय से तूं उससे विपरीत व्यवसाय, उल्टा उपदेश भी देगा तो हे मूढ़ हृदय ! निज आत्मा का आधारभूत श्री जिन मत द्वारा भी तूं किसी भी विषय में सर्वथा एकान्त कदाग्रही बनता है, किसी समय एकान्त उत्सर्ग मार्ग में चंचल बनकर तूं आकाश के अन्तिम भाग में पहुँचता है और किसी समय अपवाद में ही डूबता तूं रसातल में डूबता है। उत्सर्ग दृष्टिवाला बनता है तब तुझे अपवाद का आचरण करने वाले जीव अच्छे नहीं लगतें, फिर अपवाद दृष्टि वाला बनता है तब तुझे उत्सर्ग में प्रवृत्ति करने वाले जीव अच्छे नहीं लगतें । तथा द्रव्य क्षेत्र कालादि के अनुसार उस विषय में उत्सर्ग-अपवाद उभय मार्ग में जो चलते हैं वे भी तुझे श्रेष्ठ नहीं लगतें । इस तरह हे मन! निश्चयनय में रहे तुझे व्यवहार नय में प्रवृत्ति करते और व्यवहार नय में रहे तुझे निश्चयनय में प्रवृत्ति करते अन्य जीव अच्छे नहीं लगते हैं। तथा द्रव्य, क्षेत्र कालादि भावों के अनुसार उस विषय में जो दोनों नय में प्रवृत्ति करते हैं वे भी तुझे अच्छे नहीं लगते हैं। हे मन! उत्सर्ग अपवाद आदि में समस्त नयों से युक्त यह श्री जिनमत प्रति अरुचि वाले तुझे विशुद्ध जिन मत का शुद्ध रहस्य किस तरह प्राप्त हो सकता है? और उपशम भाव रहित तूं किसी अंश को पकड़कर 'मैंने निश्चित तत्त्व को जान लिया' ऐसा स्वयं मानकर उस विषय में श्रुत निधान रूप ज्ञानी को भी तूं कुछ नहीं पूछता, इसी तरह तुझे मलिन (अनाचरण) कार्यों की चिन्ता नहीं होती और काल के अनुसार गुण धारण करने वाले भी गुणी के सम्बन्ध में तुझे प्रसन्नता नहीं होती, तथा यदि तूं वात्सल्य, स्थिरीकरण, उपबृंहण - प्रशंसा करता है तो भी सर्वत्र समान - पक्षपात बिना नहीं करता, यदि करता है तो अपनी मान्यतानुसार करता है। इसलिए तूं इस प्रकार के मिथ्या आग्रह रूपी चक्र को विवेक रूपी चक्र से छेदन करके सद्धर्म में सर्व प्रकार की इच्छा से रहित विशुद्ध
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
87 www.jainelibrary.org