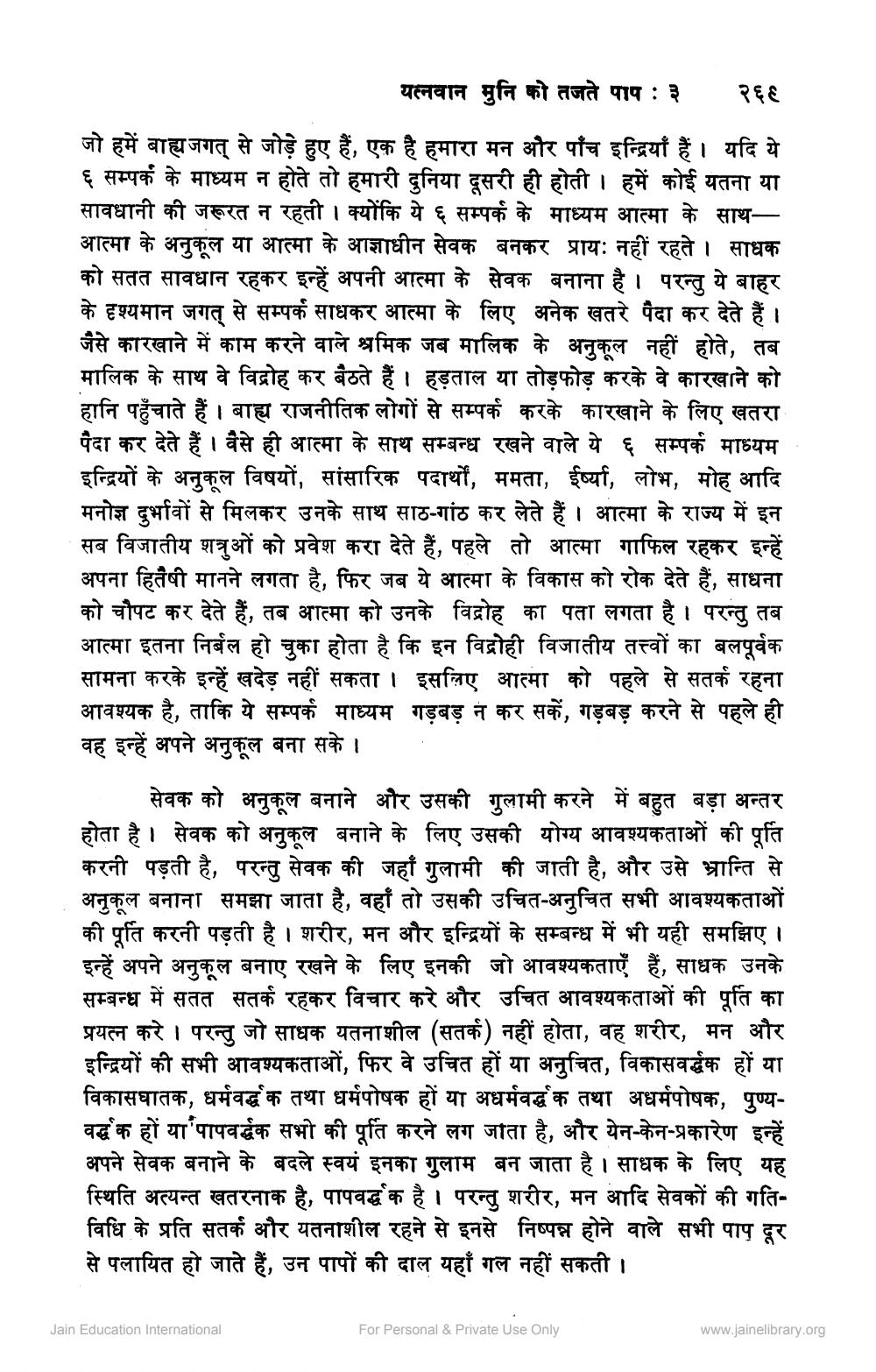________________
यत्नवान मुनि को तजते पाप : ३
२६६
जो हमें बाह्य जगत् से जोड़े हुए हैं, एक है हमारा मन और पाँच इन्द्रियाँ हैं। यदि ये ६ सम्पर्क के माध्यम न होते तो हमारी दुनिया दूसरी ही होती। हमें कोई यतना या सावधानी की जरूरत न रहती। क्योंकि ये ६ सम्पर्क के माध्यम आत्मा के साथआत्मा के अनुकूल या आत्मा के आज्ञाधीन सेवक बनकर प्रायः नहीं रहते। साधक को सतत सावधान रहकर इन्हें अपनी आत्मा के सेवक बनाना है। परन्तु ये बाहर के दृश्यमान जगत् से सम्पर्क साधकर आत्मा के लिए अनेक खतरे पैदा कर देते हैं। जैसे कारखाने में काम करने वाले श्रमिक जब मालिक के अनुकूल नहीं होते, तब मालिक के साथ वे विद्रोह कर बैठते हैं। हड़ताल या तोड़फोड़ करके वे कारखाने को हानि पहुँचाते हैं। बाह्य राजनीतिक लोगों से सम्पर्क करके कारखाने के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। वैसे ही आत्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले ये ६ सम्पर्क माध्यम इन्द्रियों के अनुकूल विषयों, सांसारिक पदार्थों, ममता, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि मनोज्ञ दुर्भावों से मिलकर उनके साथ साठ-गांठ कर लेते हैं। आत्मा के राज्य में इन सब विजातीय शत्रुओं को प्रवेश करा देते हैं, पहले तो आत्मा गाफिल रहकर इन्हें अपना हितैषी मानने लगता है, फिर जब ये आत्मा के विकास को रोक देते हैं, साधना को चौपट कर देते हैं, तब आत्मा को उनके विद्रोह का पता लगता है। परन्तु तब आत्मा इतना निर्बल हो चुका होता है कि इन विद्रोही विजातीय तत्त्वों का बलपूर्वक सामना करके इन्हें खदेड़ नहीं सकता। इसलिए आत्मा को पहले से सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि ये सम्पर्क माध्यम गड़बड़ न कर सकें, गड़बड़ करने से पहले ही वह इन्हें अपने अनुकूल बना सके।
सेवक को अनुकूल बनाने और उसकी गुलामी करने में बहुत बड़ा अन्तर होता है। सेवक को अनुकूल बनाने के लिए उसकी योग्य आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, परन्तु सेवक की जहाँ गुलामी की जाती है, और उसे भ्रान्ति से अनुकूल बनाना समझा जाता है, वहाँ तो उसकी उचित-अनुचित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है । शरीर, मन और इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी यही समझिए । इन्हें अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए इनकी जो आवश्यकताएँ हैं, साधक उनके सम्बन्ध में सतत सतर्क रहकर विचार करे और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करे । परन्तु जो साधक यतनाशील (सतर्क) नहीं होता, वह शरीर, मन और इन्द्रियों की सभी आवश्यकताओं, फिर वे उचित हों या अनुचित, विकासवर्द्धक हों या विकासघातक, धर्मवर्द्धक तथा धर्मपोषक हों या अधर्मवद्धक तथा अधर्मपोषक, पुण्यवर्द्धक हों या पापवर्द्धक सभी की पूर्ति करने लग जाता है, और येन-केन-प्रकारेण इन्हें अपने सेवक बनाने के बदले स्वयं इनका गुलाम बन जाता है। साधक के लिए यह स्थिति अत्यन्त खतरनाक है, पापवर्द्धक है। परन्तु शरीर, मन आदि सेवकों की गतिविधि के प्रति सतर्क और यतनाशील रहने से इनसे निष्पन्न होने वाले सभी पाप दूर से पलायित हो जाते हैं, उन पापों की दाल यहाँ गल नहीं सकती।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org