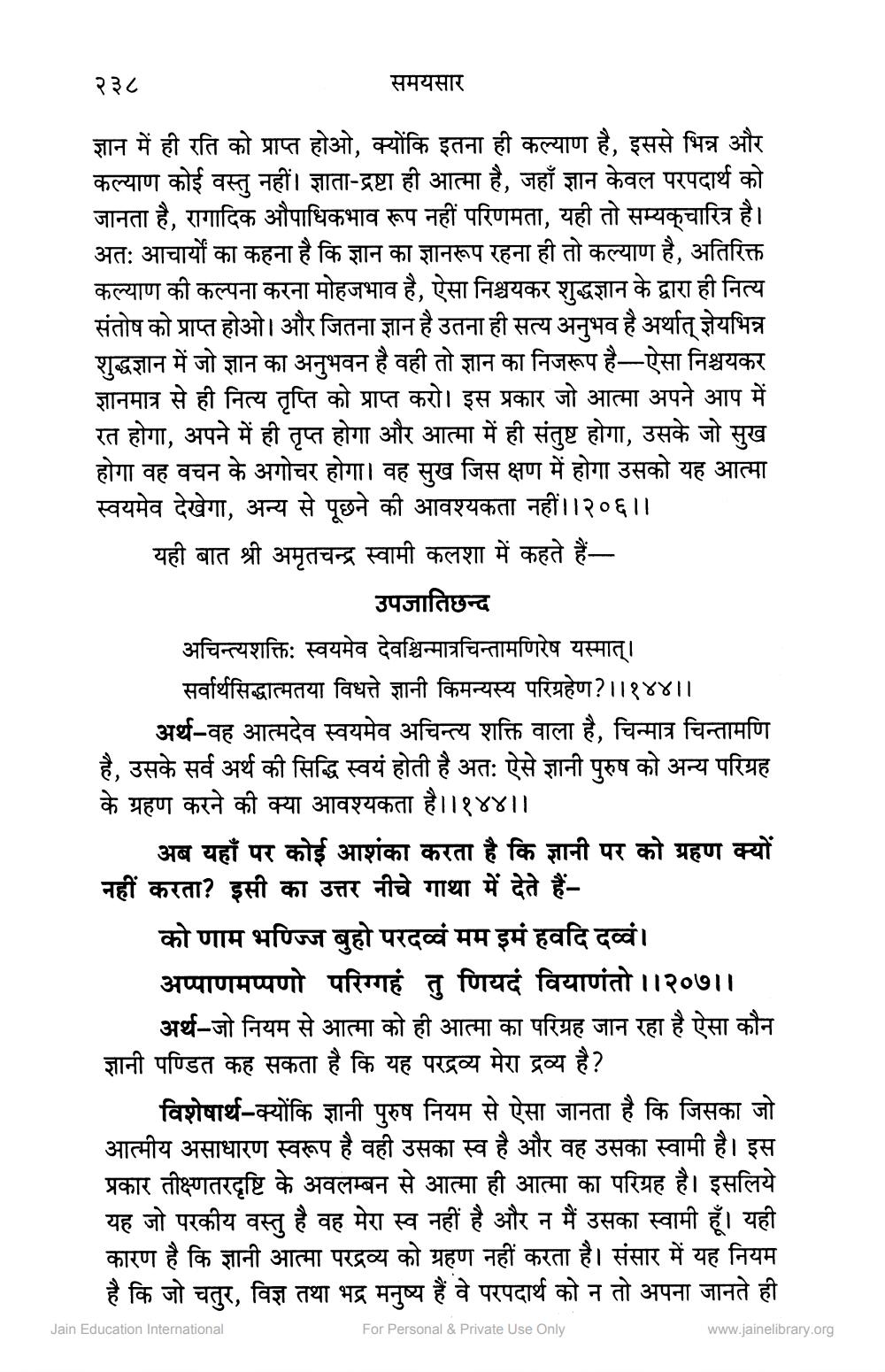________________
२३८
समयसार
ज्ञान में ही रति को प्राप्त होओ, क्योंकि इतना ही कल्याण है, इससे भिन्न और कल्याण कोई वस्तु नहीं। ज्ञाता-द्रष्टा ही आत्मा है, जहाँ ज्ञान केवल परपदार्थ को जानता है, रागादिक औपाधिकभाव रूप नहीं परिणमता, यही तो सम्यक्चारित्र है। अत: आचार्यों का कहना है कि ज्ञान का ज्ञानरूप रहना ही तो कल्याण है, अतिरिक्त कल्याण की कल्पना करना मोहजभाव है, ऐसा निश्चयकर शुद्धज्ञान के द्वारा ही नित्य संतोष को प्राप्त होओ। और जितना ज्ञान है उतना ही सत्य अनुभव है अर्थात् ज्ञेयभिन्न शुद्धज्ञान में जो ज्ञान का अनुभवन है वही तो ज्ञान का निजरूप है-ऐसा निश्चयकर ज्ञानमात्र से ही नित्य तृप्ति को प्राप्त करो। इस प्रकार जो आत्मा अपने आप में रत होगा, अपने में ही तृप्त होगा और आत्मा में ही संतुष्ट होगा, उसके जो सुख होगा वह वचन के अगोचर होगा। वह सुख जिस क्षण में होगा उसको यह आत्मा स्वयमेव देखेगा, अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं।।२०६।। यही बात श्री अमृतचन्द्र स्वामी कलशा में कहते हैं
उपजातिछन्द अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात्। सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण? ।। १४४।।
अर्थ-वह आत्मदेव स्वयमेव अचिन्त्य शक्ति वाला है, चिन्मात्र चिन्तामणि है, उसके सर्व अर्थ की सिद्धि स्वयं होती है अत: ऐसे ज्ञानी पुरुष को अन्य परिग्रह के ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है।।१४४।।
अब यहाँ पर कोई आशंका करता है कि ज्ञानी पर को ग्रहण क्यों नहीं करता? इसी का उत्तर नीचे गाथा में देते हैं
को णाम भण्ज्जि बुहो परदव्वं मम इमं हवदि दव्वं। अप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु णियदं वियाणंतो।।२०७।।
अर्थ-जो नियम से आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह जान रहा है ऐसा कौन ज्ञानी पण्डित कह सकता है कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है?
विशेषार्थ-क्योंकि ज्ञानी पुरुष नियम से ऐसा जानता है कि जिसका जो आत्मीय असाधारण स्वरूप है वही उसका स्व है और वह उसका स्वामी है। इस प्रकार तीक्ष्णतरदृष्टि के अवलम्बन से आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। इसलिये यह जो परकीय वस्तु है वह मेरा स्व नहीं है और न मैं उसका स्वामी हूँ। यही कारण है कि ज्ञानी आत्मा परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता है। संसार में यह नियम है कि जो चतुर, विज्ञ तथा भद्र मनुष्य हैं वे परपदार्थ को न तो अपना जानते ही
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org