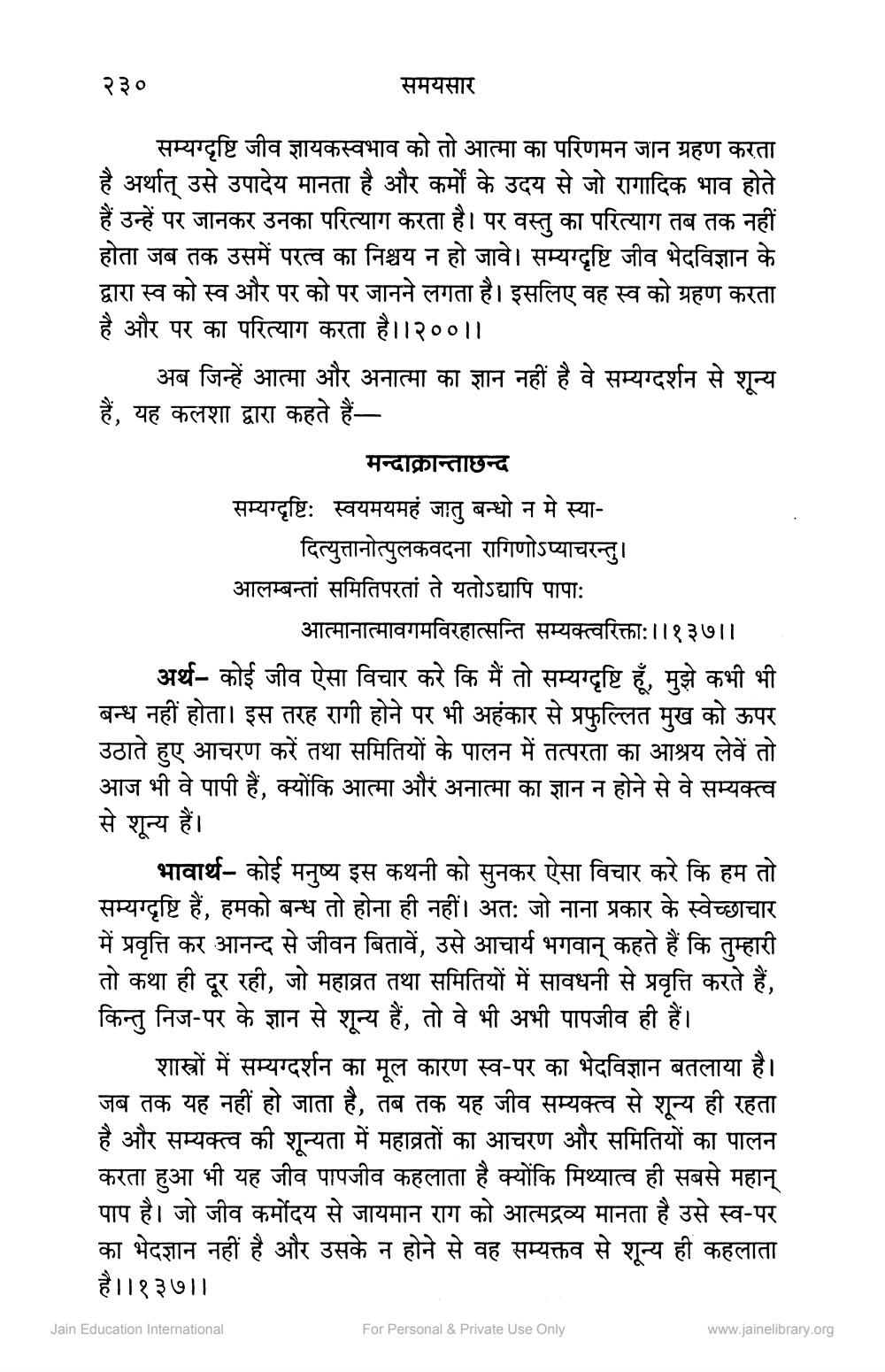________________
२३०
समयसार
__ सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञायकस्वभाव को तो आत्मा का परिणमन जान ग्रहण करता है अर्थात् उसे उपादेय मानता है और कर्मों के उदय से जो रागादिक भाव होते हैं उन्हें पर जानकर उनका परित्याग करता है। पर वस्तु का परित्याग तब तक नहीं होता जब तक उसमें परत्व का निश्चय न हो जावे। सम्यग्दृष्टि जीव भेदविज्ञान के द्वारा स्व को स्व और पर को पर जानने लगता है। इसलिए वह स्व को ग्रहण करता है और पर का परित्याग करता है।।२०।।
अब जिन्हें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है वे सम्यग्दर्शन से शून्य हैं, यह कलशा द्वारा कहते हैं
मन्दाक्रान्ताछन्द सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या
दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु। आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा:
आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः।।१३७।। अर्थ- कोई जीव ऐसा विचार करे कि मैं तो सम्यग्दृष्टि हूँ, मुझे कभी भी बन्ध नहीं होता। इस तरह रागी होने पर भी अहंकार से प्रफुल्लित मुख को ऊपर उठाते हुए आचरण करें तथा समितियों के पालन में तत्परता का आश्रय लेवें तो आज भी वे पापी हैं, क्योंकि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान न होने से वे सम्यक्त्व से शून्य हैं।
भावार्थ- कोई मनुष्य इस कथनी को सुनकर ऐसा विचार करे कि हम तो सम्यग्दृष्टि हैं, हमको बन्ध तो होना ही नहीं। अत: जो नाना प्रकार के स्वेच्छाचार में प्रवृत्ति कर आनन्द से जीवन बितावें, उसे आचार्य भगवान् कहते हैं कि तुम्हारी तो कथा ही दूर रही, जो महाव्रत तथा समितियों में सावधनी से प्रवृत्ति करते हैं, किन्तु निज-पर के ज्ञान से शून्य हैं, तो वे भी अभी पापजीव ही हैं।
शास्त्रों में सम्यग्दर्शन का मूल कारण स्व-पर का भेदविज्ञान बतलाया है। जब तक यह नहीं हो जाता है, तब तक यह जीव सम्यक्त्व से शून्य ही रहता है और सम्यक्त्व की शून्यता में महाव्रतों का आचरण और समितियों का पालन करता हुआ भी यह जीव पापजीव कहलाता है क्योंकि मिथ्यात्व ही सबसे महान् पाप है। जो जीव कर्मोदय से जायमान राग को आत्मद्रव्य मानता है उसे स्व-पर का भेदज्ञान नहीं है और उसके न होने से वह सम्यक्तव से शून्य ही कहलाता है।।१३७।।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org