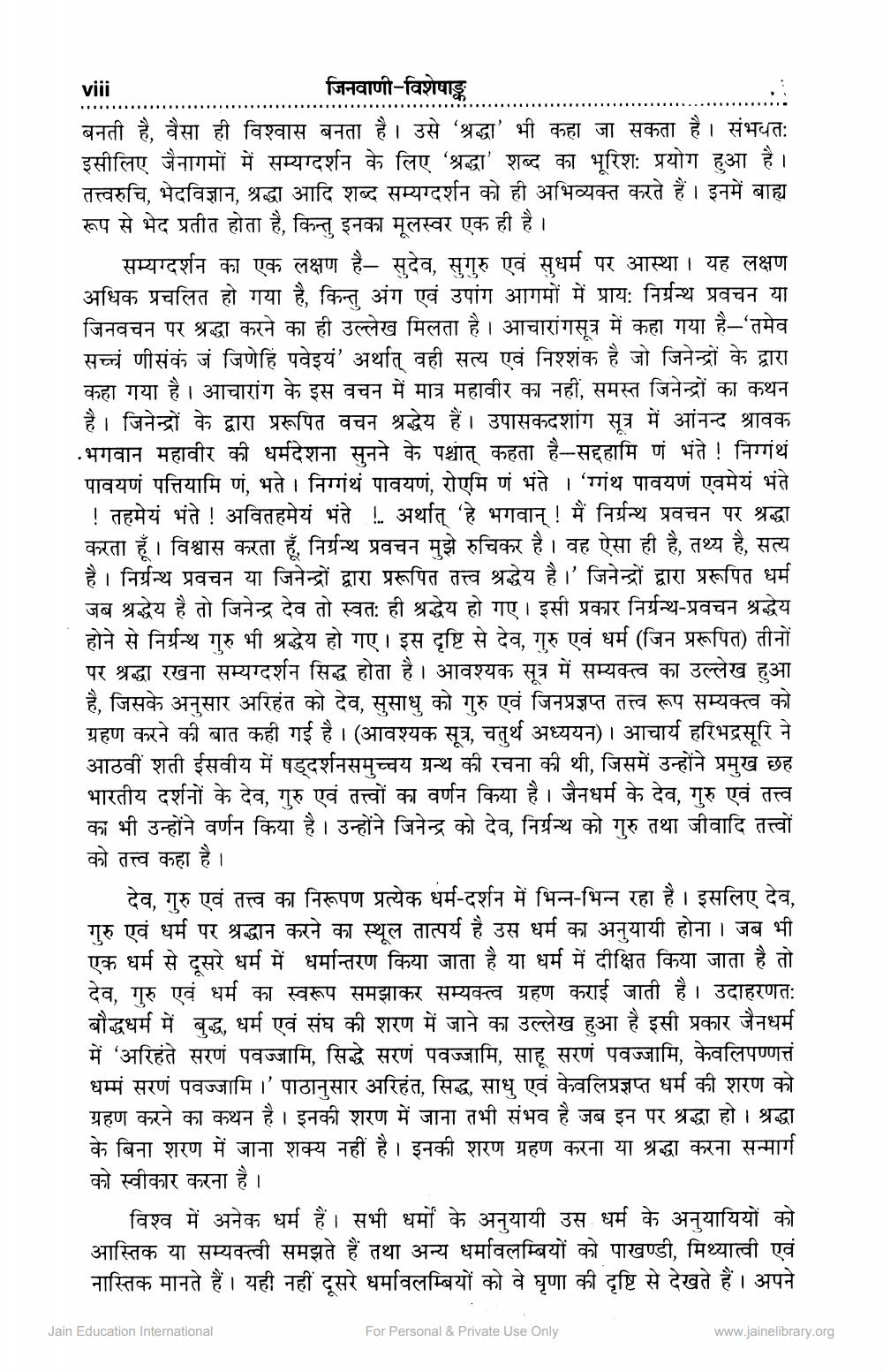________________
viii
जिनवाणी-विशेषाङ्क बनती है, वैसा ही विश्वास बनता है। उसे 'श्रद्धा' भी कहा जा सकता है। संभवत: इसीलिए जैनागमों में सम्यग्दर्शन के लिए 'श्रद्धा' शब्द का भूरिश: प्रयोग हुआ है। तत्त्वरुचि, भेदविज्ञान, श्रद्धा आदि शब्द सम्यग्दर्शन को ही अभिव्यक्त करते हैं। इनमें बाह्य रूप से भेद प्रतीत होता है, किन्तु इनका मूलस्वर एक ही है।
सम्यग्दर्शन का एक लक्षण है- सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म पर आस्था। यह लक्षण अधिक प्रचलित हो गया है, किन्तु अंग एवं उपांग आगमों में प्राय: निर्ग्रन्थ प्रवचन या जिनवचन पर श्रद्धा करने का ही उल्लेख मिलता है। आचारांगसूत्र में कहा गया है-'तमेव सच्चं णीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं' अर्थात् वही सत्य एवं निश्शंक है जो जिनेन्द्रों के द्वारा कहा गया है। आचारांग के इस वचन में मात्र महावीर का नहीं, समस्त जिनेन्द्रों का कथन है। जिनेन्द्रों के द्वारा प्ररूपित वचन श्रद्धेय हैं। उपासकदशांग सूत्र में आनन्द श्रावक .भगवान महावीर की धर्मदेशना सुनने के पश्चात् कहता है-सद्दहामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं पत्तियामि णं, भते । निग्गंथं पावयणं, रोएमि णं भंते । ‘ग्गंथ पावयणं एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! अवितहमेयं भंते !. अर्थात् 'हे भगवान् ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। विश्वास करता हूँ, निर्ग्रन्थ प्रवचन मुझे रुचिकर है। वह ऐसा ही है, तथ्य है, सत्य है। निर्ग्रन्थ प्रवचन या जिनेन्द्रों द्वारा प्ररूपित तत्त्व श्रद्धेय है।' जिनेन्द्रों द्वारा प्ररूपित धर्म जब श्रद्धेय है तो जिनेन्द्र देव तो स्वत: ही श्रद्धेय हो गए। इसी प्रकार निर्ग्रन्थ-प्रवचन श्रद्धेय होने से निर्ग्रन्थ गुरु भी श्रद्धेय हो गए। इस दृष्टि से देव, गुरु एवं धर्म (जिन प्ररूपित) तीनों पर श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन सिद्ध होता है। आवश्यक सूत्र में सम्यक्त्व का उल्लेख हुआ है, जिसके अनुसार अरिहंत को देव, सुसाधु को गुरु एवं जिनप्रज्ञप्त तत्त्व रूप सम्यक्त्व को ग्रहण करने की बात कही गई है । (आवश्यक सूत्र, चतुर्थ अध्ययन)। आचार्य हरिभद्रसूरि ने आठवीं शती ईसवीय में षड्दर्शनसमुच्चय ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने प्रमुख छह भारतीय दर्शनों के देव, गुरु एवं तत्त्वों का वर्णन किया है। जैनधर्म के देव, गुरु एवं तत्त्व का भी उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने जिनेन्द्र को देव, निम्रन्थ को गुरु तथा जीवादि तत्त्वों को तत्त्व कहा है।
देव, गुरु एवं तत्त्व का निरूपण प्रत्येक धर्म-दर्शन में भिन्न-भिन्न रहा है। इसलिए देव, गुरु एवं धर्म पर श्रद्धान करने का स्थूल तात्पर्य है उस धर्म का अनुयायी होना। जब भी एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मान्तरण किया जाता है या धर्म में दीक्षित किया जाता है तो देव, गुरु एवं धर्म का स्वरूप समझाकर सम्यक्त्व ग्रहण कराई जाती है। उदाहरणत: बौद्धधर्म में बुद्ध, धर्म एवं संघ की शरण में जाने का उल्लेख हुआ है इसी प्रकार जैनधर्म में 'अरिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्म सरणं पवज्जामि ।' पाठानुसार अरिहंत, सिद्ध, साधु एवं केवलिप्रज्ञप्त धर्म की शरण को ग्रहण करने का कथन है। इनकी शरण में जाना तभी संभव है जब इन पर श्रद्धा हो । श्रद्धा के बिना शरण में जाना शक्य नहीं है। इनकी शरण ग्रहण करना या श्रद्धा करना सन्मार्ग को स्वीकार करना है।
विश्व में अनेक धर्म हैं। सभी धर्मों के अनुयायी उस धर्म के अनुयायियों को आस्तिक या सम्यक्त्वी समझते हैं तथा अन्य धर्मावलम्बियों को पाखण्डी, मिथ्यात्वी एवं नास्तिक मानते हैं। यही नहीं दूसरे धर्मावलम्बियों को वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अपने
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org