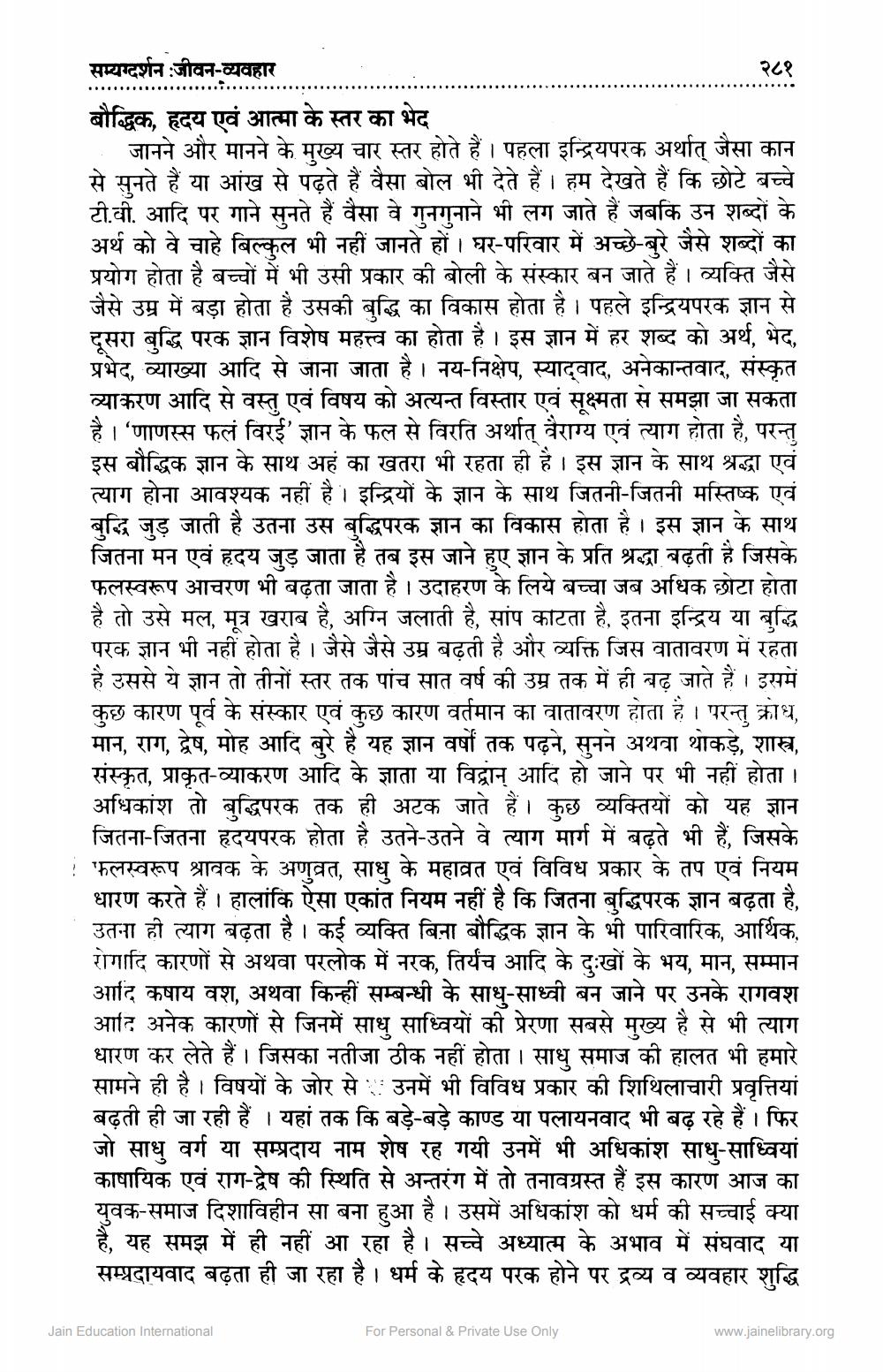________________
फलस्वर
सम्यग्दर्शन :जीवन-व्यवहार बौद्धिक, हृदय एवं आत्मा के स्तर का भेद _जानने और मानने के मुख्य चार स्तर होते हैं। पहला इन्द्रियपरक अर्थात् जैसा कान से सुनते हैं या आंख से पढ़ते हैं वैसा बोल भी देते हैं। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे टी.वी. आदि पर गाने सुनते हैं वैसा वे गुनगुनाने भी लग जाते हैं जबकि उन शब्दों के अर्थ को वे चाहे बिल्कुल भी नहीं जानते हों। घर-परिवार में अच्छे-बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है बच्चों में भी उसी प्रकार की बोली के संस्कार बन जाते हैं। व्यक्ति जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता है उसकी बुद्धि का विकास होता है। पहले इन्द्रियपरक ज्ञान से दूसरा बुद्धि परक ज्ञान विशेष महत्त्व का होता है । इस ज्ञान में हर शब्द को अर्थ, भेद, प्रभेद, व्याख्या आदि से जाना जाता है। नय-निक्षेप, स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, संस्कृत व्याकरण आदि से वस्तु एवं विषय को अत्यन्त विस्तार एवं सूक्ष्मता से समझा जा सकता है। ‘णाणस्स फलं विरई' ज्ञान के फल से विरति अर्थात् वैराग्य एवं त्याग होता है, परन्तु इस बौद्धिक ज्ञान के साथ अहं का खतरा भी रहता ही है । इस ज्ञान के साथ श्रद्धा एवं त्याग होना आवश्यक नहीं है। इन्द्रियों के ज्ञान के साथ जितनी-जितनी मस्तिष्क एवं बुद्धि जुड़ जाती है उतना उस बुद्धिपरक ज्ञान का विकास होता है। इस ज्ञान के साथ जितना मन एवं हृदय जुड़ जाता है तब इस जाने हुए ज्ञान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है जिसके
रूप आचरण भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिये बच्चा जब अधिक छोटा हाता है तो उसे मल, मूत्र खराब है, अग्नि जलाती है, सांप काटता है, इतना इन्द्रिय या बुद्धि परक ज्ञान भी नहीं होता है । जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उससे ये ज्ञान तो तीनों स्तर तक पांच सात वर्ष की उम्र तक में ही बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ कारण पूर्व के संस्कार एवं कुछ कारण वर्तमान का वातावरण होता है । परन्तु क्रोध, मान, राग, द्वेष, मोह आदि बुरे है यह ज्ञान वर्षों तक पढ़ने, सुनने अथवा थाकड़े, शास्त्र, संस्कृत, प्राकृत-व्याकरण आदि के ज्ञाता या विद्वान् आदि हो जाने पर भी नहीं होता।
अधिकांश तो बुद्धिपरक तक ही अटक जाते हैं। कुछ व्यक्तियों को यह ज्ञान जितना-जितना हृदयपरक होता है उतने-उतने वे त्याग मार्ग में बढ़ते भी हैं, जिसके । फलस्वरूप श्रावक के अणुव्रत, साधु के महाव्रत एवं विविध प्रकार के तप एवं नियम
धारण करते हैं। हालांकि ऐसा एकांत नियम नहीं है कि जितना बुद्धिपरक ज्ञान बढ़ता है, उतना ही त्याग बढ़ता है। कई व्यक्ति बिना बौद्धिक ज्ञान के भी पारिवारिक, आर्थिक, रोगादि कारणों से अथवा परलोक में नरक, तिर्यंच आदि के दुःखों के भय, मान, सम्मान आदि कषाय वश, अथवा किन्हीं सम्बन्धी के साधु-साध्वी बन जाने पर उनके रागवश आदि अनेक कारणों से जिनमें साधु साध्वियों की प्रेरणा सबसे मुख्य है से भी त्याग धारण कर लेते हैं। जिसका नतीजा ठीक नहीं होता। साधु समाज की हालत भी हमारे सामने ही है। विषयों के जोर से उनमें भी विविध प्रकार की शिथिलाचारी प्रवृत्तियां बढ़ती ही जा रही हैं । यहां तक कि बड़े-बड़े काण्ड या पलायनवाद भी बढ़ रहे हैं। फिर जो साधु वर्ग या सम्प्रदाय नाम शेष रह गयी उनमें भी अधिकांश साधु-साध्वियां काषायिक एवं राग-द्वेष की स्थिति से अन्तरंग में तो तनावग्रस्त हैं इस कारण आज का युवक-समाज दिशाविहीन सा बना हुआ है। उसमें अधिकांश को धर्म की सच्चाई क्या है, यह समझ में ही नहीं आ रहा है। सच्चे अध्यात्म के अभाव में संघवाद या सम्प्रदायवाद बढ़ता ही जा रहा है। धर्म के हृदय परक होने पर द्रव्य व व्यवहार शुद्धि
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org