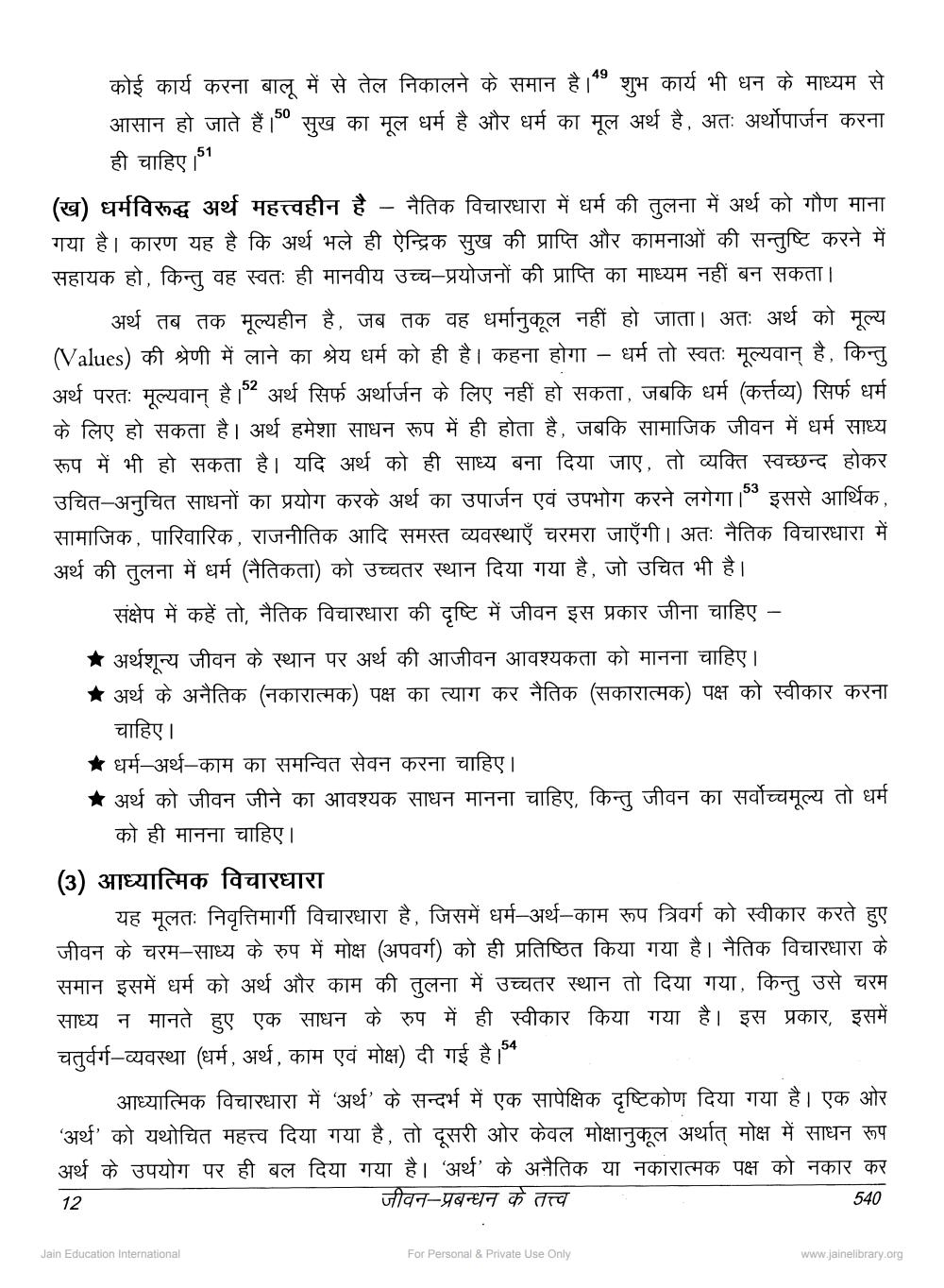________________
कोई कार्य करना बालू में से तेल निकालने के समान है। शुभ कार्य भी धन के माध्यम से आसान हो जाते हैं। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है, अतः अर्थोपार्जन करना
ही चाहिए। (ख) धर्मविरूद्ध अर्थ महत्त्वहीन है – नैतिक विचारधारा में धर्म की तुलना में अर्थ को गौण माना गया है। कारण यह है कि अर्थ भले ही ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति और कामनाओं की सन्तुष्टि करने में सहायक हो, किन्तु वह स्वतः ही मानवीय उच्च-प्रयोजनों की प्राप्ति का माध्यम नहीं बन सकता।
__ अर्थ तब तक मूल्यहीन है, जब तक वह धर्मानुकूल नहीं हो जाता। अतः अर्थ को मूल्य (Values) की श्रेणी में लाने का श्रेय धर्म को ही है। कहना होगा - धर्म तो स्वतः मूल्यवान् है, किन्तु अर्थ परतः मूल्यवान् है। अर्थ सिर्फ अर्थार्जन के लिए नहीं हो सकता, जबकि धर्म (कर्त्तव्य) सिर्फ धर्म के लिए हो सकता है। अर्थ हमेशा साधन रूप में ही होता है, जबकि सामाजिक जीवन में धर्म साध्य रूप में भी हो सकता है। यदि अर्थ को ही साध्य बना दिया जाए, तो व्यक्ति स्वच्छन्द होकर उचित-अनुचित साधनों का प्रयोग करके अर्थ का उपार्जन एवं उपभोग करने लगेगा। इससे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक आदि समस्त व्यवस्थाएँ चरमरा जाएँगी। अतः नैतिक विचारधारा में अर्थ की तुलना में धर्म (नैतिकता) को उच्चतर स्थान दिया गया है, जो उचित भी है।
संक्षेप में कहें तो, नैतिक विचारधारा की दृष्टि में जीवन इस प्रकार जीना चाहिए - ★ अर्थशून्य जीवन के स्थान पर अर्थ की आजीवन आवश्यकता को मानना चाहिए। ★ अर्थ के अनैतिक (नकारात्मक) पक्ष का त्याग कर नैतिक (सकारात्मक) पक्ष को स्वीकार करना
चाहिए। ★ धर्म-अर्थ-काम का समन्वित सेवन करना चाहिए। ★ अर्थ को जीवन जीने का आवश्यक साधन मानना चाहिए, किन्तु जीवन का सर्वोच्चमूल्य तो धर्म
को ही मानना चाहिए। (3) आध्यात्मिक विचारधारा
यह मूलतः निवृत्तिमार्गी विचारधारा है, जिसमें धर्म-अर्थ-काम रूप त्रिवर्ग को स्वीकार करते हुए जीवन के चरम-साध्य के रुप में मोक्ष (अपवर्ग) को ही प्रतिष्ठित किया गया है। नैतिक विचारधारा के समान इसमें धर्म को अर्थ और काम की तुलना में उच्चतर स्थान तो दिया गया, किन्तु उसे चरम साध्य न मानते हुए एक साधन के रुप में ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार, इसमें चतुर्वर्ग-व्यवस्था (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष) दी गई है।
आध्यात्मिक विचारधारा में 'अर्थ' के सन्दर्भ में एक सापेक्षिक दृष्टिकोण दिया गया है। एक ओर 'अर्थ' को यथोचित महत्त्व दिया गया है, तो दूसरी ओर केवल मोक्षानुकूल अर्थात् मोक्ष में साधन रूप अर्थ के उपयोग पर ही बल दिया गया है। 'अर्थ' के अनैतिक या नकारात्मक पक्ष को नकार कर
जीवन-प्रबन्धन के तत्त्व
12
540
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org