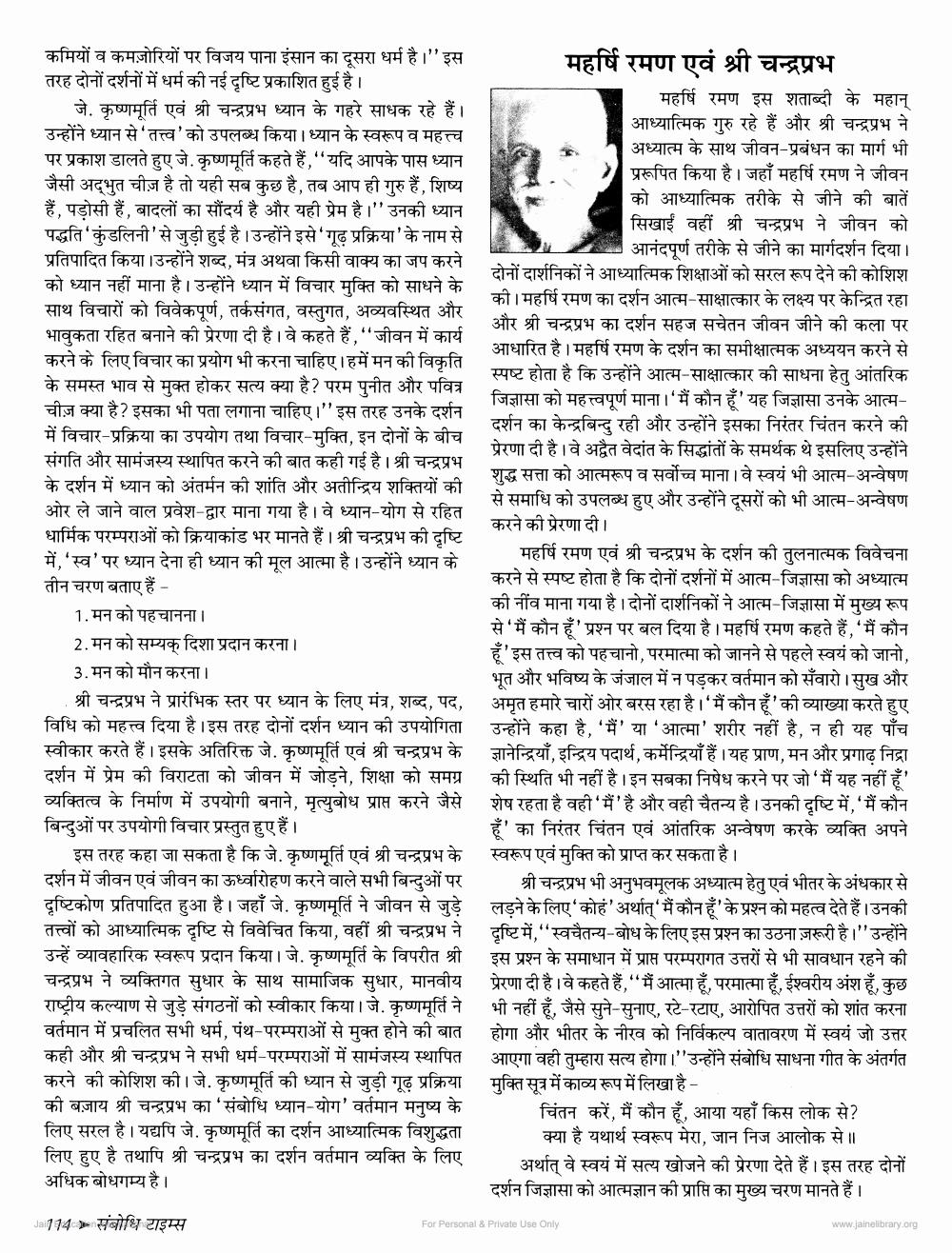________________
कमियों व कमजोरियों पर विजय पाना इंसान का दूसरा धर्म है।" इस
महर्षि रमण एवं श्री चन्द्रप्रभ तरह दोनों दर्शनों में धर्म की नई दृष्टि प्रकाशित हुई है।
महर्षि रमण इस शताब्दी के महान् जे. कृष्णमूर्ति एवं श्री चन्द्रप्रभ ध्यान के गहरे साधक रहे हैं।
आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और श्री चन्द्रप्रभ ने उन्होंने ध्यान से 'तत्त्व' को उपलब्ध किया। ध्यान के स्वरूप व महत्त्व
अध्यात्म के साथ जीवन-प्रबंधन का मार्ग भी पर प्रकाश डालते हुए जे. कृष्णमूर्ति कहते हैं, "यदि आपके पास ध्यान
प्ररूपित किया है। जहाँ महर्षि रमण ने जीवन जैसी अद्भुत चीज़ है तो यही सब कुछ है, तब आप ही गुरु हैं, शिष्य
को आध्यात्मिक तरीके से जीने की बातें हैं, पड़ोसी हैं, बादलों का सौंदर्य है और यही प्रेम है।" उनकी ध्यान
सिखाईं वहीं श्री चन्द्रप्रभ ने जीवन को पद्धति कुंडलिनी' से जुड़ी हुई है। उन्होंने इसे 'गूढ प्रक्रिया के नाम से
| आनंदपूर्ण तरीके से जीने का मार्गदर्शन दिया। प्रतिपादित किया। उन्होंने शब्द, मंत्र अथवा किसी वाक्य का जप करने
दोनों दार्शनिकों ने आध्यात्मिक शिक्षाओं को सरल रूप देने की कोशिश को ध्यान नहीं माना है। उन्होंने ध्यान में विचार मुक्ति को साधने के
की। महर्षि रमण का दर्शन आत्म-साक्षात्कार के लक्ष्य पर केन्द्रित रहा साथ विचारों को विवेकपूर्ण, तर्कसंगत, वस्तुगत, अव्यवस्थित और
और श्री चन्द्रप्रभ का दर्शन सहज सचेतन जीवन जीने की कला पर भावुकता रहित बनाने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं, "जीवन में कार्य
आधारित है। महर्षि रमण के दर्शन का समीक्षात्मक अध्ययन करने से करने के लिए विचार का प्रयोग भी करना चाहिए। हमें मन की विकृति
स्पष्ट होता है कि उन्होंने आत्म-साक्षात्कार की साधना हेतु आंतरिक के समस्त भाव से मुक्त होकर सत्य क्या है? परम पुनीत और पवित्र चीज़ क्या है? इसका भी पता लगाना चाहिए।" इस तरह उनके दर्शन
जिज्ञासा को महत्त्वपूर्ण माना। 'मैं कौन हूँ' यह जिज्ञासा उनके आत्म
दर्शन का केन्द्रबिन्दु रही और उन्होंने इसका निरंतर चिंतन करने की में विचार-प्रक्रिया का उपयोग तथा विचार-मुक्ति, इन दोनों के बीच
प्रेरणा दी है। वे अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के समर्थक थे इसलिए उन्होंने संगति और सामंजस्य स्थापित करने की बात कही गई है। श्री चन्द्रप्रभ
शुद्ध सत्ता को आत्मरूप व सर्वोच्च माना। वे स्वयं भी आत्म-अन्वेषण के दर्शन में ध्यान को अंतर्मन की शांति और अतीन्द्रिय शक्तियों की
से समाधि को उपलब्ध हुए और उन्होंने दूसरों को भी आत्म-अन्वेषण ओर ले जाने वाल प्रवेश-द्वार माना गया है। वे ध्यान-योग से रहित
करने की प्रेरणा दी। धार्मिक परम्पराओं को क्रियाकांड भर मानते हैं। श्री चन्द्रप्रभ की दृष्टि में, 'स्व' पर ध्यान देना ही ध्यान की मूल आत्मा है। उन्होंने ध्यान के
महर्षि रमण एवं श्री चन्द्रप्रभ के दर्शन की तुलनात्मक विवेचना तीन चरण बताए हैं
करने से स्पष्ट होता है कि दोनों दर्शनों में आत्म-जिज्ञासा को अध्यात्म
की नींव माना गया है। दोनों दार्शनिकों ने आत्म-जिज्ञासा में मुख्य रूप 1.मन को पहचानना।
से 'मैं कौन हूँ' प्रश्न पर बल दिया है। महर्षि रमण कहते हैं, 'मैं कौन 2. मन को सम्यक् दिशा प्रदान करना।
हूँ' इस तत्त्व को पहचानो, परमात्मा को जानने से पहले स्वयं को जानो, 3.मन को मौन करना।
भूत और भविष्य के जंजाल में न पड़कर वर्तमान को सँवारो।सुख और श्री चन्द्रप्रभ ने प्रारंभिक स्तर पर ध्यान के लिए मंत्र, शब्द, पद, अमृत हमारे चारों ओर बरस रहा है। मैं कौन हूँ' की व्याख्या करते हुए विधि को महत्त्व दिया है। इस तरह दोनों दर्शन ध्यान की उपयोगिता उन्होंने कहा है, 'मैं' या 'आत्मा' शरीर नहीं है, न ही यह पाँच स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त जे. कृष्णमूर्ति एवं श्री चन्द्रप्रभ के ज्ञानेन्द्रियाँ, इन्द्रिय पदार्थ, कर्मेन्द्रियाँ हैं। यह प्राण, मन और प्रगाढ़ निद्रा दर्शन में प्रेम की विराटता को जीवन में जोड़ने, शिक्षा को समग्र की स्थिति भी नहीं है। इन सबका निषेध करने पर जो 'मैं यह नहीं हूँ' व्यक्तित्व के निर्माण में उपयोगी बनाने, मृत्युबोध प्राप्त करने जैसे शेष रहता है वही 'मैं' है और वही चैतन्य है। उनकी दृष्टि में, 'मैं कौन बिन्दुओं पर उपयोगी विचार प्रस्तुत हुए हैं।
हूँ' का निरंतर चिंतन एवं आंतरिक अन्वेषण करके व्यक्ति अपने इस तरह कहा जा सकता है कि जे. कृष्णमूर्ति एवं श्री चन्द्रप्रभ के स्वरूप एवं मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। दर्शन में जीवन एवं जीवन का ऊर्ध्वारोहण करने वाले सभी बिन्दुओं पर श्री चन्द्रप्रभ भी अनुभवमूलक अध्यात्म हेतु एवं भीतर के अंधकार से दृष्टिकोण प्रतिपादित हुआ है। जहाँ जे. कृष्णमूर्ति ने जीवन से जुड़े लड़ने के लिए कोहं' अर्थात् 'मैं कौन हूँ' के प्रश्न को महत्व देते हैं। उनकी तत्त्वों को आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचित किया, वहीं श्री चन्द्रप्रभ ने दृष्टि में,"स्वचैतन्य-बोध के लिए इस प्रश्न का उठना ज़रूरी है।" उन्होंने उन्हें व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। जे. कृष्णमूर्ति के विपरीत श्री इस प्रश्न के समाधान में प्राप्त परम्परागत उत्तरों से भी सावधान रहने की चन्द्रप्रभ ने व्यक्तिगत सुधार के साथ सामाजिक सुधार, मानवीय प्रेरणा दी है। वे कहते हैं, "मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वरीय अंश हूँ, कुछ राष्ट्रीय कल्याण से जुड़े संगठनों को स्वीकार किया। जे. कृष्णमूर्ति ने भी नहीं हूँ, जैसे सुने-सुनाए, रटे-रटाए, आरोपित उत्तरों को शांत करना वर्तमान में प्रचलित सभी धर्म, पंथ-परम्पराओं से मुक्त होने की बात होगा और भीतर के नीरव को निर्विकल्प वातावरण में स्वयं जो उत्तर कही और श्री चन्द्रप्रभ ने सभी धर्म-परम्पराओं में सामंजस्य स्थापित आएगा वही तुम्हारा सत्य होगा।"उन्होंने संबोधि साधना गीत के अंतर्गत करने की कोशिश की। जे. कृष्णमूर्ति की ध्यान से जुड़ी गूढ़ प्रक्रिया मुक्ति सूत्र में काव्य रूप में लिखा हैकी बजाय श्री चन्द्रप्रभ का 'संबोधि ध्यान-योग' वर्तमान मनुष्य के
चिंतन करें, मैं कौन हूँ, आया यहाँ किस लोक से? लिए सरल है। यद्यपि जे. कृष्णमूर्ति का दर्शन आध्यात्मिक विशुद्धता
क्या है यथार्थ स्वरूप मेरा, जान निज आलोक से॥ लिए हुए है तथापि श्री चन्द्रप्रभ का दर्शन वर्तमान व्यक्ति के लिए
अर्थात् वे स्वयं में सत्य खोजने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह दोनों अधिक बोधगम्य है।
दर्शन जिज्ञासा को आत्मज्ञान की प्राप्ति का मुख्य चरण मानते हैं। Ja114) संबोधि टाइम्स
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org