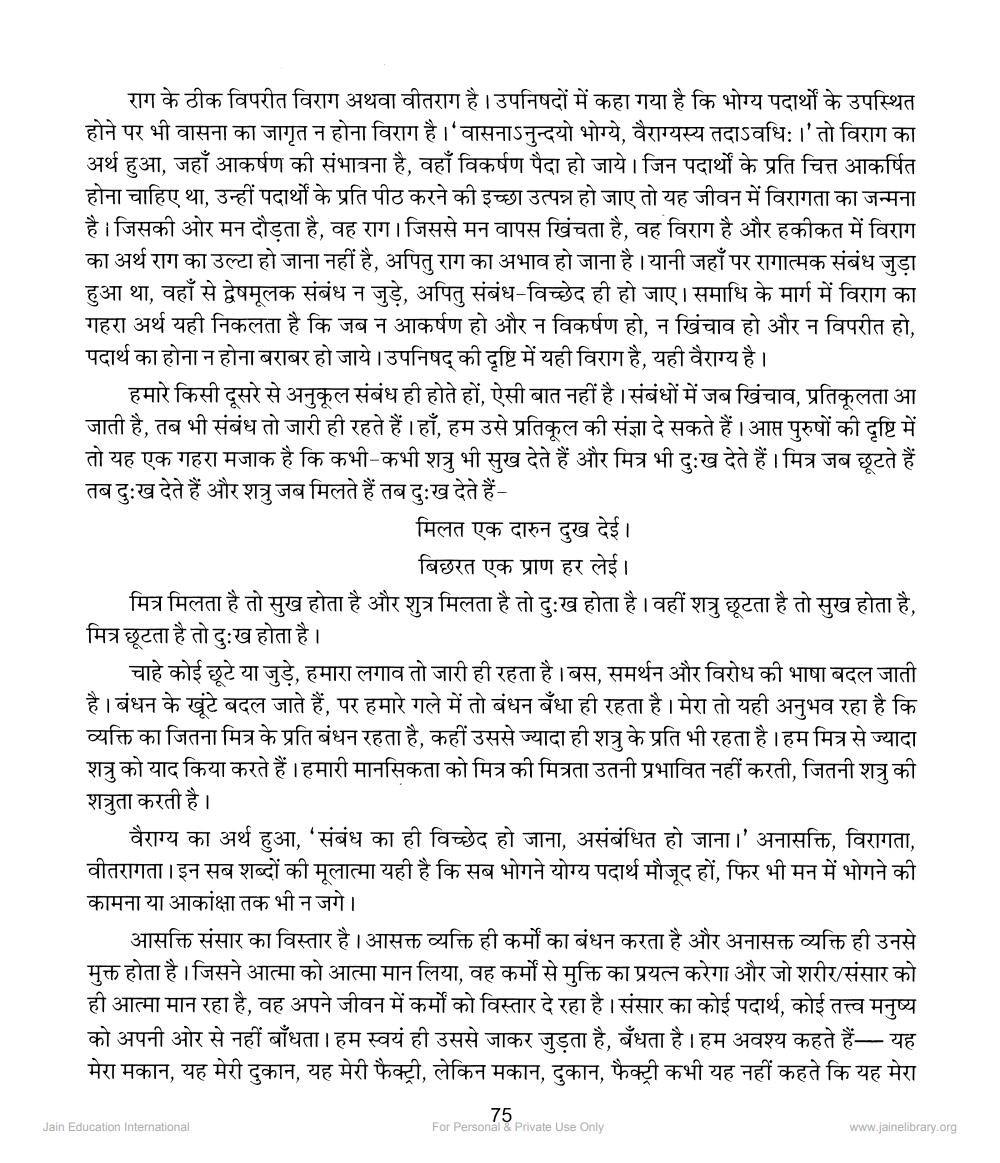________________
राग के ठीक विपरीत विराग अथवा वीतराग है। उपनिषदों में कहा गया है कि भोग्य पदार्थों के उपस्थित होने पर भी वासना का जागृत न होना विराग है । 'वासनाऽनुन्दयो भोग्ये, वैराग्यस्य तदाऽवधिः । ' तो विराग का अर्थ हुआ, जहाँ आकर्षण की संभावना है, वहाँ विकर्षण पैदा हो जाये। जिन पदार्थों के प्रति चित्त आकर्षित होना चाहिए था, उन्हीं पदार्थों के प्रति पीठ करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो यह जीवन में विरागता का जन्मना है। जिसकी ओर मन दौड़ता है, वह राग। जिससे मन वापस खिंचता है, वह विराग है और हकीकत में विराग का अर्थ राग का उल्टा हो जाना नहीं है, अपितु राग का अभाव हो जाना है। यानी जहाँ पर रागात्मक संबंध जुड़ा हुआ था, वहाँ से द्वेषमूलक संबंध न जुड़े, अपितु संबंध-विच्छेद ही हो जाए। समाधि के मार्ग में विराग का गहरा अर्थ यही निकलता है कि जब न आकर्षण हो और न विकर्षण हो, न खिंचाव हो और न विपरीत हो, पदार्थ का होना न होना बराबर हो जाये । उपनिषद् की दृष्टि में यही विराग है, यही वैराग्य है ।
हमारे किसी दूसरे से अनुकूल संबंध ही होते हों, ऐसी बात नहीं है। संबंधों में जब खिंचाव, प्रतिकूलता आ जाती है, तब भी संबंध तो जारी ही रहते हैं। हाँ, हम उसे प्रतिकूल की संज्ञा दे सकते हैं। आप्त पुरुषों की दृष्टि में तो यह एक गहरा मजाक है कि कभी-कभी शत्रु भी सुख देते हैं और मित्र भी दुःख देते हैं। मित्र जब छूटते हैं तब दुःख देते हैं और शत्रु जब मिलते हैं तब दुःख देते हैं
मिलत एक दारुन दुख देई । बिछरत एक प्राण हर लेई ।
मित्र मिलता है तो सुख होता है और शुत्र मिलता है तो दुःख होता है। वहीं शत्रु छूटता है तो सुख होता है, मित्र छूटता है तो दुःख होता है ।
चाहे कोई छूटे या जुड़े, हमारा लगाव तो जारी ही रहता है। बस, समर्थन और विरोध की भाषा बदल जाती है। बंधन के खूंटे बदल जाते हैं, पर हमारे गले में तो बंधन बँधा ही रहता है । मेरा तो यही अनुभव रहा है कि व्यक्ति का जितना मित्र के प्रति बंधन रहता है, कहीं उससे ज्यादा ही शत्रु के प्रति भी रहता है। हम मित्र से ज्यादा `शत्रु को याद किया करते हैं। हमारी मानसिकता को मित्र की मित्रता उतनी प्रभावित नहीं करती, जितनी शत्रु की शत्रुता करती है।
वैराग्य का अर्थ हुआ, ‘संबंध का ही विच्छेद हो जाना, असंबंधित हो जाना।' अनासक्ति, विरागता, वीतरागता । इन सब शब्दों की मूलात्मा यही है कि सब भोगने योग्य पदार्थ मौजूद हों, फिर भी मन में भोगने की कामना या आकांक्षा तक भी न जगे ।
आसक्ति संसार का विस्तार है । आसक्त व्यक्ति ही कर्मों का बंधन करता है और अनासक्त व्यक्ति ही उनसे मुक्त होता है। जिसने आत्मा को आत्मा मान लिया, वह कर्मों से मुक्ति का प्रयत्न करेगा और जो शरीर/संसार को ही आत्मा मान रहा है, वह अपने जीवन में कर्मों को विस्तार दे रहा है। संसार का कोई पदार्थ, कोई तत्त्व मनुष्य को अपनी ओर से नहीं बाँधता । हम स्वयं ही उससे जाकर जुड़ता है, बँधता है। हम अवश्य कहते हैं - यह मेरा मकान, यह मेरी दुकान, यह मेरी फैक्ट्री, लेकिन मकान, दुकान, फैक्ट्री कभी यह नहीं कहते कि यह मेरा
Jain Education International
75
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org