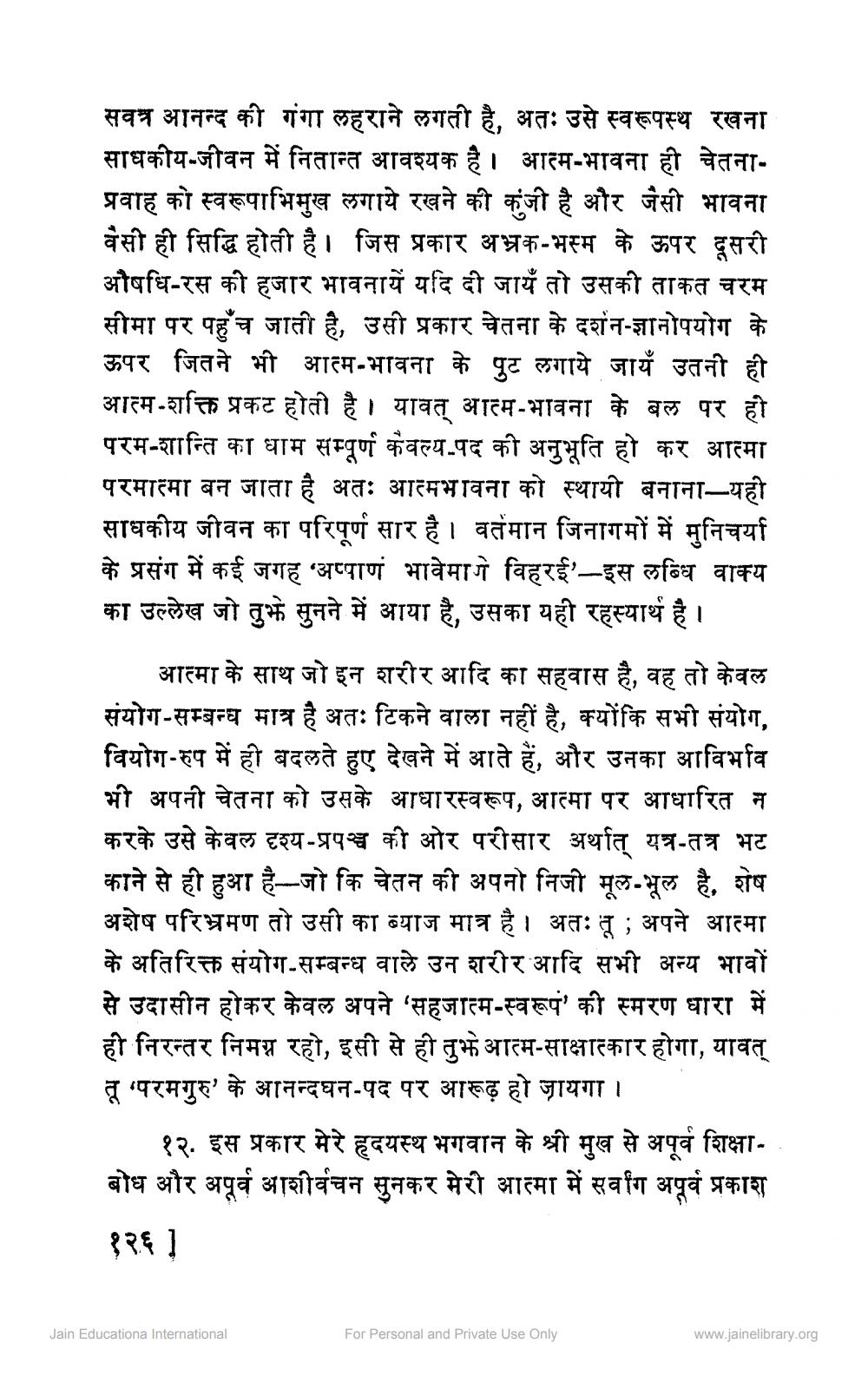________________
सवत्र आनन्द की गंगा लहराने लगती है, अतः उसे स्वरूपस्थ रखना साधकीय-जीवन में नितान्त आवश्यक है। आत्म-भावना ही चेतनाप्रवाह को स्वरूपाभिमुख लगाये रखने की कुंजी है और जैसी भावना वैसी ही सिद्धि होती है। जिस प्रकार अभ्रक भस्म के ऊपर दूसरी
औषधि-रस की हजार भावनायें यदि दी जायँ तो उसकी ताकत चरम सीमा पर पहुँच जाती है, उसी प्रकार चेतना के दर्शन-ज्ञानोपयोग के ऊपर जितने भी आत्म-भावना के पुट लगाये जायँ उतनी ही आत्म-शक्ति प्रकट होती है। यावत् आत्म-भावना के बल पर ही परम-शान्ति का धाम सम्पूर्ण कैवल्य.पद की अनुभूति हो कर आत्मा परमात्मा बन जाता है अतः आत्मभावना को स्थायी बनाना–यही साधकीय जीवन का परिपूर्ण सार है। वर्तमान जिनागमों में मुनिचर्या के प्रसंग में कई जगह 'अप्पाणं भावेमागे विहरई'- इस लब्धि वाक्य का उल्लेख जो तुझे सुनने में आया है, उसका यही रहस्यार्थ है ।
आत्मा के साथ जो इन शरीर आदि का सहवास है, वह तो केवल संयोग-सम्बन्ध मात्र है अतः टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सभी संयोग, वियोग-रुप में ही बदलते हुए देखने में आते हैं, और उनका आविर्भाव भी अपनी चेतना को उसके आधारस्वरूप, आत्मा पर आधारित न करके उसे केवल दृश्य-प्रपञ्च की ओर परीसार अर्थात् यत्र-तत्र भट काने से ही हुआ है जो कि चेतन की अपनो निजी मूल-भूल है, शेष अशेष परिभ्रमण तो उसी का ब्याज मात्र है। अतः तू ; अपने आत्मा के अतिरिक्त संयोग-सम्बन्ध वाले उन शरीर आदि सभी अन्य भावों से उदासीन होकर केवल अपने 'सहजात्म-स्वरूपं' की स्मरण धारा में ही निरन्तर निमग्न रहो, इसी से ही तुझे आत्म-साक्षात्कार होगा, यावत् तू 'परमगुरु' के आनन्दघन-पद पर आरूढ़ हो जायगा।
१२. इस प्रकार मेरे हृदयस्थ भगवान के श्री मुख से अपूर्व शिक्षाबोध और अपूर्व आशीर्वचन सुनकर मेरी आत्मा में सर्वांग अपूर्व प्रकाश १२६ ]
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org