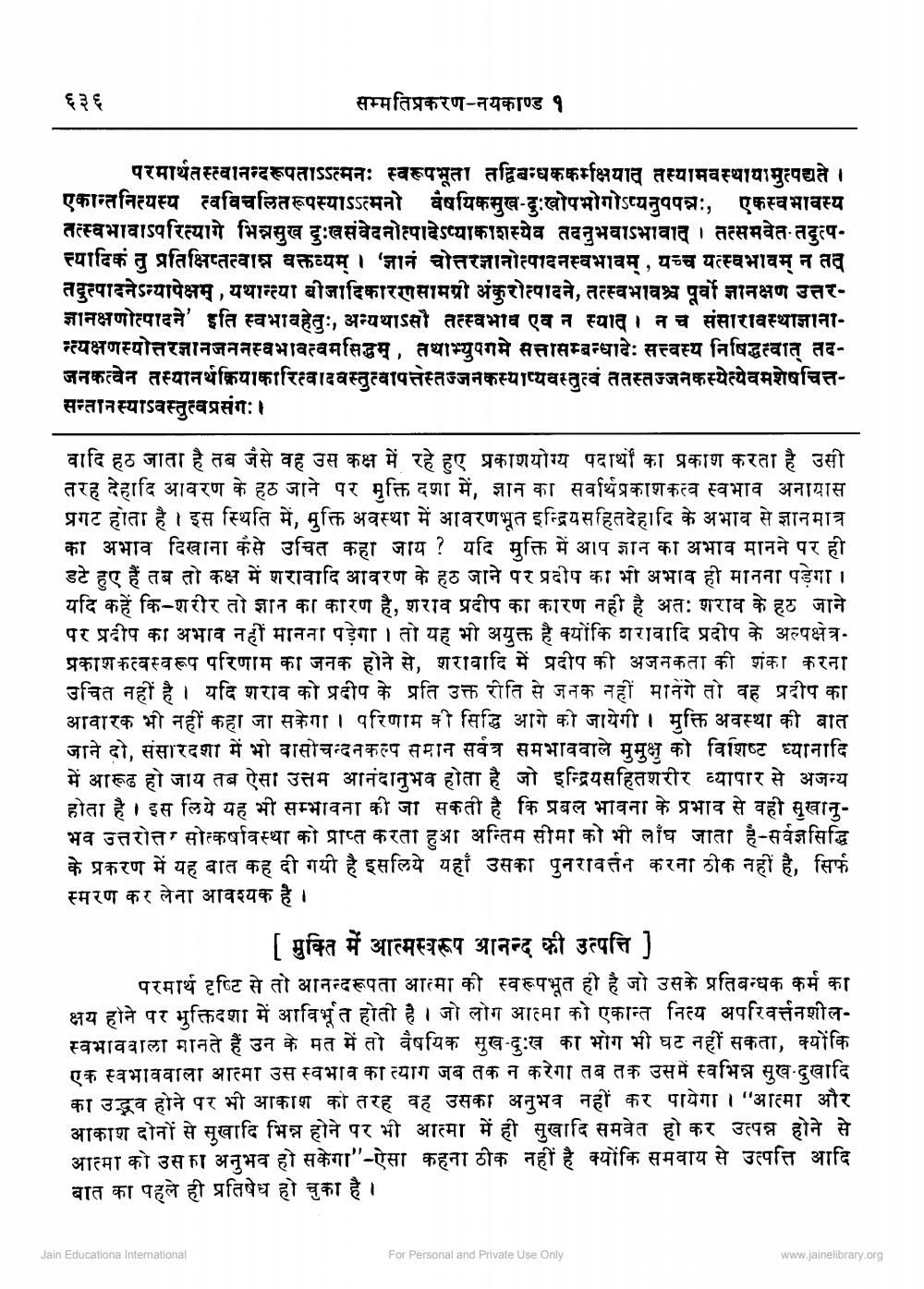________________
सम्मतिप्रकरण-नयकाण्ड १
परमार्थतस्त्वानन्दरूपताऽऽत्मनः स्वरूपभूता तद्विबन्धककर्मक्षयाव तस्यामवस्थायामुत्पद्यते । एकान्त नित्यस्य त्वविचलितरूपस्याऽऽत्मनो वैषयिकसुख-दुःखोपभोगोऽप्यनुपपन्नः, एफस्वभावस्य तत्स्वभावाऽपरित्यागे भिन्नसुख दुःखसंवेदनोत्पादेऽप्याकाशस्येव तदनुभवाऽभावात् । तत्समवेत तदुत्प. त्यादिकं तु प्रतिक्षिप्तत्वान्न वक्तव्यम् । 'ज्ञानं चोत्तरज्ञानोत्पादनस्वभावम् , यच्च यत्स्वभावम् न तव तदुत्पादनेऽन्यापेक्षम् , यथान्त्या बीजादिकारणसामग्री अंकुरोत्पादने, तत्स्वभावश्च पूर्वो ज्ञानक्षण उत्तरज्ञानक्षणोत्पादने' इति स्वभावहेतुः, अन्यथाऽसौ तत्स्वभाव एव न स्यात्। न च संसारावस्थाज्ञाना. न्यक्षणस्योत्तरज्ञानजननस्वभावत्वमसिद्धम् , तथाभ्युपगमे सत्तासम्बन्धादेः सत्त्वस्य निषिद्धत्वात् तदजनकत्वेन तस्यानर्थक्रियाकारित्वादवस्तुत्वापत्तेस्तज्जनकस्याप्यवस्तुत्वं ततस्तज्जनकस्येत्येवमशेषचित्तसन्तानस्याऽवस्तुत्वप्रसंगः।
वादि हठ जाता है तब जैसे वह उस कक्ष में रहे हुए प्रकाशयोग्य पदार्थों का प्रकाश करता है उसी तरह देहादि आवरण के हठ जाने पर मुक्ति दशा में, ज्ञान का सर्वार्थप्रकाशकत्व स्वभाव अनायास प्रगट होता है। इस स्थिति में, मुक्ति अवस्था में आवरणभूत इन्द्रिय सहितदेहादि के अभाव से ज्ञानमात्र का अभाव दिखाना कैसे उचित कहा जाय ? यदि मुक्ति में आप ज्ञान का अभाव मानने पर ही डटे हुए हैं तब तो कक्ष में शरावादि आवरण के हठ जाने पर प्रदीप का भी अभाव ही मानना पड़ेगा। यदि कहें कि-शरीर तो ज्ञान का कारण है, शराव प्रदीप का कारण नही है अत: शराव के हठ जाने पर प्रदीप का अभाव नहीं मानना पड़ेगा। तो यह भी अयुक्त है क्योंकि गरावादि प्रदीप के अल्पक्षेत्र. प्रकाशकत्वस्वरूप परिणाम का जनक होने से, शरावादि में प्रदीप की अजनकता की शंका करना उचित नहीं है। यदि शराव को प्रदीप के प्रति उक्त रीति से जनक नहीं मानेंगे तो वह प्रदीप का आवारक भी नहीं कहा जा सकेगा। परिणाम की सिद्धि आगे को जायेगी। मुक्ति अवस्था की बात जाने दो, संसारदशा में भी वासोचन्दनकल्प समान सर्वत्र समभाववाले मुमुक्षु को विशिष्ट ध्यानादि में आरूढ हो जाय तब ऐसा उत्तम आनंदानुभव होता है जो इन्द्रियसहितशरीर व्यापार से अजन्य होता है । इस लिये यह भी सम्भावना की जा सकती है कि प्रबल भावना के प्रभाव से वही सुखानुभव उत्तरोत्तर सोत्कर्षावस्था को प्राप्त करता हआ अन्तिम सीमा को भी लाँघ जाता है-सर्वज्ञसिद्धि के प्रकरण में यह बात कह दी गयी है इसलिये यहाँ उसका पुनरावर्तन करना ठीक नहीं है, सिर्फ स्मरण कर लेना आवश्यक है।
[ मुक्ति में आत्मस्वरूप आनन्द की उत्पत्ति ] परमार्थ दृष्टि से तो आनन्दरूपता आत्मा की स्वरूपभूत ही है जो उसके प्रतिबन्धक कर्म का क्षय होने पर मुक्तिदशा में आविर्भूत होती है । जो लोग आत्मा को एकान्त नित्य अपरिवर्तनशीलस्वभाववाला मानते हैं उन के मत में तो वैषयिक सुख-दुःख का भोग भी घट नहीं सकता, क्योंकि एक स्वभाववाला आत्मा उस स्वभाव का त्याग जब तक न करेगा तब तक उस में स्वभिन्न सुख-दुखादि का उद्भव होने पर भी आकाश को तरह वह उसका अनुभव नहीं कर पायेगा। "आत्म आकाश दोनों से सुखादि भिन्न होने पर भी आत्मा में ही सुखादि समवेत हो कर उत्पन्न होने से आत्मा को उसका अनुभव हो सकेगा"-ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि समवाय से उत्पत्ति आदि बात का पहले ही प्रतिषेध हो चुका है।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org