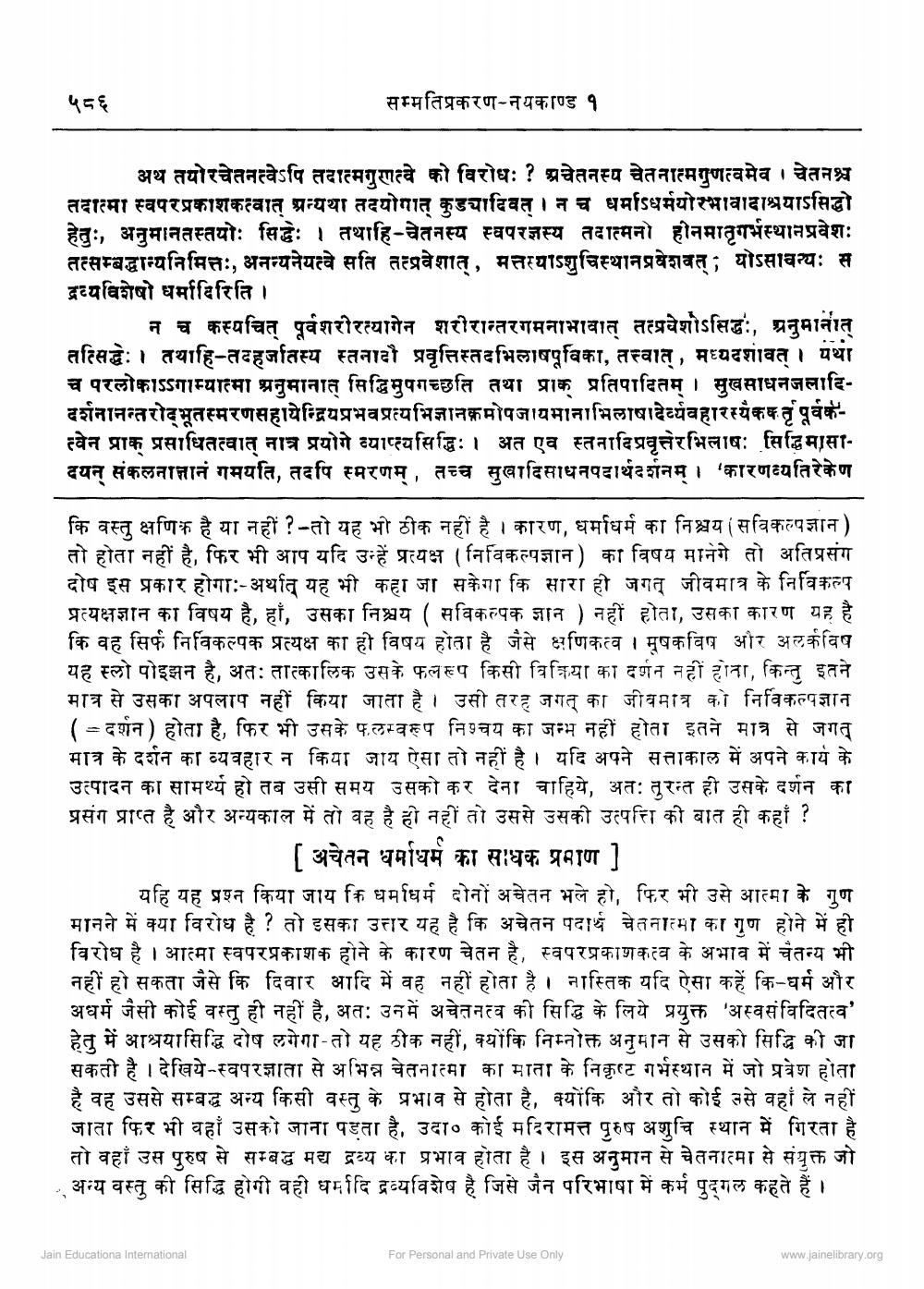________________
५८६
सम्मतिप्रकरण - नयकाण्ड १
अथ तयोरचेतनत्वेऽपि तदात्मगुणत्वे को विरोध: ? प्रचेतनस्य चेतनात्मगुणत्वमेव । चेतनश्च तदात्मा स्वपर प्रकाशकत्वात् अन्यथा तदयोगात् कुडचादिवत् । न च धर्माधर्मयोरभावादाश्रयाऽसिद्धो हेतु:, अनुमानतस्तयोः सिद्धेः । तथाहि चेतनस्य स्वपरज्ञस्य तदात्मनो होनमातृगर्भस्थानप्रवेशः तत्सम्बद्धान्यनिमित्तः, अनन्यनेयत्वे सति तत्प्रवेशात् मत्तस्याऽशुचिस्थानप्रवेशवत् ; योऽसावन्यः स द्रव्यविशेषो धर्मादिरिति ।
,
न च कस्यचित् पूर्वशरीरत्यागेन शरीरान्तरगमनाभावात् तत्प्रवेशोऽसिद्ध:, श्रनुमानात् तत्सिद्धेः । तथाहि तदहर्जातस्य स्तनादौ प्रवृत्तिस्तदभिलाषपूविका, तस्वात्, मध्यदशावत् । यथा च परलोकाऽऽगाम्यात्मा श्रनुमानात् सिद्धिमुपगच्छति तथा प्राक् प्रतिपादितम् । सुखसाधनजलादिदर्शनानन्तरोद्भूतस्मरणसहायेन्द्रियप्रभव प्रत्यभिज्ञानक्रमोपजायमानाभिलाषादेर्व्यवहारस्यैककर्तृ पूर्वकेत्वेन प्राक् प्रसाधितत्वात् नात्र प्रयोगे व्याप्त्यसिद्धिः । अत एव स्तनादिप्रवृत्तेरभिलाषः सिद्धिमासादयन् संकलनातानं गमयति, तदपि स्मरणम्, तच्च सुखादिसाधनपदार्थदर्शनम् । 'कारणव्यतिरेकेण
कि वस्तु क्षणिक है या नहीं ? - तो यह भी ठीक नहीं है । कारण, धर्माधर्म का निश्चय ( सविकल्पज्ञान ) तो होता नहीं है, फिर भी आप यदि उन्हें प्रत्यक्ष ( निविकल्पज्ञान ) का विषय मानेगे तो अतिप्रसंग दोष इस प्रकार होगा :- अर्थात् यह भी कहा जा सकेगा कि सारा ही जगत् जीवमात्र के निर्विकल्प प्रत्यक्षज्ञान का विषय है, हाँ, उसका निश्चय ( सविकल्पक ज्ञान ) नहीं होता, उसका कारण यह है कि वह सिर्फ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का ही विषय होता है जैसे क्षणिकत्व । मुषकविष और अलर्कविष यह स्लो पोइझन है, अतः तात्कालिक उसके फलरूप किसी विक्रिया का दर्शन नहीं होता, किन्तु इतने मात्र से उसका अपलाप नहीं किया जाता है । उसी तरह जगत् का जीवमात्र को निर्विकल्पज्ञान ( = दर्शन ) होता है, फिर भी उसके फलस्वरूप निश्चय का जन्म नहीं होता इतने मात्र से जगत् मात्र के दर्शन का व्यवहार न किया जाय ऐसा तो नहीं है । यदि अपने सत्ताकाल में अपने कार्य के उत्पादन का सामर्थ्य हो तब उसी समय उसको कर देना चाहिये, अत: तुरन्त ही उसके दर्शन का प्रसंग प्राप्त है और अन्यकाल में तो वह है ही नहीं तो उससे उसकी उत्पत्ति की बात ही कहाँ ?
Jain Educationa International
[ अचेतन धर्माधर्म का साधक प्रमाण ]
यहि यह प्रश्न किया जाय कि धर्माधर्म दोनों अचेतन भले हो, फिर भी उसे आत्मा के गुण मानने में क्या विरोध है ? तो इसका उत्तर यह है कि अचेतन पदार्थ चेतनात्मा का गुण होने में ही विरोध है । आत्मा स्वपरप्रकाशक होने के कारण चेतन है, स्वपरप्रकाशकत्व के अभाव में चैतन्य भी नहीं हो सकता जैसे कि दिवार आदि में वह नहीं होता है । नास्तिक यदि ऐसा कहें कि धर्म और अधर्म जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, अत: उनमें अचेतनत्व की सिद्धि के लिये प्रयुक्त 'अस्वसंविदितत्व' हेतु में आश्रयासिद्धि दोष लगेगा तो यह ठीक नहीं, क्योंकि निम्नोक्त अनुमान से उसको सिद्धि की जा सकती है | देखिये - स्वपरज्ञाता से अभिन्न चेतनात्मा का माता के निकृष्ट गर्भस्थान में जो प्रवेश होता है वह उससे सम्बद्ध अन्य किसी वस्तु के प्रभाव से होता है, क्योंकि और तो कोई उसे वहाँ ले नहीं जाता फिर भी वहाँ उसको जाना पड़ता है, उदा० कोई मदिरामत्त पुरुष अशुचि स्थान में गिरता है तो वहाँ उस पुरुष से सम्बद्ध मद्य द्रव्य का प्रभाव होता है । इस अनुमान से चेतनात्मा से संयुक्त जो अन्य वस्तु की सिद्धि होगी वही धर्मादि द्रव्यविशेष है जिसे जैन परिभाषा में कर्म पुद्गल कहते हैं ।
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org