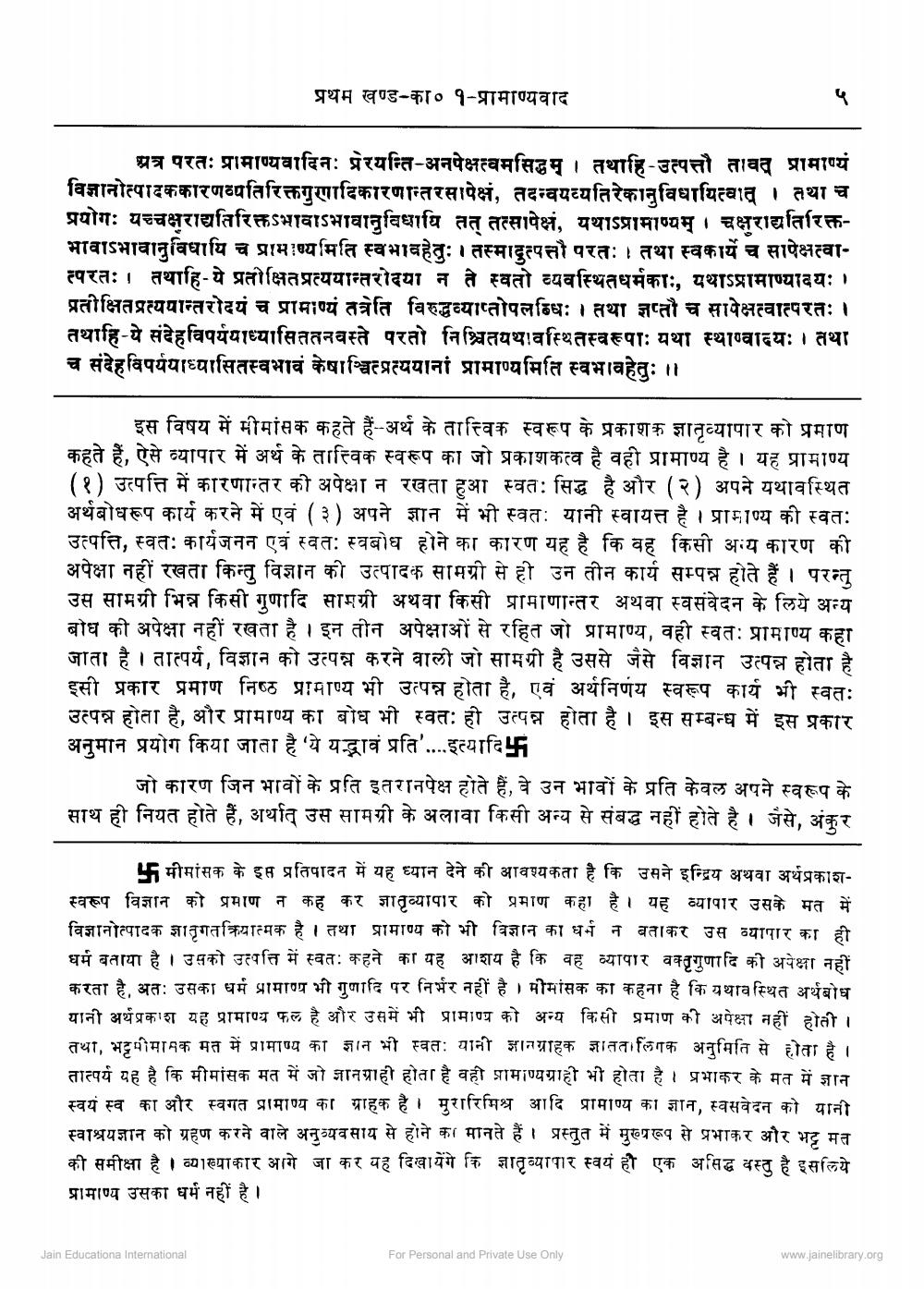________________
प्रथम खण्ड-का० १- प्रामाण्यवाद
अत्र परतः प्रामाण्यवादिनः प्रेरयन्ति - अनपेक्षत्वमसिद्धम् । तथाहि उत्पत्तौ तावत् प्रामाण्यं विज्ञानोत्पादक कारणव्यतिरिक्तगुणादिकारणान्तरसापेक्षं, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् । तथा च प्रयोग: यच्चक्षुराद्यतिरिक्तभावाऽभावानुविधायि तत् तत्सापेक्षं यथाप्रामाण्यम् । चक्षुराद्यतिरिक्तभावाभावानुविधायि च प्रामाण्यमिति स्वभावहेतुः । तस्मादुत्पत्तौ परतः । तथा स्वकार्ये च सापेक्षत्वात्परतः । तथाहि - ये प्रतीक्षित प्रत्ययान्तरोदया न ते स्वतो व्यवस्थितधर्मकाः यथाऽप्रामाण्यावयः । प्रतीक्षित प्रत्ययान्तरोदयं च प्रामाण्यं तत्रेति विरुद्धव्याप्तोपलब्धिः । तथा ज्ञप्तौ च सापेक्षत्वात्परतः । तथाहि ये संदेह विपर्ययाध्यासिततनवस्ते परतो निश्चितयथावस्थितस्वरूपाः यथा स्थाण्वादयः । तथा च संदेह विपर्ययाध्यासितस्वभावं केषाञ्चित्प्रत्ययानां प्रामाण्यमिति स्वभावहेतुः ॥
इस विषय में मीमांसक कहते हैं - अर्थ के तात्त्विक स्वरूप के प्रकाशक ज्ञातृव्यापार को प्रमाण कहते हैं, ऐसे व्यापार में अर्थ के तात्त्विक स्वरूप का जो प्रकाशकत्व है वही प्रामाण्य है । यह प्रामाण्य ( १ ) उत्पत्ति में कारणान्तर की अपेक्षा न रखता हुआ स्वत: सिद्ध है और ( २ ) अपने यथावस्थित अर्थबोधरूप कार्य करने में एवं (३) अपने ज्ञान में भी स्वतः यानी स्वायत्त है । प्रामाण्य की स्वतः उत्पत्ति, स्वतः कार्यजनन एवं स्वत: स्वबोध होने का कारण यह है कि वह किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता किन्तु विज्ञान की उत्पादक सामग्री से ही उन तीन कार्य सम्पन्न होते हैं । परन्तु अथवा किसी प्रामाणान्तर अथवा स्वसंवेदन के लिये अन्य अपेक्षाओं से रहित जो प्रामाण्य, वही स्वतः प्रामाण्य कहा वाली जो सामग्री है उससे जैसे विज्ञान उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है, एवं अर्थनिर्णय स्वरूप कार्य भी स्वतः स्वत: ही उत्पन्न होता है । इस सम्बन्ध में इस प्रकार इत्यादि
उस सामग्री भिन्न किसी गुणादि सामग्री बोध की अपेक्षा नहीं रखता है । इन तीन जाता है । तात्पर्य, विज्ञान को उत्पन्न करने इसी प्रकार प्रमाण निष्ठ प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है, और प्रामाण्य का बोध भी अनुमान प्रयोग किया जाता है 'ये यद्भावं प्रति'
५
....
Jain Educationa International
जो कारण जिन भावों के प्रति इतरानपेक्ष होते हैं, वे उन भावों के प्रति केवल अपने स्वरूप के साथ ही नियत होते हैं, अर्थात् उस सामग्री के अलावा किसी अन्य से संबद्ध नहीं होते है । जैसे, अंकुर
5 मीमांसक के इस प्रतिपादन में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसने इन्द्रिय अथवा अर्थप्रकाशस्वरूप विज्ञान को प्रमाण न कह कर ज्ञातृव्यापार को प्रमाण कहा है। यह व्यापार उसके मत में विज्ञानोत्पादक ज्ञातृगतक्रियात्मक है । तथा प्रामाण्य को भी विज्ञान का धर्म न बताकर उस व्यापार का ही धर्म बताया है । उसको उत्पत्ति में स्वतः कहने का यह आशय है कि वह व्यापार वक्तृगुणादि की अपेक्षा नहीं करता है, अतः उसका धर्म प्रामाण्य भी गुणादि पर निर्भर नहीं है। मीमांसक का कहना है कि यथावस्थित अर्थ यानी अर्थप्रकाश यह प्रामाण्य फल है और उसमें भी प्रामाण्य को अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती । तथा, भट्टमीमामक मत में प्रामाण्य का ज्ञान भी स्वतः यानी ज्ञानग्राहक ज्ञातता लिगक अनुमिति से होता 1 तात्पर्य यह है कि मीमांसक मत में जो ज्ञानग्राही होता है वही प्रामाण्यग्राही भी होता है । प्रभाकर के मत में ज्ञान स्वयं स्व का और स्वगत प्रामाण्य का ग्राहक है । मुरारिमिश्र आदि प्रामाण्य का ज्ञान, स्वसवेदन को यानी स्वाश्रयज्ञान को ग्रहण करने वाले अनुव्यवसाय से होने का मानते हैं । प्रस्तुत में मुख्यरूप से प्रभाकर और भट्ट मत की समीक्षा है | व्याख्याकार आगे जा कर यह दिखायेंगे कि ज्ञातृव्यापार स्वयं ही एक असिद्ध वस्तु है इसलिये प्रामाण्य उसका धर्म नहीं है ।
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org