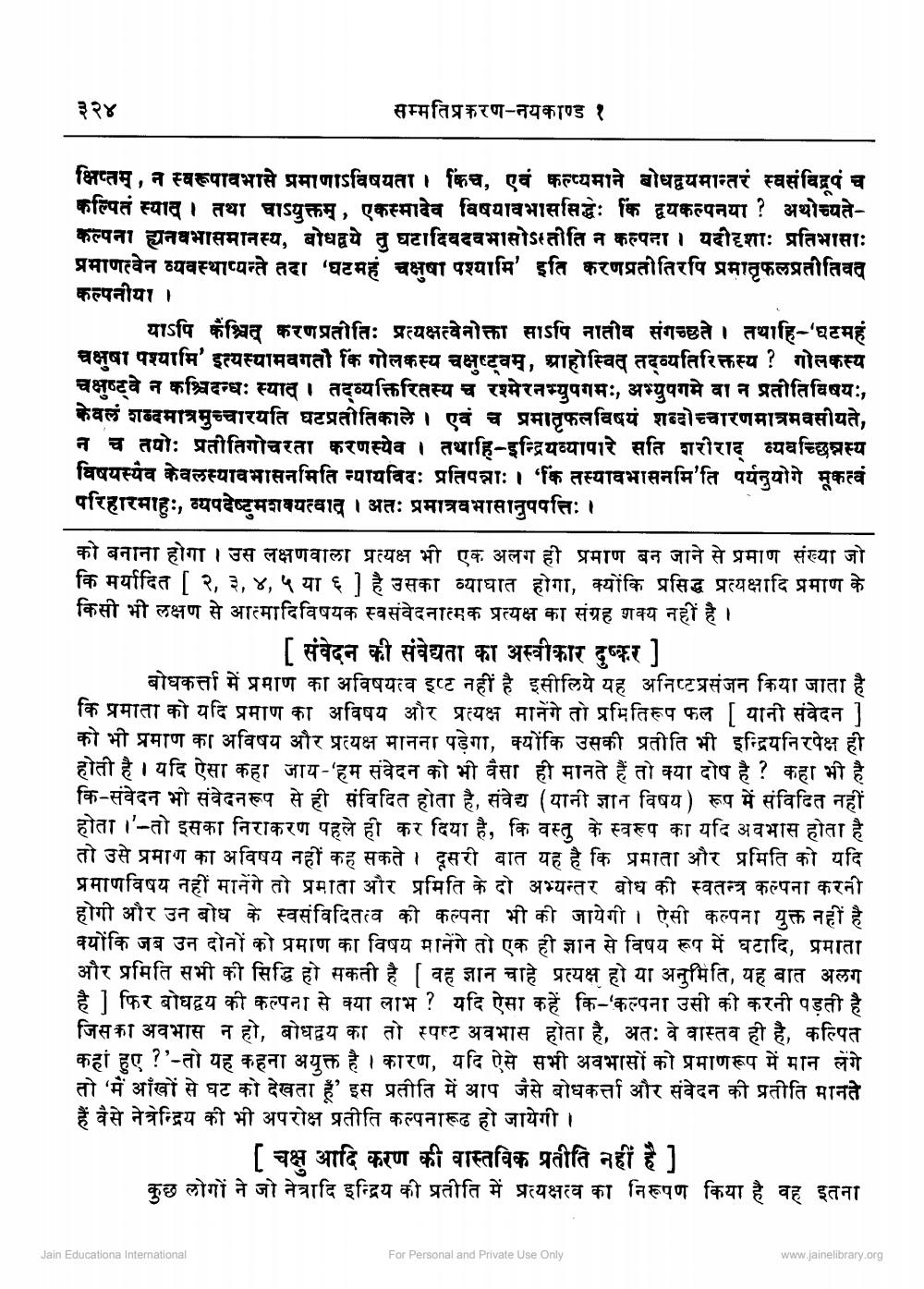________________
३२४
सम्मतिप्रकरण - नयकाण्ड १
क्षिप्तम्, न स्वरूपावभासे प्रमाणाऽविषयता । किंच, एवं कल्प्यमाने बोधद्वयमान्तरं स्वसंविद्रूपं च कल्पितं स्यात् । तथा चाऽयुक्तम्, एकस्मादेव विषयावभाससिद्धेः किं द्वयकल्पनया ? अथोच्यतेकल्पना ह्यनवभासमानस्य, बोधद्वये तु घटादिवदवभासोऽस्तीति न कल्पना । यदीदृशाः प्रतिभासाः प्रमाणत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते तदा 'घटमहं चक्षुषा पश्यामि' इति करणप्रतीतिरपि प्रमातृफलप्रतीतिवत् कल्पनीया ।
याsपि कैश्चित् करण प्रतीतिः प्रत्यक्षत्वेनोक्ता साऽपि नातीव संगच्छते । तथाहि - 'घटमहं चक्षुषा पश्यामि' इत्यस्यामवगतौ कि गोलकस्य चक्षुष्ट्वम्, श्राहोस्वित् तद्व्यतिरिक्तस्य ? गोलकस्य चक्षुष्ट्वे न कश्चिदन्धः स्यात् । तद्व्यक्तिरितस्य च रश्मेरनभ्युपगमः, अभ्युपगमे वा न प्रतीतिविषयः, केवलं शब्दमात्रमुच्चारयति घटप्रतीतिकाले । एवं च प्रमातृफलविषयं शब्दोच्चारणमात्रमवसीयते, न च तयोः प्रतीतिगोचरता करणस्येव । तथाहि इन्द्रियव्यापारे सति शरीराद् व्यवच्छिन्नस्य विषयस्यैव केवलस्यावभासनमिति न्यायविदः प्रतिपन्नाः । किं तस्यावभासनमिति पर्यनुयोगे मूकत्वं परिहारमाहुः, व्यपदेष्टुमशक्यत्वात् । अतः प्रमात्रवभासानुपपत्तिः ।
को बनाना होगा । उस लक्षणवाला प्रत्यक्ष भी एक अलग ही प्रमाण बन जाने से प्रमाण संख्या जो कि मर्यादित २, ३, ४, ५ या ६ ] है उसका व्याघात होगा, क्योंकि प्रसिद्ध प्रत्यक्षादि प्रमाण के किसी भी लक्षण से आत्मादिविषयक स्वसंवेदनात्मक प्रत्यक्ष का संग्रह शक्य नहीं है ।
[ संवेदन की संवेद्यता का अस्वीकार दुष्कर ]
बोधकर्त्ता में प्रमाण का अविषयत्व इष्ट नहीं है इसीलिये यह अनिष्टसंजन किया जाता है कि प्रमाता को यदि प्रमाण का अविषय और प्रत्यक्ष मानेंगे तो प्रमितिरूप फल [ यानी संवेदन ] को भी प्रमाण का अविषय और प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रतीति भी इन्द्रियनिरपेक्ष ही होती है । यदि ऐसा कहा जाय - 'हम संवेदन को भी वैसा ही मानते हैं तो क्या दोष है ? कहा भी है कि- संवेदन भी संवेदन रूप से ही संविदित होता है, संवेद्य (यानी ज्ञान विषय) रूप में संविदित नहीं होता ।' - तो इसका निराकरण पहले ही कर दिया है, कि वस्तु के स्वरूप का यदि अवभास होता है तो उसे प्रमाण का अविषय नहीं कह सकते । दूसरी बात यह है कि प्रमाता और प्रमिति को यदि प्रमाणविषय नहीं मानेंगे तो प्रमाता और प्रमिति के दो अभ्यन्तर बोध की स्वतन्त्र कल्पना करनी होगी और उन बोध के स्वसंविदितत्व की कल्पना भी की जायेगी । ऐसी कल्पना युक्त नहीं है। क्योंकि जब उन दोनों को प्रमाण का विषय मानेंगे तो एक ही ज्ञान से विषय रूप में घटादि, प्रमाता और प्रमिति सभी की सिद्धि हो सकती है [ वह ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष हो या अनुमिति, यह बात अलग है ] फिर बोधय की कल्पना से क्या लाभ ? यदि ऐसा कहें कि ' कल्पना उसी की करनी पड़ती है जिसका अवभास न हो, बोधद्वय का तो स्पष्ट अवभास होता है, अतः वे वास्तव ही है, कल्पित कहां हुए ?'- तो यह कहना अयुक्त है । कारण, यदि ऐसे सभी अवभासों को प्रमाणरूप में मान लेंगे तो 'मैं' आँखों से घट को देखता हूँ' इस प्रतीति में आप जैसे बोधकर्ता और संवेदन की प्रतीति मानते हैं वैसे नेत्रेन्द्रिय की भी अपरोक्ष प्रतीति कल्पनारूढ हो जायेगी ।
[ चक्षु आदि करण की वास्तविक प्रतीति नहीं है ]
कुछ लोगों ने जो नेत्रादि इन्द्रिय की प्रतीति में प्रत्यक्षत्व का निरूपण किया है वह इतना
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org