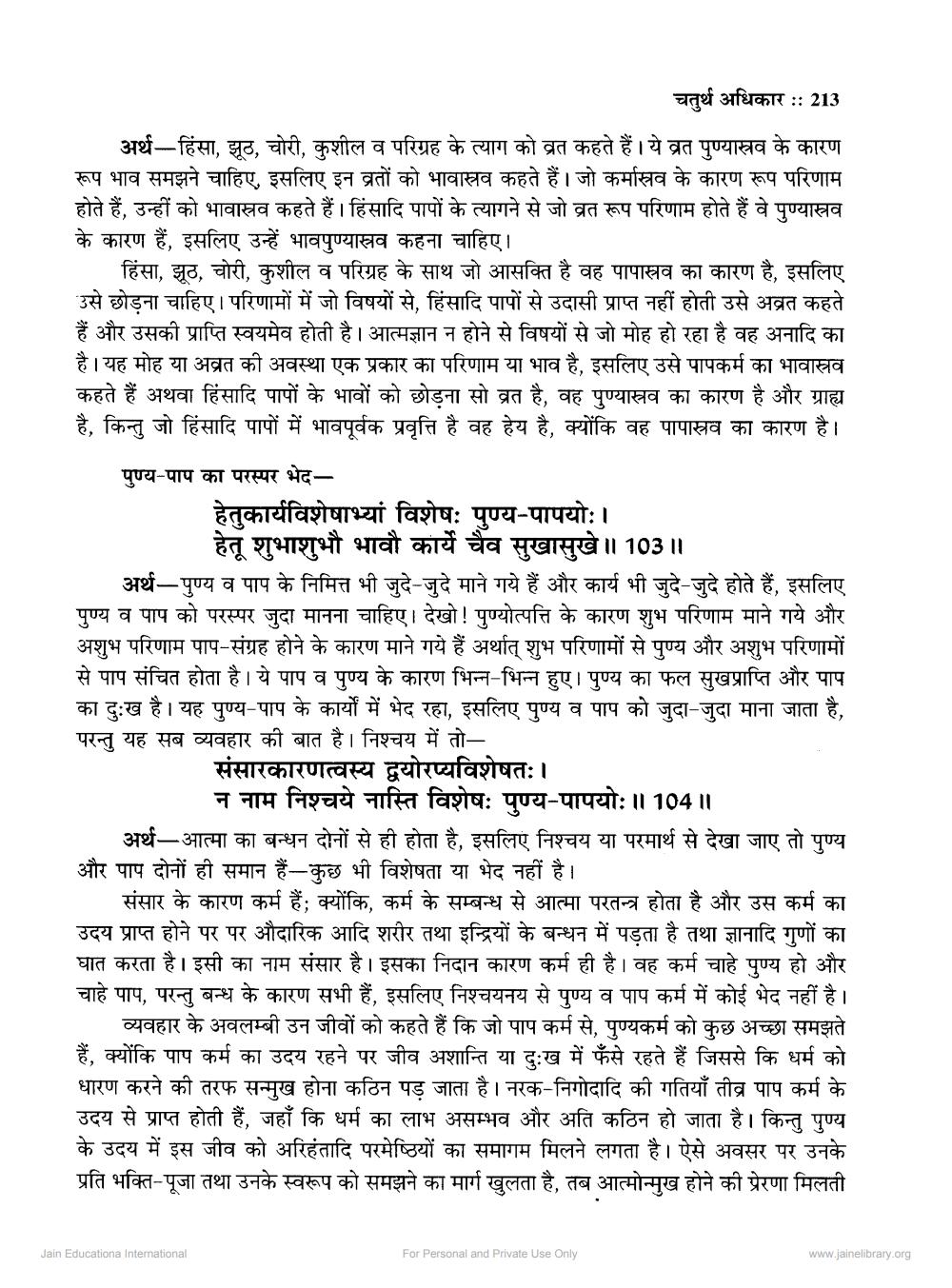________________
चतुर्थ अधिकार :: 213
अर्थ – हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह के त्याग को व्रत कहते हैं । ये व्रत पुण्यास्रव के कारण रूप भाव समझने चाहिए, इसलिए इन व्रतों को भावास्रव कहते हैं । जो कर्मास्रव के कारण रूप परिणाम होते हैं, उन्हीं को भावास्रव कहते हैं। हिंसादि पापों के त्यागने से जो व्रत रूप परिणाम होते हैं वे पुण्यास्रव
कारण हैं, इसलिए उन्हें भावपुण्यास्रव कहना चाहिए ।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह के साथ जो आसक्ति है वह पापास्रव का कारण है, इसलिए उसे छोड़ना चाहिए। परिणामों में जो विषयों से, हिंसादि पापों से उदासी प्राप्त नहीं होती उसे अव्रत कहते हैं और उसकी प्राप्ति स्वयमेव होती है। आत्मज्ञान न होने से विषयों से जो मोह हो रहा है वह अनादि का है । यह मोह या अव्रत की अवस्था एक प्रकार का परिणाम या भाव है, इसलिए उसे पापकर्म का भावास्रव कहते हैं अथवा हिंसादि पापों के भावों को छोड़ना सो व्रत है, वह पुण्यास्रव का कारण है और ग्राह्य है, किन्तु जो हिंसादि पापों में भावपूर्वक प्रवृत्ति है वह हेय है, क्योंकि वह पापास्रव का कारण है।
पुण्य-पाप का परस्पर भेद
हेतुकार्यविशेषाभ्यां विशेषः पुण्य-पापयोः ।
तू शुभाशुभ भावी कार्ये चैव सुखासुखे ॥ 103 ॥
अर्थ – पुण्य व पाप के निमित्त भी जुदे - जुदे माने गये हैं और कार्य भी जुदे - जुदे होते हैं, इसलिए पुण्य व पाप को परस्पर जुदा मानना चाहिए। देखो ! पुण्योत्पत्ति के कारण शुभ परिणाम माने गये और अशुभ परिणाम पाप-संग्रह होने के कारण माने गये हैं अर्थात् शुभ परिणामों से पुण्य और अशुभ परिणामों से पाप संचित होता है। ये पाप व पुण्य के कारण भिन्न-भिन्न हुए । पुण्य का फल सुखप्राप्ति और पाप का दुःख है । यह पुण्य - पाप के कार्यों में भेद रहा, इसलिए पुण्य व पाप को जुदा-जुदा माना जाता है, परन्तु यह सब व्यवहार की बात है । निश्चय में तो
Jain Educationa International
संसारकारणत्वस्य द्वयोरप्यविशेषतः ।
न नाम निश्चये नास्ति विशेषः पुण्य-पापयोः ॥ 104 ॥
अर्थ- आत्मा का बन्धन दोनों से ही होता है, इसलिए निश्चय या परमार्थ से देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों ही समान हैं - कुछ भी विशेषता या भेद नहीं है ।
संसार के कारण कर्म हैं; क्योंकि, कर्म के सम्बन्ध से आत्मा परतन्त्र होता है और उस कर्म का उदय प्राप्त होने पर पर औदारिक आदि शरीर तथा इन्द्रियों के बन्धन में पड़ता है तथा ज्ञानादि गुणों का घात करता है। इसी का नाम संसार है। इसका निदान कारण कर्म ही है। वह कर्म चाहे पुण्य हो और चाहे पाप, परन्तु बन्ध के कारण सभी हैं, इसलिए निश्चयनय से पुण्य व पाप कर्म में कोई भेद नहीं है। व्यवहार के अवलम्बी उन जीवों को कहते हैं कि जो पाप कर्म से, पुण्यकर्म को कुछ अच्छा समझते हैं, क्योंकि पाप कर्म का उदय रहने पर जीव अशान्ति या दुःख में फँसे रहते हैं जिससे कि धर्म को धारण करने की तरफ सन्मुख होना कठिन पड़ जाता है। नरक- निगोदादि की गतियाँ तीव्र पाप कर्म के उदय से प्राप्त होती हैं, जहाँ कि धर्म का लाभ असम्भव और अति कठिन हो जाता है। किन्तु पुण्य के उदय में इस जीव को अरिहंतादि परमेष्ठियों का समागम मिलने लगता है। ऐसे अवसर पर उनके प्रति भक्ति-पूजा तथा उनके स्वरूप को समझने का मार्ग खुलता है, तब आत्मोन्मुख होने की प्रेरणा मिलती
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org